भौतिक भूगोल एवं मूल सिद्धांत – जलवायु विज्ञान (Climatology)
जलवायु विज्ञान (Climatology)
1. पृथ्वी का ताप बजट, तापमान और दाब बेल्ट
पृथ्वी का ताप बजट (Heat Budget of Earth)
परिभाषा:
पृथ्वी का ताप बजट सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा (सौर विकिरण) और पृथ्वी द्वारा वापस अंतरिक्ष में उत्सर्जित दीर्घ तरंग विकिरण के बीच संतुलन है।मुख्य घटक:
- आगमन (Incoming):
- सूर्य की ओर से आने वाला शॉर्टवेव विकिरण (सौर ऊर्जा)
- परावर्तन (Reflection):
- पृथ्वी की सतह और बादलों द्वारा अवशोषित न होने वाला हिस्सा, जिसे एल्बिडो कहते हैं
- उत्सर्जन (Outgoing):
- पृथ्वी द्वारा दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में अंतरिक्ष में छोड़ी गई ऊष्मा
- आगमन (Incoming):
महत्व:
यदि आने वाली ऊष्मा और उत्सर्जित ऊष्मा का संतुलन बना रहता है, तो पृथ्वी का औसत तापमान स्थिर रहता है। यदि यह संतुलन बिगड़ता है (जैसे कि ग्रीनहाउस गैसों के कारण), तो वैश्विक तापमान में वृद्धि हो सकती है।
तापमान वितरण (Distribution of Temperature)
क्षैतिज वितरण (Horizontal Distribution)
अक्षांश का प्रभाव:
- भूमध्यरेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं, जिससे तापमान अधिक रहता है।
- ध्रुवों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए तापमान कम रहता है।
भूमि-समुद्र अंतर:
- भूमि तेजी से गर्म और ठंडी होती है, जबकि महासागरों का तापमान स्थिर रहता है।
ऊर्ध्वाधर वितरण (Vertical Distribution)
- वायुमंडलीय परतों में:
- सतह के पास तापमान उच्च होता है, लेकिन ऊँचाई बढ़ने पर हवा पतली हो जाती है और तापमान में गिरावट आती है।
- सामान्यतः, हर 300 मीटर की ऊँचाई पर वायुदाब में लगभग 34 मिलीबार की कमी होती है।
दाब पेटियाँ (Pressure Belts)
वायुमंडलीय दबाव, जो तापमान के अंतर के कारण बनता है, पृथ्वी पर विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग होता है। मुख्य पेटियाँ निम्नलिखित हैं:
भूमध्यरेखीय निम्न दाब पेटी (Equatorial Low Pressure Belt):
- भूमध्य रेखा पर अत्यधिक सूर्यतापन के कारण गर्म हवा ऊपर उठती है, जिससे निम्न दबाव का क्षेत्र बनता है।
- इसे इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस ज़ोन (ITCZ) भी कहते हैं।
उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटी (Subtropical High Pressure Belt):
- लगभग 25° से 35° अक्षांश पर स्थित, जहाँ वायुमंडलीय हवा नीचे उतरती है, ठंडी और सूखी हो जाती है।
- यही क्षेत्र अक्सर रेगिस्तान के रूप में भी प्रकट होते हैं।
उप-ध्रुवीय निम्न दाब पेटी (Subpolar Low Pressure Belt):
- लगभग 60° से 65° अक्षांश के बीच, जहाँ गर्म हवा ऊपर उठती है और निम्न दबाव बनता है।
- यह क्षेत्र तूफानी और बदलीले मौसम से संबंधित होता है।
ध्रुवीय उच्च दाब पेटी (Polar High Pressure Belt):
- 70° से 90° अक्षांश पर, जहाँ ठंडी हवा सघन होती है और उच्च दबाव बनता है।
Important
ऊष्मा बजट का संतुलन:
सूर्य से आने वाली ऊष्मा का एक हिस्सा परावर्तित (एल्बिडो) होता है और शेष ऊर्जा पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित की जाती है। यही संतुलन पृथ्वी के स्थायी तापमान का कारण है।तापमान बेल्ट:
भूमध्यरेखा, उपोष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण और ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान में क्रमिक अंतर होता है, जो अक्षांश, भूमि-समुद्र अंतर, ऊँचाई और अन्य भौगोलिक विशेषताओं पर निर्भर करता है।दाब पेटियाँ और वायुमंडलीय परिसंचरण:
ये पेटियाँ वैश्विक पवन पैटर्न (जैसे ट्रेड विंड्स, पश्चिमी हवाएँ, ध्रुवीय हवाएँ) को आकार देती हैं, जो मौसम और जलवायु प्रणाली के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
2. वायुमंडलीय परिसंचरण, मौसमी हवाएँ, मानसून, जेट धाराएँ
1. वायुमंडलीय परिसंचरण (Atmospheric Circulation)
- सूर्य की असमानता: सूर्य की असमान तापीय ऊर्जा वितरण के कारण भूमध्य रेखा के पास अधिक ताप और ध्रुवीय क्षेत्रों में कम ताप होता है। यही ताप अंतर वायुमंडलीय परिसंचरण का मूल आधार है।
- मुख्य सेल: इस ताप अंतर से तीन प्रमुख वायुमंडलीय सेल – हैडले सेल (0° से लगभग 30° तक), फेरल सेल (30° से 60° तक) और पोलर सेल (60° से 90° तक) – बनते हैं।
- कोरिओलिस प्रभाव: पृथ्वी के घूर्णन के कारण हवाओं में दाएं (उत्तर गोलार्ध में) या बाएं (दक्षिण गोलार्ध में) मुड़ाव होता है, जो वैश्विक परिसंचरण के पैटर्न को प्रभावित करता है।
2. मौसमी हवाएँ (Seasonal Winds)
- स्थलीय-सागरी अंतर: गर्मियों में स्थलीय क्षेत्रों में तापमान वृद्धि से आकाशीय दाब कम हो जाता है, जिससे समुद्र से गर्म हवा की ओर हवाएँ (जैसे दक्षिण-पश्चिमी मानसून) बहने लगती हैं। वहीं सर्दियों में ठंडे स्थलीय क्षेत्रों में उच्च दाब बनता है, जिससे समुद्र से ठंडी हवाएँ स्थलीय क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होती हैं।
- परिणाम: ये मौसमी हवाएँ स्थानीय और क्षेत्रीय जलवायु पैटर्न, कृषि और जल संसाधनों के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
3. मानसून (Monsoon)
- तापमान अंतर: मानसून का मुख्य कारण स्थलीय और सागरी क्षेत्रों के बीच तापमान अंतर है। भारतीय उपमहाद्वीप में गर्मियों में स्थलीय तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है, जिससे समुद्र के तुलनात्मक रूप से ठंडे क्षेत्र में उच्च दाब बनता है।
- दिशा परिवर्तन: इस दाब अंतर के कारण हवाओं की दिशा पलट जाती है – जून से सितंबर तक दक्षिण-पश्चिमी हवाएँ भारत में भारी वर्षा लाती हैं, जो भारतीय कृषि और जलवायु के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- परिणाम: मानसून की तीव्रता, समय और वितरण में परिवर्तन से सूखा, बाढ़ जैसी घटनाएँ हो सकती हैं, जिनका UPSC में मौसम एवं पर्यावरण से जुड़े प्रश्नों में उल्लेख किया जाता है।
4. जेट धाराएँ (Jet Streams)
- परिभाषा: जेट धाराएँ वायुमंडल की ऊपरी परत (लगभग 9–16 किलोमीटर ऊंचाई) में बहुत तेज गति से बहने वाली पतली हवाएँ होती हैं।
- प्रकार: मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं – उपोष्णकटिबंधीय (Subtropical) और ध्रुवीय (Polar) जेट धाराएँ।
- उत्पत्ति: ये धाराएँ तेज तापमान अंतर (temperature gradients) के कारण बनती हैं और मौसम प्रणालियों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- महत्व: जेट धाराएँ चक्रवातों, तूफानों तथा मानसून की गतिशीलता और तीव्रता को प्रभावित करती हैं, जिससे वैश्विक मौसम पैटर्न पर भी गहरा असर पड़ता है।
3. कोपेन, थॉर्नथवेट आदि का जलवायु वर्गीकरण
कोपेन जलवायु वर्गीकरण:
यह प्रणाली व्लादिमीर कोपेन द्वारा विकसित की गई है, जो मुख्य रूप से तापमान और वर्षा के आधार पर जलवायु को पाँच प्रमुख समूहों में बाँटती है:
- A (उष्णकटिबंधीय): पूरे वर्ष ऊँचे तापमान और पर्याप्त वर्षा (जैसे ट्रॉपिकल रेनफ़ॉरेस्ट, मॉनसून क्लाइमेट)
- B (सूखा): ऐसी जलवायु जहाँ वर्षा बहुत कम होती है, और वाष्पीकरण अधिक (मरुस्थलीय या अर्ध-शुष्क क्षेत्र)
- C (मध्यम): सौम्य तापमान के साथ स्पष्ट ऋतु परिवर्तन, मध्यम वर्षा (उष्णकटिबंधीय से थोड़ी ठंडी, या भूमध्यरेखीय क्षेत्र)
- D (महाद्वीपीय): गहन ऋतु परिवर्तन, जहाँ गर्मियाँ और सर्दियाँ दोनों स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं (ठंडे क्षेत्रों के लिए)
- E (ध्रुवीय): अत्यंत ठंडी जलवायु, जहाँ तापमान बहुत कम रहता है और वर्षा न्यूनतम होती है
थॉर्नथवेट जलवायु वर्गीकरण:
यह प्रणाली थॉर्नथवेट द्वारा विकसित की गई है, जो केवल तापमान नहीं बल्कि जलवायु में जल उपलब्धता पर भी जोर देती है। इसमें संभावित वाष्पीकरण (Potential Evapotranspiration) के आधार पर एक “मॉइस्चर इंडेक्स” निकाला जाता है। इस इंडेक्स से यह निर्धारित किया जाता है कि क्षेत्र में वर्षा से कितनी मात्रा में नमी उपलब्ध है या कमी है। इस आधार पर विभिन्न क्षेत्रों को हाइपर-आरिड (अत्यधिक सूखा), आरिड, सेमी-आरिड, सब-ह्यूमिड, ह्यूमिड या पेर-ह्यूमिड के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
जलवायु का वर्गीकरण
जलवायु का वर्गीकरण विभिन्न प्रणालियों के आधार पर किया जाता है। सबसे प्रमुख और व्यापक रूप से प्रयोग में लाया जाने वाला वर्गीकरण है कोपेन जलवायु वर्गीकरण, जिसे व्लादिमीर कोपेन ने विकसित किया था। इस प्रणाली में जलवायु को मुख्य रूप से निम्नलिखित पाँच समूहों में बाँटा जाता है:
A (उष्णकटिबंधीय जलवायु):
- पूरे वर्ष उच्च तापमान रहता है
- पर्याप्त वर्षा होती है, जिससे वर्षा-आधारित वनस्पति (जैसे रेनफॉरेस्ट) पाई जाती है
B (सूखा जलवायु):
- वर्षा बहुत कम होती है
- वाष्पीकरण की दर वर्षा से अधिक होती है, जिसके परिणामस्वरूप मरुस्थल या अर्ध-शुष्क क्षेत्र बनते हैं
C (उपोष्ण जलवायु):
- यहाँ तापमान में मामूली अंतर होता है
- स्पष्ट रूप से परिभाषित ऋतुएँ होती हैं, जैसे गर्म और ठंडे महीनों का अंतर
D (महाद्वीपीय जलवायु):
- इसमें तापमान में गहरी ऋतु परिवर्तन होते हैं
- गर्मियाँ काफी गर्म और सर्दियाँ ठंडी होती हैं, आमतौर पर महाद्वीपीय क्षेत्रों में
E (ध्रुवीय जलवायु):
- अत्यंत ठंडी जलवायु जहाँ तापमान हमेशा बहुत कम रहता है
- वर्षा अत्यंत न्यून होती है, ज्यादातर बर्फ के रूप में
प्रत्येक मुख्य समूह के अंतर्गत उप-वर्गीकरण भी होता है, जो तापमान, वर्षा और ऋतुओं की अवधि के आधार पर और अधिक विश्लेषणात्मक रूप से विभाजन प्रदान करते हैं।
इसके अलावा, थॉर्नथवेट जलवायु वर्गीकरण भी महत्वपूर्ण है, जो जलवाष्पीकरण (Potential Evapotranspiration) के आधार पर किसी क्षेत्र की नमी स्थिति का आकलन करता है। इस प्रणाली में क्षेत्र की नमी उपलब्धता के आधार पर सूखे, आर्द्र और मध्यम क्षेत्रों की पहचान की जाती है।
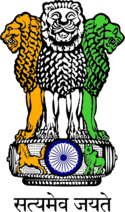
What’s up guys? Gave yo88vina a whirl. Not bad, not amazing, just alright. Has many Vietnamese favorite games, which is cool for some users. The graphics, while not overly stylized, are acceptable. Come see it for yourself yo88vina.