विज्ञान और सभ्यता की विरासत (प्राचीन भारत का इतिहास)
धर्म
प्रकृति के साथ मनुष्य के टकराव होने से कई महत्त्वपूर्ण घटनाएँ घटीं। लोगों को अपने जीविकोपार्जन के लिए जंगलों, पहाड़ों, कठोर मिट्टी, सूखे, बाढ़, जंगली जानवरों इत्यादि द्वारा उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करना पड़ा। इस प्रक्रिया में उन्होंने प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित किए। उन्होंने ई.पू. सातवीं सहस्राब्दि में कृषि करना शुरू किया। लेकिन उस समय तक वह आग, बाढ़ और अकाल जैसे प्राकृतिक खतरों से प्रभावी ढंग से लड़ने में सक्षम नहीं थे। इन खतरों से संघर्ष के दौरान उनके लिए कुछ खतरों और कठिनाइयों पर काबू करना असम्भव प्रतीत हुआ। इसलिए इस स्थिति में उन्हें प्रकृति के साथ सम्ञ्जस्यता का व्यवहार भी करना पड़ा। दूसरी ओर, लोगों ने उपजाऊ मिट्टी, समयानुकूल बारिश और प्रकृति के अन्य उपहारों का लाभ उठाया। इसलिए प्रकृति प्रदत्त इन साधनों और प्रकृति द्वारा निर्मित कमी ने उन्हें धर्म और अलौकिक शक्तियों के बारे में सोचने पर मजबूर किया।
प्राचीन भारत में ब्राह्मणवाद या हिन्दू धर्म, प्रमुख धर्म के रूप में विकसित हुआ; और समग्र रूप से कला, साहित्य एवं समाज को प्रभावित किया। ब्राह्मणवाद के अतिरिक्त, भारत में जैन और बौद्ध धर्म का भी जन्म हुआ। ईसाई धर्म यहाँ पहली शताब्दी में ही पहुँच चुका था, किन्तु प्राचीन काल में यह बहुत विस्तृत नहीं था। बौद्ध धर्म भी कुछ समय बाद भारत से गायब हो गया, हालाँकि इसका विस्तार पूर्व में जापान और उत्तर-पश्चिम में मध्य एशिया तक हो चुका था। प्रसार की प्रक्रिया में, बौद्ध धर्म ने व्यापक स्तर पर पड़ोसी देशों में भारतीय कला, भाषा और साहित्य को बढ़ाया। जैन धर्म भारत में बना रहा और अपनी कला एवं साहित्य के विकास में इसने सहायता की। आज भी इनके अनुयायियों की संख्या, खासकर राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक के व्यापारिक समुदायों में अधिक है।
वर्ण व्यवस्था
भारत में सामाजिक वर्गों के निर्माण में धर्म का विशेष प्रभाव पड़ा। अन्य प्राचीन समाज में, सामाजिक वर्गों के कर्तव्यों और कार्यों को कानून द्वारा तय किया जाता था, जो काफी हद तक राज्य द्वारा संचालित होता था। हालाँकि भारत में वर्ण संबंधी-कानून, राज्य एवं धर्म, दोनों से तय होता था। पुजारियों, क्षत्रियों, किसानों और मजदूरों के कार्यों को दैवीय आदेशों की तरह परिभाषित और निर्धारित किया गया था। जो लोग अपने कार्य से मुकरते थे और दोषी पाए जाते थे, उन्हें दण्डित किया जाता था। वे अपने वर्षों के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान और पश्चाताप करते थे। प्रत्येक वर्ण की न केवल सामाजिक बल्कि अनुष्ठानिक पहचान थी। समय के साथ, वर्षों या सामाजिक वर्गों और जातियों को कानून और धर्म द्वारा वंशानुगत बना दिया गया। यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया गया कि ब्राह्मणों को पुरोहित तथा क्षत्रियों को शासक बनाए रखने के लिए वैश्य उत्पादन और कर-भुगतान करते रहें तथा शूद्र मजदूरी करते रहें। श्रम एवं व्यवसायों की विशेषज्ञता के आधार पर निर्धारित जाति या वर्ण विभाजन की इस व्यवस्था ने, निश्चय ही प्रारम्भिक चरण में समाज और अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक रही। उत्पादन और श्रमिक वर्गों को निरस्त्र कर दिया गया और धीरे-धीरे प्रत्येक जाति को एक दूसरे के खिलाफ ऐसा भड़काया गया कि जो दमित थे, वे कभी भी इस उच्च वर्ग या विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों के खिलाफ एकजुट न होने पाएँ।
विभिन्न वर्गों के दिमाग में अपने कार्यों को पूरा करने की आवश्यकता इतनी गहराई से बैठाई गई थी कि वे सामान्यतः अपने धर्म से भटकने की कभी सोच भी नहीं पाते थे। भगवद्गीता ने सिखाया कि लोगों को अपने धर्म की रक्षा करने में जीवन लगा देना चाहिए; दूसरों के धर्म को अपनाना खतरनाक साबित होगा। निचले वर्ण के लोगों ने दृढ़ विश्वास से कड़ी मेहनत की, ताकि वे अगले जन्म में और बेहतर जीवन के लायक हों सकें। वस्तुतः, इसी धारणा ने उत्पादन करने वाले लोगों और इन उत्पादनों पर निर्भर रहने वाले शासकों, पुजारियों, अधिकारियों, सैनिकों एवं बड़े व्यापारियों के बीच तनाव और संघर्ष की तीव्रता एवं बारम्बारता को कम किया। इसलिए, प्राचीन भारत में निम्न वर्गों का दमन के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही की इतनी जरूरत नहीं हुई, जितनी ग्रीस और रोम में शासक के आदेशों के विरुद्ध गुलामों एवं अन्य उत्पादक वर्गों के खिलाफ की जाती थी। क्योंकि ब्राह्मणवादी विचार एवं वर्ण व्यवस्था से उपजी परिस्थिति के विरुद्ध वैश्यों एवं शूद्रों की मान्यता एवं दृढ़ विश्वास ने उन्हें स्वतः ही इस उच्च वर्ण या वर्ग के अधीन बनाए रखा।
दार्शनिक प्रणालियाँ
भारतीय विचारकों ने दुनिया को एक भ्रम यानि ‘माया’ माना। उन्होंने आत्मा एवं परमात्मा के सम्बन्ध पर गम्भीर मन्थन किया। दरअसल, भारतीय दार्शनिकों के अलावा और किसी देश के दार्शनिकों ने इस विषय में इतनी गहराई से नहीं सोचा। दर्शन और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्राचीन भारत महत्त्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन इसके अलावा भी भारतीयों ने भी दुनिया के बारे में भौतिकवादी दृष्टि विकसित की। भारतीयों द्वारा निर्मित दर्शन की छह प्रणालियों में से एक, सांख्य प्रणाली में भौतिकवादी दर्शन के तत्त्व पाए जाते हैं। ई.पू. 580 के आस-पास पैदा हुए कपिल, इसके प्रवर्तक थे। उनका मानना था कि आत्मा केवल वास्तविक ज्ञान के माध्यम से ही मुक्ति प्राप्त कर सकती है, जो प्रत्यक्ष, अनुमान और श्रवण से प्राप्त किया जा सकता है। सांख्य प्रणाली ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानती। इसके अनुसार, संसार का निर्माण ईश्वर ने नहीं, बल्कि प्रकृति ने किया है। संसार एवं मानव जीवन, प्राकृतिक शक्तियों द्वारा नियन्त्रित होती हैं। तर्क के विकास से सांख्य प्रणाली को सहायता मिली। पाँचवीं शताब्दी से पहले, तर्क कोई विधिवत् स्थापित अनुशासन नहीं था। ऐसा लगता है कि सन् 400 के आस-पास न्याय सूत्र संकलित किया गया। इसमें चार प्रमाणों का उल्लेख, जिनमें प्रत्यक्ष, अनुमान, सापेक्ष और शब्द-प्रमाण शामिल हैं। इसमें वैध और अमान्य ज्ञान के बारे में विस्तृत चर्चा है; हर प्रकार के प्रमाण के पहलुओं पर विस्तार से विचार किया गया है। यद्यपि, वाद-विवाद विधियों का उपयोग धार्मिक विवादों में किया जाता था, लेकिन इन्हें भूमि विवाद सहित अन्य किसी विवाद से अलग विकसित नहीं किया जा सकता था।
भौतिकवादी दर्शन को सर्वाधिक प्रोत्साहन चार्वक से मिला, जो ई.पू. छठी शताब्दी में थे। उन्होंने जो दर्शन दिया, उसे लोकायत कहा जाता है। उन्होंने तर्क दिया कि मनुष्य अपने संवेदी अंगों के माध्यम से जो अनुभव नहीं करता, वास्तव में उसका अस्तित्व नहीं होता। इसका अर्थ हुआ कि ईश्वर का भी अस्तित्व नहीं है। हालाँकि, व्यापार, हस्तशिल्प और शहरीकरण में पतन के साथ, दर्शन की आदर्शवादी स्थिति अस्तित्व में आई। आदर्शवादी दर्शन ने सिखाया कि दुनिया भ्रम है। उपनिषद द्वारा लोगों को संसारिकता से मुक्त होने और वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने को प्रेरित किया गया। पश्चिमी विचारकों ने उपनिषदों की शिक्षाओं को माना, क्योंकि वे आधुनिक प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित मानव समस्याओं को हल करने में असमर्थ थे। प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक, शोपेनहावर ने अपने दर्शन में वेदों और उपनिषदों को स्थान दिया। उनका मानना था कि उपनिषद ने उनके जीवन में शान्ति प्रदान की और मृत्यूपरान्त भी शान्ति देगा।
शिल्प और प्रौद्योगिकी
यह सोचना गलत होगा कि भारतीयों ने भौतिक संस्कृति में कोई योगदान नहीं दिया। पहला सबसे बड़ा योगदान हड़प्पा संस्कृति द्वारा किया गया था। इस काँस्य युग की संस्कृति के दौरान, इसका क्षेत्र विस्तार मिस्त्र या मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी ज्यादा था। इस दौरान सर्वाधिक पकी ईंटें तैयार हुई, शिल्प, वाणिज्य और कृषि की खूब प्रगति हुई। जिसने निःसन्देह अच्छे शहर नियोजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।
प्राचीन काल में भारतीयों ने उत्पादन के कई क्षेत्रों में भी दक्षता हासिल की। भारतीय कारीगरों ने रंगाई और विभिन्न प्रकार के रंगों को तैयार करने में विशेषज्ञता हासिल की। भारत में बने मूल रंग इतने चमकदार और स्थायी थे कि अजन्ता के अद्भुत चित्रों में अब भी उतनी ही चमक बरकरार हैं।
इसी तरह, भारतीयों ने इस्पात बनाने की कला में भी विलक्षण विशेषज्ञता हासिल की। यह शिल्प सबसे पहले भारत में ई.पू. 200 में विकसित हुआ। भारतीय इस्पात बहुत पहले से दुनिया के कई देशों में निर्यात किया गया। बाद में इसे बुद्ध कहा जाता था। भारतीय कारीगरों द्वारा निर्मित तलवार दुनिया के किसी भी अन्य देशों की तुलना में श्रेष्ठ थे और एशिया से लेकर पूर्वी यूरोप तक इनकी माँग थी।
राजनीति
कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार, बड़े साम्राज्य का प्रशासन चलाने और जटिल समाज की समस्याओं को सुलझाने में भारतीय हमेशा से, निःसन्देह सक्षम थे। भारत ने अशोक जैसे महान शासक को जन्म दिया, जिसने कलिंग पर अपनी जीत के बावजूद शान्ति और अनाक्रमण की नीति अपनाई। अशोक एवं कई अन्य भारतीय राजा धार्मिक सहिष्णुता को मानते थे; अन्य धर्मों के अनुयायियों की इच्छाओं का सम्मान करने पर बल देते थे। ग्रीस के अलावा, भारत एकमात्र ऐसा देश था, जहाँ लोकतन्त्र के स्वरूप को अपनाया गया।
विज्ञान और गणित
भारत ने विज्ञान में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। प्राचीन काल में, धर्म और विज्ञान अतुलनीय रूप से जुड़े हुए थे। भारतीय खगोल विज्ञान ने भी काफी प्रगति की हालाँकि उस समय ग्रहों को ईश्वर का रूप माना जाता था, किन्तु इससे यह हुआ कि इस पर काफी ध्यान दिया गया। जो कि कृषि कार्यों के लिय ऋतुओं और मौसम की स्थितियों में परिवर्तन के कारण ग्रहों का अध्ययन आवश्यक ही था। व्याकरण और भाषा विज्ञान का ज्ञान भी उत्पन्न हुआ, क्योंकि प्राचीन ब्राह्मणों ने हर वैदिक प्रार्थना और मन्त्रोच्चार की शुद्धता पर जोर दिया। वस्तुतः, भारतीयों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पहला परिणाम संस्कृत व्याकरण का विकास था। ई.पू. पाँचवीं शताब्दी में, पाणिनी ने संस्कृत को नियन्त्रित करने वाले नियम बनाए और अष्टाध्ययी शीर्षक से व्याकरण तैयार किया।
ई.पू. तीसरी शताब्दी तक, गणित, खगोलशास्त्र और औषधि विज्ञान अलग-अलग विकसित हुए। गणित के क्षेत्र में, प्राचीन भारतीयों ने तीन विभिन्न योगदान दिए-अंकन प्रणाली, दशमलव प्रणाली और शून्य का उपयोग। पाँचवीं शताब्दी की शुरुआत में दशमलव प्रणाली के उपयोग के लिखित साक्ष्य मिलते हैं। भारतीय अंकन प्रणाली को अरबों ने अपनाया और इसे पश्चिमी दुनिया में फैलाया। भारतीय अंकों को अंग्रेजी में अरबी कहा जाता है, लेकिन अरबों ने स्वयं अपने अंक को हिन्द नाम दिया और पश्चिम में अपनाए जाने से पहले सदियों तक भारत में इस्तेमाल होता रहा। ऐसा अशोक के अभिलेखों में भी मिलता है जो ई.पू. तीसरी शताब्दी में लिखे गए थे।
भारतीयों ने दशमलव प्रणाली का सबसे पहले इस्तेमाल किया। आर्यभट्ट (सन् 476-500) इससे परिचित थे। चीनियों ने इसे बौद्ध धर्म प्रचारकों से सीखा और जब अरब भारत के सम्पर्क में आए, तो बाद में पश्चिमी दुनिया ने इसे अरबों से सीखा। ई.पू. दूसरी शताब्दी में भारतीयों द्वारा शून्य की खोज की गई थी। भारतीय गणितज्ञ शून्य को एक अलग अंक मानते थे और इस अर्थ में इसे अंकगणित में उपयोग किया गया। अरब में, शून्य का सबसे पहला उपयोग सन् 873 में हुआ। अरबों ने इसे भारत से सीखा, अपनाया और यूरोप में फैलाया। हालाँकि भारतीयों और यूनानियों, दोनों ने बीजगणित में योगदान दिया; लेकिन पश्चिमी यूरोप में इसका ज्ञान यूनान से नहीं, अरब से सीखा, जबकि अरबों ने इसे भारत से सीखा था।
हड़प्पा के ईंट निर्माण दर्शाते हैं कि उत्तर-पश्चिमी भारत में, लोगों को माप और ज्यामिति का पर्याप्त ज्ञान था। आखिरकार वैदिक लोग इस ज्ञान से लाभान्वित हुए, जो लगभग ई.पू. पाँचवीं शताब्दी के सुल्वसूत्र में मिलता है। ई.पू. दूसरी शताब्दी में, राजाओं को यज्ञ करने हेतु अपस्तम्बा ने वेदियों के निर्माण के लिए एक व्यावहारिक ज्यामिति का निर्माण किया। उन्होंने न्यूनकोण, अधिककोण और समकोण का वर्णन किया। आर्यभट्ट ने त्रिभुज के क्षेत्र की गणना करने की विधि बनाई, जिससे त्रिकोणमिति का उद्भव हुआ। इस काल की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक सूर्यसिद्धान्त है। समकालीन प्राचीन पूरब में इस तरह की कोई दूसरी रचना नहीं मिलती है।
खगोलशास्त्र के सबसे प्रसिद्ध विद्वान आर्यभट्ट और वराहमिहिर थे। आर्यभट्ट और वराहमिहिर क्रमशः पाँचवीं और छठी शताब्दी में थे। आर्यभट्ट ने ग्रहों की स्थिति की गणना बेबीलोनियन विधि के अनुसार की थी। उन्होंने चन्द्र और सूर्य ग्रहण के कारणों की खोज की। पृथ्वी की परिधि, जिसे उन्होंने अटकलों के आधार पर मापा, आज भी सही मानी जाती है। उन्होंने कहा कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूमती है। गणितीय और खगोलीय ज्ञान के विकास में आर्यभट्ट की विशिष्ट कृति आर्यभट्टीय एक मील का पत्थर है; यह त्रिकोणमिति के क्षेत्र में एक विशिष्ट योगदान है। इसके आधार पर, उपहार और सम्पत्ति के विभाजन में शामिल सभी आकृतियों और आकारों को मापा जा सकता है और प्रारम्भिक मध्य काल में किराए या कर निर्धारण के लिए मूल्यांकन किया जा सकता था। मन्दिरों एवं महलों के निर्माण तथा अन्य इंजीनियरिंग कार्यों के लिए आवश्यक विभिन्न मापों के लिए भी इस ज्ञान का इस्तेमाल किया जा सकता है। शून्य एवं दशमलव प्रणाली का उल्लेख आर्यभट्टीय में है, लेकिन भारत में इसका उपयोग किसी महत्त्वपूर्ण काम में नहीं हुआ। अरबों के माध्यम से जब यह पश्चिम की ओर फैला, तो दसवीं शताब्दी में इसे इटली के व्यापारियों द्वारा बही-खाता के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। छठी और दसवीं शताब्दी के बीच व्यापार में भारत का नुकसान सम्भवतः शून्य और दशमलव प्रणाली की उपेक्षा से जुड़ा हो सकता है। सातवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ब्रह्मगुप्त द्वारा विकसित बीजगणित के माध्यम से, माप एवं कृषि खगोलीय गणनाओं से सम्बद्ध अधिक सटीक, सुसंगत और प्रासंगिक ज्ञान प्रस्तुत किया गया।
वराहमिहिर की प्रसिद्ध कृति बृहत्संहिता छठी शताब्दी में लिखी गई। उन्होंने कहा कि चन्द्रमा, पृथ्वी के चारों ओर और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। उन्होंने ग्रहों की गतिविधियाँ और कुछ अन्य खगोलीय समस्याओं की व्याख्या के लिए कई यूनानी कार्यों का उपयोग किया। यद्यपि यूनानी ज्ञान ने भारतीय खगोल विज्ञान को प्रभावित किया, लेकिन भारतीयों ने निश्चित रूप से इस विषय को आगे बढ़ाया और ग्रहों की अपनी टिप्पणियों में इसका इस्तेमाल किया।
वराहमिहिर द्वारा प्रस्तुत पौध एवं पशु सम्बन्धी वर्गीकरण ने कृषि ज्ञान को समृद्ध किया। यद्यपि उनकी भविष्यवाणियाँ कई सामाजिक मामलों से सम्बन्धित हैं, नए घरों के निर्माण हेतु स्थलों के चयन के सम्बन्ध में उनके द्वारा दिए गए निर्देश नए गाँवों की स्थापना से जुड़े हैं। इसी तरह, ऋतुओं एवं मौसम से सम्बद्ध वराहमिहिर का अवलोकन कृषि पंचांग बनाने में उपयोगी साबित हुआ। उन्होंने जोर दिया कि मौसम में परिवर्तन के साथ तालमेल रखने के लिए पंचांग को निरन्तर अद्यतन किया जाना चाहिए। वराहमिहिर ने एक प्रकार से खगोलविद-सह-ज्योतिषी का काम किया। कई भूमि दस्तावेजों से प्राप्त सूचनानुसार ज्योतिषी का काम प्रारम्भिक मध्यकाल में शुरू हुआ। ग्रामीण इलाकों में, ज्योतिष पुजारी जजमानी प्रथा के अभिन्न अंग बन गए।
भारतीय कारीगरों ने रसायन विज्ञान के विकास में बहुत योगदान दिया। भारतीय रंगरेजों ने स्थायी रंगों का आविष्कार किया और उन्होंने नीले रंग की खोज की। हमें याद हो कि इस्पात का उत्पादन करने वाले दुनिया के सबसे पहले कारीगर, भारतीय ही थे।
औषधि
प्राचीन भारतीय चिकित्सकों ने शारीरिक रचना का अध्ययन किया। उन्होंने बीमारियों की व्याख्या की और उसके उपचार के लिए दवाइयाँ तैयार कीं। दवाओं का सबसे पहला उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, लेकिन अन्य प्राचीन समाज की तरह यहाँ बीमारियों के उपचार हेतु टोने-टोटके एवं जादुई मन्त्रों का उपयोग होता था, वैज्ञानिक रूप से दवाएँ विकसित नहीं हुई थीं।
दूसरी शताब्दी ईस्वी में भारत ने आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध विद्वानों को जन्म दिया, सुश्रुत और चरक। सुश्रुतसंहिता में, सुश्रुत ने मोतियाबिन्द, पथरी जैसी कई अन्य बीमारियों की शल्य चिकित्सा के तरीके का वर्णन किया है। उन्होंने शल्य चिकित्सा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 121 औजारों का उल्लेख किया। बीमारी के उपचार में उन्होंने आहार और सफाई पर विशेष बल दिया। चरक की चरकसंहिता भारतीय औषधि के विश्वकोष की तरह है। इसमें विभिन्न प्रकार के बुखार, कुष्ठ रोग, हिस्टीरिया (मिर्गी) और तपेदिक का वर्णन है। शायद चरक को पता नहीं था कि इनमें से कुछ रोग संक्रामक हैं। उनकी पुस्तक में बड़ी संख्या में पौधों और जड़ी-बूटियों के नाम शामिल हैं, जिन्हें दवाइयों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अतः यह ग्रन्थ न केवल भारतीय औषधि के अध्ययन के लिए, बल्कि प्राचीन भारतीय वनस्पतियों एवं रसायन विज्ञान के लिए भी उपयोगी है। कालान्तर में चरक को आधार मानकर ही भारतीय दवाइयाँ विकसित हुईं।
भूगोल
भूगोल के अध्ययन में, प्राचीन भारतीयों ने भी कुछ योगदान दिया। उन्हें भारत के बाहर की भूमि के भूगोल का बहुत ज्ञान नहीं था, लेकिन नदियों, पर्वत श्रृंखलाओं, तीर्थस्थलों और देश के विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन महाकाव्यों और पुराणों में मिलता है। भारत के लोग यद्यपि चीन और पश्चिमी देशों से परिचित थे, लेकिन उन्हें उन जगहों और उसकी दूरी का कोई स्पष्ट अनुमान नहीं था।
शुरुआती समय में भारतीयों ने समुद्री मार्ग के कुछ ज्ञान प्राप्त किए और जहाज निर्माण में योगदान दिया। चूँकि महत्त्वपूर्ण राजनीतिक शक्तियों का केन्द्र तट से दूर था और समुद्र से कोई खतरा नहीं था, इसलिए प्राचीन भारत के शासकों ने समुद्री यात्रा पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया।
कला और साहित्य
हड़प्पा के समय से ही प्राचीन भारतीय राजमिस्त्री और कारीगरों ने कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए। ऐतिहासिक काल में, अशोक द्वारा बनावाए गए एक-एक खम्भे, चमक एवं पॉलिश के लिए प्रसिद्ध है, जो उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड (NBPW) की चमक से मिलता है। यह अब भी एक रहस्य का विषय है कि कारीगरों ने मिट्टी के बर्तनों और स्तम्भों पर कैसे ऐसी पॉलिश की। मौर्य काल के पॉलिश किए खम्भों पर जानवरों की मूर्तियाँ पर, विशेष रूप से शेरों की मूर्तियाँ मिलती हैं। शेर के सिर वाले स्तम्भ को भारत गणराज्य द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। हम अजन्ता के गुफा-मन्दिरों के साथ-साथ प्रसिद्ध अजन्ता-चित्रों का भी उल्लेख कर सकते हैं, जो ईस्वी सन् की शुरुआत में निर्मित हुए। अजन्ता, एक तरह से एशियाई कला का जन्म स्थान है। ई.पू. दूसरी शताब्दी से ईस्वी सन् सातवीं शताब्दी के बीच तीस गुफा मन्दिरों का निर्माण हुआ। दूसरी शताब्दी में चित्रकारी की शुरुआत हुई, उनमें से ज्यादातर गुप्त काल से सम्बन्धित हैं। उनके विषय बुद्ध के पिछले अवतार और अन्य प्राचीन साहित्य की कहानियों से लिए गए थे। अजन्ता के भारतीय चित्रकारों की उपलब्धि को सभी कला समुदायों द्वारा भरपूर सराहा गया है। अजन्ता में इस्तेमाल की जाने वाली रेखाएँ और रंग, प्रवीणता प्रदर्शित करते हैं, जो यूरोप में पुनर्जागरण के पहले तक दुनिया कहीं नहीं पाई गईं हैं। इसके अलावा, भारतीय कला भारत तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि एक तरफ मध्य एशिया एवं चीन तथा दूसरी तरफ दक्षिण-पूर्व एशिया तक फैली। अफगानिस्तान और मध्य एशिया के पड़ोसी हिस्सों में भारतीय कला के प्रसार का केन्द्र बिन्दु गान्धार था। भारतीय कला के तत्त्वों को मध्य एशियाई और हेलेनिस्टिक कला के साथ जोड़ दिया गया, जिसने एक नई कला शैली को जन्म दिया, जिसे गान्धारशैली कहा जाता था। बुद्ध की पहली प्रतिमा इसी शैली में निर्मित थी। हालाँकि, यह भारतीय कला का नमूना है किन्तु इसके आकार और सिर की बनावट और वस्त्रों पर यूनानी प्रभाव दिखते हैं। इसी प्रकार, दक्षिण भारत में निर्मित मन्दिरों को दक्षिण-पूर्व एशिया में मन्दिर निर्माण के आदर्श नमूने के रूप में पेश किया गया। हम कम्बोडिया के अंकोर वाट और जावा में बोरोबुदुर मन्दिर को याद कर सकते हैं।
शिक्षा के क्षेत्र में, लेखन का पहला उपयोग, हड़प्पा संस्कृति में ई.पू. तीसरी सहस्राब्दि में किया गया, हालाँकि इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। ऐतिहासिक समय में हम नालन्दा के विशाल विहारों की स्थापना में उच्च शिक्षा का प्रावधान पाते हैं, जो न केवल भारत के विभिन्न हिस्सों, बल्कि तिब्बत और चीन से भी छात्रों को आकर्षित करता था। परीक्षा के कठोर मानदण्ड थे और विश्वविद्यालय में केवल उन्हीं को प्रवेश मिलता था जो द्वारपण्डित या ‘स्कॉलर एट द गेट’ द्वारा निर्धारित परीक्षा में उत्तीर्ण होते थे। नालन्दा एक आवासीय-सह-शिक्षण संस्थान के शुरुआती उदाहरणों में से एक है, जहाँ हजारो भिक्षु ज्ञान, दर्शन और चिन्तन के प्रति समर्पित थे।
साहित्य के क्षेत्र में, भारतीयों ने ऋग्वेद की रचना की, जो इण्डो-आर्यन भाषा और साहित्य का प्राचीन उदाहरण है और इसके आधार पर आर्य संस्कृति के स्वाभाव का निर्धारण करने का प्रयास किया गया है। गुप्त काल में कलिदास ने सर्वश्रेष्ठ कृतियों की रचना की दुनिया के सभी महत्त्वपूर्ण भाषाओं में उनके नाटक अभिज्ञानशकुन्तलम का अनुवाद किया गया।
विशेषताएँ और खामियाँ
प्राचीन भारत की उपलब्धियों को गिनना मुश्किल है। हड़प्पा संस्कृति की उपलब्धिया चौंका देने वाले हैं। हड़प्पा की वस्तुएँ भारत और पाकिस्तान के संग्रहालयों में प्रदर्शित हैं, हालाँकि द्वितीय खाड़ी युद्ध में समकालीन मेसोपोटामिया की पुरातन वस्तुएँ काफी हद तक खो गईं या नष्ट हो गईं। उत्तरवर्ती हड़प्पा काल में, लोगों ने विज्ञान और सभ्यता के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दिया।
इस सब के बावजूद ब्राह्मणवादी विचारधारा पर आधारित जाति व्यवस्था आज तक बनी हुई है। प्राचीन काल में, अस्पृश्यों सहित शूद्रों को जन्म से ही उनके निम्नता का बोध करा दिया जाता था; महिलाओं की भी यही स्थिति थी, जिन्हें वस्तु समझा जाता था। इस धारणा की धमक अभी भी पूरी तरह गायब नहीं हुई है। इसी तरह, आम लोगों को आज तक भूमि की समस्या झेलनी पड़ रही है। सातवाहनों ने दूसरी शताब्दी में प्रशासनिक अधिकारों के साथ भूमि अनुदान की प्रथा शुरू की। उत्तरवर्ती शासकों ने व्यापक रूप से इस प्रथा का पालन किया, जो भूमि के असमान वितरण और किसानों के दमन का कारण बना। जमीन्दारों और उनके अधिकारों का सम्मान करना लोगों के लिए आवश्यक था और आदेश दिया गया कि भूमि अनुदान के विरोधियों को दण्डित किया जाएगा। इस प्रकार महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में बहुत असमानता दिखी। हालाँकि, कुछ प्राचीन ग्रन्थों ने पूरी दुनिया को एक परिवार (वसुधैव कुटुम्बकम) के रूप में देखा, लेकिन इस आदर्श ने कोई प्रभाव नहीं छोड़ा।
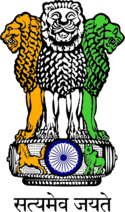
Yo, check out Onebravip! Been having some decent luck there. Super easy to get around the site, and the games are pretty solid. Definitely worth a peek if you’re looking for a new spot to play! Give onebravip a try!