सामाजिक परिवर्तन का अनुक्रम (प्राचीन भारत का इतिहास)
परिचय
हमारे पास पूर्व वैदिक काल के समाज के अध्ययन हेतु कोई लिखित ग्रन्थ उपलब्ध ह नहीं है। किन्तु पुरातत्त्व से हमें जानकारी मिलती है कि पुरापाषाण काल में लोग पहाड़ी इलाकों में छोटे समूहों में रहते थे एवं संगृहीत फल, कन्द-मूल और शिकार, उनके निर्वाह का मुख्य स्रोत था। मनुष्य ने पाषाण युग के अन्त और धातु युग की शुरुआत तक भोजन उत्पादन करना और घरों में रहना सीख लिया था। नवपाषाण और ताम्रपाषाण युगीन समुदाय पहाड़ियों और नदियों के निकट ऊपरी क्षेत्रों में रहते थे। धीरे-धीरे सिन्धु घाटी क्षेत्रों में किसानों के गाँव स्थापित हुए और अन्ततः वे बड़े और छोटे घरों के साथ, हड़प्पा शहरी समाज के रूप में विकसित हुए। हालाँकि, एक बार जब हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई, तो उसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप में दोबारा शहरों का विकास लगभग 1500 वर्षों तक नहीं हुआ।
जनजातीय और पशुचारण काल
ऋग्वेद से आगे के सामाजिक इतिहास के लिए, हम लिखित ग्रन्थों का उपयोग कर सकते हैं। वे हमें बताते हैं कि ऋग्वैदिक समाज, कृषि में दक्षता के बावजूद, मुख्य रूप से पशुचारक था। लोग अर्द्ध-खानाबदोश थे और उनकी प्रमुख सम्पत्ति मवेशी और घोड़े थे। ऋग्वेद में अक्सर गाय, बैल और घोड़े के लिए शब्द आते हैं। मवेशी को धन का समानार्थी माना जाता था, धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। मवेशियों के लिए युद्ध होते थे; इसलिए, राजा, जिनकी मुख्य जिम्मेदारी गायों की रक्षा करनी थी, उन्हें गोप या गोपति कहा जाता था। गाय परिवार के निर्वाह के लिए इतनी महत्त्वपूर्ण थी कि बेटी को दुहित्र कहा जाता था, जिसका अर्थ दूध दुहने वाली होता है। वैदिक लोग मवेशियों से इतने परिचित थे कि जब उन्होंने भारत में भैंस देखी, तो उन्हें गोवाला या बालों वाली गाय कहा। ऋग्वेद में गायों और बैलों के सन्दर्भ के विपरीत, कृषि का उल्लेख कम ही किया गया यद्यपि बाद की ऋचाओं में कुछ उल्लेख मिलता है। सार रूप में, इस समय पशुपालन ही आजीविका का प्रमुख स्रोत था।
ऐसे समाज में, लोग अपनी जरूरत से अधिक उत्पादन नहीं कर पाते थे। जनजाति अपने प्रमुखों को कम ही उपहार दे पाते थे। प्रमुख या राजकुमार की मुख्य आय का स्रोत युद्ध की लूटपाट था। वे दुश्मन जनजातियों को लूटते थे और उनके सहयोगियों से नजराना लेते थे। उनसे प्राप्त नजराना बलि कहलाती थी। ऐसा लगता है कि कबीलाई परिवार अपने प्रमुखों पर भरोसा करते थे और उन्हें स्वेच्छा से उपहार देते थे। इसके बदले, प्रमुख उन्हें विजय दिलाते थे और कठिन समय में उनकी सहायता करते थे। राजकुमारों को अपने कबीले से सम्मान और उपहार प्राप्त करना वैदिक काल में नियम सा बन गया था। हालाँकि, पराजित जनजातियों को लगान वसूली के लिए मजबूर किया जाता था। महत्त्वपूर्ण अवसरों पर उपहार एवं नजराना को सभी स्वजनों में बाँट दिया जाता था। इन उपहारों का सबसे बड़ा हिस्सा पुजारियों को मिलता था, जो अपने जजमानों की ओर से उनकी भलाई के लिए देवताओं से प्रार्थना करते थे। ऋग्वेद के एक अवतरण में, केवल पुजारी, राजकुमारों और यज्ञ करने वालों को समृद्ध करने हेतु देवता से प्रार्थना की गई है। जिसमें असमान वितरण के संकेत के प्रयास दिखते हैं। राजकुमार और पुजारियों ने आम लोगों को दरकिनार कर अपने हिस्से को बढ़ाने का प्रयास किया, जबकि सामान्य लोग राजकुमारों और उनके सैन्य बलों की वीरता एवं उपयोगिता के कारण स्वेच्छा से उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा दे देते थे। यद्यपि इन कबीलों के साधारण सदस्यों को एक हिस्सा ही मिलता था, जिसे अंश या भाग कहा जाता था, यह राजाओं और उनके परिवारों की उपस्थिति में लोकसभा समारोहों में वितरित किया जाता था।
यद्यपि ऋग्वेद के प्रारम्भिक हिस्से में कारीगरों, किसानों, पुजारियों एवं योद्धाओं का उल्लेख मिलता है परन्तु समग्र रूप में यह समाज पूरी तरह से कबीलाई, पशुचारक, अर्ध-खानाबदोश और समतावादी ही था। युद्ध में लूटे गए पशु ही प्रमुख सम्पत्ति होते थे। उपहार के रूप में मवेशी और महिलाओं को दास के रूप में पेश किया जाता था। उपहार के रूप में अनाज का उल्लेख विरले ही है, क्योंकि ये किसी बड़े पैमाने पर उत्पादित नहीं किए जाते थे। इसलिए, युद्धों में लूटी गई सामग्रियों के अलावा, राजकुमारों और पुजारियों के रख-रखाव के लिए कोई अन्य महत्त्वपूर्ण स्रोत नहीं था। ऊँचे सामाजिक वर्ग के बजाय ऊँचा दर्जा प्राप्त करना ज्यादा आसान था। राजकुमार और पुजारी घरेलू सेवा के लिए महिला दास नियुक्त करते थे, लेकिन उनकी संख्या शायद अधिक नहीं थी। ऋग्वैदिक समाज में श्रम श्रेणी का विभाजन नहीं था, बाद में शूद्रों के साथ यह प्रारम्भ हुआ।
कृषि और उच्च श्रेणियों का उद्भव
पैमाने पर कृषक बन गए। उत्तरवर्ती वैदिक काल में, दो या तीन शताब्दियों तक निरन्तर जब वैदिक लोग अफगानिस्तान और पंजाब से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर बढ़े तो वे बड़े बस्तियों का निर्माण होता रहा। इससे क्षेत्रीय प्रमुखों का उदय हुआ। किसानों और अन्य लोगों से प्राप्त करों से राजकुमार यज्ञ करते थे और पुजारियों को दान देते थे। उत्तरवर्ती वैदिक किसानों ने राजवंशों और योद्धाओं को नजराना दिया, जिससे वह पुजारियों को भी यज्ञ के लिए और दक्षिणा स्वरूप शुल्क देते थे। कारीगरों, रथ निर्माताओं, बढ़ई इत्यादि, जो मुख्यतः योद्धाओं की सेवा करते थे, किसान उन्हें भोजन प्रदान करते थे। हालाँकि, उत्तरवतीं वैदिक किसान, व्यापार एवं कस्बों के उदय में योगदान करने में असमर्थ थे; यह बात बुद्ध काल में स्पष्ट गोचर थी। उत्तरवर्ती वैदिक समाज ने सीमित पैमाने पर लोहे का इस्तेमाल किया, लेकिन धातु के पैसे का उपयोग अज्ञात था।
वैदिक समुदायों ने न तो कर प्रणाली विकसित की, न ही वैतनिक सैन्य बल स्थापित किया। शासकों के रिश्तेदार के अलावा कोई कर संग्रहकर्ता नहीं होते थे। राजा को दिया गया कर, भगवान को यज्ञ आदि में दिए गए चढ़ावे के समान होता था। पशुचारक समाज के कबीलाई सेनाओं को हटाकर कृषक समाज के किसानी सेना तैयार हुई। विस, अर्थात् जनजातीय किसानों ने ही सेना गठित की। उत्तरवर्ती वैदिक काल में किसानों को बल कहा जाता था। अश्वमेध घोड़ों की रक्षा करने के लिए सेना में क्षत्रिय और विस दोनों होते थे। आगे-आगे धनुष, तरकस और ढाल से सशस्त्र होकर सेनापति चलता था और पीछे-पीछे लाठी लेकर विस चलते थे। कहा गया है जीत हासिल करने के लिए, प्रमुख राजा या कुलीन को भी विस के साथ एक बर्तन में भोजन करना चाहिए। कृषकों या वैश्यों को योद्धाओं के अधीन करने हेतु पुजारियों ने अनुष्ठानों पर बल दिया, लेकिन फिर भी आदिवासियों को करदाता बनाने में वे असफल रहे। लकड़ी के हल का उपयोग और मवेशियों की अन्धाधुन्ध बलि के कारण किसानों को उत्पादन कर देना मुश्किल होने लगा और वे निरन्तर कर चुकाने में असमर्थ हो गए। दूसरी ओर, राजकुमार पूरी तरह किसानों से अलग नहीं थे। कबीलाई प्रथाओं के अनुरूप, राजाओं से उम्मीद की जाती थी कि वे कृषि कार्य का विस्तार करें और यहाँ तक की हल की मूठ पर हाथ रखने की भी उम्मीद की जाती थी, इसीलिए वैश्य और राजन्य के बीच का अन्तर बहुत नहीं होता था। यद्यपि कुलीनों और योद्धाओं ने किसानों पर शासन किया, उन्हें दुश्मनों से लड़ने के लिए किसानी सेनाओं पर निर्भर होना पड़ता था और जनजातीय किसानों की सहमति के बिना भूमि नहीं दी जा सकती थी। इससे कुलीनों और योद्धाओं को मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ता था और शासकों और शोषितों में अन्तर करना मुश्किल होता था।
उत्पादन और शासन की वर्ण व्यवस्था
उत्तरवर्ती वैदिक काल में तीन प्रक्रियाएँ एक दूसरे से जुड़ीं। ये आर्याकरण, लौह्यकरण और शहरीकरण थे। आर्गीकरण, का अर्थ था संस्कृत, प्राकृत और पाली जैसी इण्डो-आर्यन भाषाओं का प्रसार। इसका अर्थ उच्च वर्गों का वर्चस्व और महिलाओं का दमन भी था। उत्तरवर्ती वैदिक ग्रन्थों में, आर्य शब्द, शूद्रों और दासों को छोड़कर, शुरू के तीन वर्ण समझे जाते थे। यहाँ तक कि बौद्ध सन्दर्भ में, आर्य का अर्थ कुलीन होता है। उत्तरवर्ती वैदिक काल में, आर्याकरण का मतलब आर्येतर जनजातियों को ब्राह्मण संस्कृति के अनुकूल बनाना था। लौह्यकरण का अर्थ निम्न गुणवत्ता वाले इस्पात से निर्मित लोहे के हथियार और उपकरणों का प्रसार था। इससे कृषि एवं शिल्प के विकास और बस्तियों के निर्माण में क्रान्तिकारी बदलाव आए। इस प्रक्रिया ने शासकों की सैन्य शक्तियों को भी बढ़ाया, जिन्होंने अपने राज्यों की सीमाओं को तो बढ़ाया ही साथ ही वर्ण प्रणाली का भी समर्थन किया। शहरीकरण, या शहरों के विकास से व्यापारियों और कारीगरों को मदद मिली और उससे राज्य के राजकोष की आय में भी बढ़ोतरी हुई।
ई.पू. पाँचवीं शताब्दी के आस-पास कृषि और शिल्प के लिए लोहे के औजारों के इस्तेमाल ने इस अपेक्षाकृत समतावादी वैदिक समाज में परिवर्तन कर जाति-विभाजित सामाजिक व्यवस्था की स्थिति में ला खड़ा किया। प्राचीन समय में, लोग लोहे के उपकरणों से परिचित नहीं थे, उनकी संख्या भी सीमित ही थी। अब हालात बदल चुके थे। एक बार जब गंगा के मैदानी इलाकों के जंगलों को आग और लोहे की कुल्हाड़ी की सहायता से साफ कर दिया गया, तो इस दुनिया के सबसे उपजाऊ भाग में बस्तियों का निर्माण होना शुरू हो गया। ई.पू. 500 में, कई ग्रामीण और शहरी बस्तियों की स्थापना हुई। बड़े क्षेत्रीय राज्य मगध साम्राज्य के रूप में उभरे। यह सब सम्भव था, क्योंकि लोहे के हल, हँसिया और अन्य औजारों का उपयोग करते हुए, किसान अपने निर्वाह से अधिक उत्पादन करने में सक्षम थे। किसानों को कारीगरों की जरूरत थी, जिनसे न केवल उन्हें औजार, कपड़े जैसे सामान प्राप्त होते थे, बल्कि वे राजकुमारों और पुजारियों को शस्त्र और विलासिता के सामान भी प्रदान करते थे। उत्तरवर्ती वैदिक काल में नई कृषि उत्पादन तकनीक ने वैदिक युग के लोगों की तुलना में विकास का ऊँचा स्तर प्राप्त किया।
नई तकनीकों और बल प्रयोग ने कुछ लोगों को बड़े पैमाने पर जमीन के मालिक होने में सक्षम बनाया, जिसके लिए पर्याप्त संख्या में दासों और मजदूरों की जरूरत थी। वैदिक काल में, लोग सिर्फ अपने परिवार की सहायता से ही कृषि करते थे; वैदिक साहित्य में मजदूरी के लिए कोई शब्द नहीं है। हालाँकि, कृषि से जुड़े दास और मजदूर बुद्ध काल में प्रमुख विशेषता थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख है कि मौर्य काल में वे बड़े स्तर पर खेती करते थे। हालाँकि, कुल मिलाकर, प्राचीन भारत में दास घरेलू कार्यों के लिए होते थे। आम तौर पर छोटे किसान, कभी-कभी दासों और मजदूरों की सहायता से, उत्पादन में प्रमुख भूमिका निभाते थे।
नई तकनीकों के साथ, किसानों, कारीगरों, मजदूरों और कृषि दासों ने अपने निर्वाह से बहुत अधिक उत्पादन किया। इस उपज का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा राजकुमारों और पुजारियों द्वारा ले लिया जाता था। नियमित संग्रह के लिए, प्रशासनिक और धार्मिक तरीके बनाए गए। राजा ने कर-निर्धारण और कर-संग्रह के लिए कर-संग्रह अधिकारियों को नियुक्त किया था, उन्हें यह भी निर्देश था कि वे राजा के आदेशों के पालन, करों के भुगतान, और पुजारियों को उपहार देने के लिए भी लोगों को समझाएँ। इस उद्देश्य के लिए,वर्ण प्रणाली तैयार की गई थी। इसके अनुसार, तीन उच्च वर्णों या सामाजिक श्रेणी के सदस्यों को चौथे वर्ण के लोगों से विवेकपूर्वक अलग किया गया था। द्विजों को वैदिक अध्ययन और उपनयन संस्कार का अधिकार था और चौथे वर्ण या महिलाओं और शूद्रों को इससे अलग रखा गया था। शूद्र उच्च वर्णों की सेवा के लिए थे और कुछ कानून-निर्माताओं ने दासत्व केवल शुद्रों के लिए निर्धारित किया था। इस प्रकार द्विज ही नागरिक कहे जाते थे और शूद्र गैर-नागरिक। हालाँकि, वहाँ द्विजों और नागरिकों के बीच फर्क पैदा हो गया। ब्राह्मणों को हल चलाने की अनुमति नहीं थी और कारीगरी के लिए उनके तिरस्कार की भावना इतनी बलवती हो उठी कि वे शिल्पकला को अशिष्ट और घृणा की दृष्टि से देखने लगे और कुछ मजदूरों को अछूत समझने लगे। जो व्यक्ति शारीर श्रम कम करता था, वह अधिक शुद्ध माना जाता था। हालाँकि, वैश्य, जो द्विज में आते थे, किसानों, चरवाहों और कारीगरों के रूप में काम करते थे और बाद में व्यापारियों के रूप में। ध्यान देने की बात है कि यहीं लोग प्रमुख करदाता भी थे, जिनके योगदान ने क्षत्रियों और ब्राह्मणों को बनाए रखा। वर्ण प्रणाली ने क्षत्रिय को व्यापारियों और कारीगरों से लगान और किसानों से करें का संग्रह करने का अधिकार प्रदान किया, जिसने उन्हें अपने पुजारियों और कर्मचारियों को नकद भुगतान देने में सक्षम बनाया।
व्यक्ति के वर्ण के अनुसार भुगतान और आर्थिक विशेषाधिकारों के दर भिन्न थे। इस प्रकार, ब्राह्मण को 2 प्रतिशत, क्षत्रिय को 3 प्रतिशत, वैश्य को 4 प्रतिशत और शूद्र को 5 प्रतिशत का ब्याज भुगतान करना पड़ता था। शूद्र मेहमानों को तभी खिलाया जाता था, जब वे मेजबान के घर कुछ काम करते थे। इन धर्मशास्त्रों के नियम निर्धारित थे, हो सकता है कड़ाई से उनका पालन नहीं किया जाता रहा हो लेकिन वे प्रमुख सामाजिक वर्षों द्वारा निर्धारित मानदण्डों के आदर्श की तरफ संकेत देते थे।
चूँकि पुजारी और योद्धा, दोनों ही करों, चुंगियों, दशमांश और किसानों एवं कारीगरों द्वारा दिए गए श्रमदान पर ही निर्भर थे, इसलिए उनके सम्बन्धों में हिस्सेदारी को लेकर अक्सर विवाद उत्पन्न हो जाते थे। ब्राह्मणों के दम्भ से क्षत्रिय भी आहत होते थे, जो समाज में सर्वश्रेष्ठता का दावा करते थे। हालाँकि, वैश्य और शूद्र के विरोध की स्थिति में दोनों अपना मतभेद भूल जाते थे। प्राचीन ग्रन्थों में बलपूर्वक उल्लेख है कि क्षत्रिय ब्राह्मणों के समर्थन के बिना समृद्ध नहीं हो सकते और क्षत्रियों के समर्थन के बिना ब्राह्मण समृद्ध नहीं हो सकते। दोनों एक साथ मिलकर विकास कर सकते थे और दुनिया में शासन कर सकते थे।
सामाजिक संकट और सामन्त वर्ग का उदय
कई शताब्दियों तक, गंगा के मैदानी और आस-पास के इलाके में इस सामाजिक व्यवस्था ने अच्छी तरह काम किया, जिसमें बड़े राज्यों का निरन्तर विकास हुआ। पहली और दूसरी शताब्दी में व्यापार और शहरीकरण का विकास इसकी विशेषता थी। इस चरण में, कला का भी अभूतपूर्व विकास हुआ। किन्तु तीसरी शताब्दी तक यह व्यवस्था पुरानी होकर लगभग अपने अवसान पर पहुँच चुकी थी जिससे इसका विकास रुक गया था। तीसरी शताब्दी के आस-पास पुरानी सामाजिक संरचना गहरे संकट से घिर गई। तीसरी और चौथी शताब्दी से सम्बन्धित पुराणों के कुछ हिस्सों में कलियुग के वर्णन में यह संकट स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। कलियुग को वर्णसंकर के माध्यम से दिखाया गया है, जिसका अर्थ है सामाजिक वर्षों या सामाजिक श्रेणियों का अन्तर्मिश्रण, जिसका तात्पर्य था, वैश्यों और शूद्रों (किसानों, कारीगरों और मजदूरों) द्वारा उत्पादन कार्य करने से इनकार। जिसमें वैश्य किसानों ने करों के भुगतान से और शूद्रों ने श्रम से इनकार कर दिया। उन्होंने शादी और अन्य प्रकार के सामाजिक सम्बन्धों के मामलों में वर्ण सीमाओं को मानने से इनकार कर दिया। ऐसी परिस्थिति में, महाकाव्यों में दण्ड या कठोर उपाय के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया और मनु ने कहा कि वैश्य और शूद्रों को उनके निर्धारित कर्तव्यों से नहीं हटने देना चाहिए। राजा का यह कर्तव्य है कि वर्ण व्यवस्था का पालन करवाए और संरक्षण करे।
हालाँकि, सिर्फ कठोर उपाय ही किसानों से कर वसूलने और मजदूरों से काम लेने के लिए पर्याप्त नहीं थे। अपने अधिकारियों के माध्यम से सीधे कर-संग्रह करने और उसके बाद उन्हें पुरोहित, सैन्य और अन्य कर्मचारियों एवं समर्थकों के बीच वितरित करने के बजाय, राज्य ने अपने रख-रखाव के लिए, भूमि राजस्व संचय का कार्य पुजारियों, सेनाओं, प्रमुखों, प्रशासकों को सौंपना ज्यादा सरल समझा। यह व्यवस्था वैदिक प्रथा के बिलकुल विपरीत थी। पहले, पुजारियों को, तथा सम्भवतः अपने प्रमुखों एवं शासकों को, भूमि देने का अधिकार केवल समुदाय को था। अब राजा ने इस शक्ति का अधिग्रहण कर लिया। और वे अपने प्रमुख सदस्यों को भूमि देकर अपना अनुग्रहित कर लिया। इसके साथ ही इन नए भूस्वामियों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने के अधिकार भी दे दिए गए। वित्तीय और प्रशासनिक समस्याओं का समाधान ऐसे ही किया जाता था। नए एवं विस्तृत होते राज्यों को स्वयं को बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक करों की आवश्यकता थी। जो कि पिछड़े कबीलाई क्षेत्रों से ही प्राप्त हो सकते थे। किन्तु यह तभी सम्भव था जब वे आदिवासियों को नए तकनीकी से कृषि करने के लिए प्रशिक्षित करें एवं राज्य के प्रति उनमें वफादारी सिखाई जाय। इस समस्या को सुलझाने की कोशिश उद्यमशील ब्राह्मणों को जनजातीय क्षेत्रों में भूमि देकर की गई, जहाँ वे जंगली इलाकों के निवासियों को इससे जोड़ते, उन्हें कृषि के बेहतर तरीके सिखाते और उन्हें अनुशासन के अनुकूल बनाते।
पिछड़े क्षेत्रों में, ब्राह्मणों और अन्य लोगों को भूमि अनुदान से कृषि का विस्तार हुआ, आयुर्वेद का ज्ञान फैला और इस प्रकार समग्र अनाज उत्पादन में वृद्धि हुई। लेखन की कला, प्राकृत एवं संस्कृत भाषा के उपयोग को प्रसारित किया गया। भूमि अनुदान के माध्यम से, सुदूर दक्षिण और पूर्व में सभ्यता का विस्तार हुआ, हालांकि व्यापारियों और जैनों एवं बौद्धों ने पहले ही इस दिशा में कुछ प्रारम्भिक कार्य किए थे। ब्राह्मणों को भूमि दिए जाने से बड़ी संख्या में किसानों की गिनती शूद्रों में होने लगी। इसलिए प्रारम्भिक मध्ययुगीन ग्रन्थों में शूद्रों को किसानों के रूप में जाना जाने लगा। हालाँकि, वैश्यों ने, विशेष रूप से विकसित क्षेत्रों के, स्वतन्त्र किसानों का दर्जा खो दिया। इसलिए उत्तरवतीं गुप्त काल में, आर्थिक और सामाजिक रूप से वैश्य और शूद्र के बीच का अन्तर कम हो गया। भूमि अनुदान का सबसे महत्त्वपूर्ण परिणाम किसानों के उत्पादन पर जीने वाले जमीन्दारों के एक वर्ग का उदय था। आगे चलकर प्राचीन भारतीय समाज में ऐसी स्थितियाँ बन गई कि पाँचवीं-छठी शताब्दियों तक यह एक नए प्रकार के सामाजिक निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ जिसे सामन्ती व्यवस्था कहा जा सकता है।
सामन्ती व्यवस्था में, जमीन्दारों और क्षत्रिय वर्गों की महिलाओं की स्थिति और ज्यादा खराब होती गई। प्रारम्भिक मध्यकाल में, राजस्थान में सती होना एक सामान्य प्रथा बन गई। हालाँकि, निम्न वर्ण की महिलाएँ आर्थिक गतिविधियों और पुनर्विवाह के लिए स्वतन्त्र थीं।
सारांश
सामाजिक शक्तियों के बदलाव को ध्यान में रखते हुए प्राचीन भारत में समाज को कोई एक नाम देना सम्भव नहीं है और हमें इसके विकास के कई चरणों के बारे में सोचना होगा। पाषाणकाल के भोजन संग्रह करने वाले समाज के बाद नवपाषाण और ताम्रपाषाण युग के खाद्य उत्पादक समुदायों का विकास हुआ। अन्ततः कृषक समुदाय हड़प्पा के शहरी समाज में तब्दील हो गया। इसके एक अन्तराल के बाद घोड़े का इस्तेमाल करने वाले और पशुपालक समाज दिखते हैं। ऋग्वेद एक सामाजिक संरचना की ओर इंगित करता है जो काफी हद तक पशुचारक और कबीलाई है। उत्तरवर्ती वैदिक काल में पशुचारक समाज कृषक समाज बन गया, लेकिन कृषि के अपने प्राचीन तरीकों के कारण, शासकों को किसानों से ज्यादा वसूली नहीं मिल पाई। उत्तरवर्ती वैदिक काल में वर्ग-विभाजित समाज पूरी तरह उभरा जिसे वर्ण व्यवस्था के रूप में जाना गया। यह सामाजिक संरचना शूद्रों की सहायता पर निर्भर और वैश्यों के उत्पादन कार्यों पर आश्रित थी। आखिरकार, यह सामाजिक व्यवस्था बुद्ध काल से गुप्त काल तक चली। फिर आन्तरिक उथल-पुथल के कारण इसमें फिर बदलाव आया। पुजारियों और अधिकारियों के रख-रखाव के लिए उन्हें भूमि प्रदान की जाने लगी और धीरे-धीरे वहाँ किसानों एवं राज्य के बीच जमीन्दारों का एक वर्ग उभरा। इससे वैश्यों की स्थिति कमजोर हुई और वर्ण व्यवस्था में भी बदलाव आया।
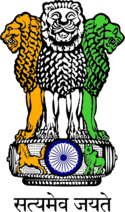
Alright, pk88betvn time to roll the dice! New place to test my luck, let’s see what happens. Check it out here: pk88betvn