एशियाई देशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध (प्राचीन भारत का इतिहास)
विश्व के अन्य देशों से भारत का सम्बन्ध
मध्ययुगीन नीति-निर्माताओं और विभिन्न टीकाकारों ने ने लिखा था कि किसी भी व्यक्ति को समुद्र पार नहीं जाना चाहिए। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि भारत बाहरी दुनिया के साथ सम्पर्क में नहीं रहा होगा। किन्तु यह पूर्णतया सत्य नहीं है, क्योंकि भारत ने हड़प्पा सभ्यता के समय से ही एशियाई पड़ोसी देशों के साथ सम्पर्क बनाए रखा था। भारतीय व्यापारी मेसोपोटामिया के शहरों में जाते थे, जहाँ उनकी मुहरें ई.पू. तीसरी शताब्दी के उत्तरार्ध में मिली हैं। ईस्वी सन् की शुरुआत होते-होते भारत ने चीन, दक्षिण-पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और रोमन साम्राज्य के साथ व्यावसायिक सम्पर्क बना लिए थे। इसके उदाहरण चीनी सिल्क रूट से भारतीय स्थल मार्ग के जुड़ाव और रोमन साम्राज्य के पूर्वी भाग के साथ व्यापारिक सम्बन्धों में देखा जा सकता है। भारत ने अपने धर्म प्रचारकों, विजेताओं और व्यापारियों को पड़ोसी देशों में भेजा, जहाँ पर उन्होंने विभिन्न प्रकार की बस्तियों की स्थापना कीं।
श्रीलंका, म्याँमार, चीन और मध्य एशिया में बौद्ध धर्म
बौद्ध धर्म के प्रसार ने श्रीलंका, म्याँमार, चीन और मध्य एशिया के साथ भारत के सम्पर्कों को बढ़ाने में मदद की। ई.पू. तीसरी शताब्दी में बौद्ध धर्म प्रचारकों को अशोक के शासनकाल में श्रीलंका भेजा गया था। जिसके साक्ष्य श्रीलंका में ई.पू. दूसरी और पहली शताब्दी से सम्बन्धित ब्राह्मी लिपि में लिखे गए लघु अभिलेखों में पाए जाते हैं। बाद में श्रीलंका, बौद्ध धर्म का स्थायी गढ़ बन गया। ईस्वी सन् की प्रारम्भिक शताब्दियों में, बौद्ध धर्म भारत से बर्मा (आधुनिक म्यांमार) तक फैला। बर्मा ने बौद्ध धर्म के थेरवाद रूप को विकसित किया और बुद्ध के सम्मान में कई मन्दिरों और मूर्तियों का निर्माण किया। इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण यह रहा कि, बर्मा और श्रीलंका के बौद्धों ने बौद्ध साहित्य के कई ग्रन्थो की रचना की। जो भारत में नहीं मिलता। सारे पाली ग्रन्थों और टिप्पणी साहित्य की रचनाएँ श्रीलंका में ही की गई। भले ही बौद्ध धर्म भारत से गायब ईसाई धर्म ने इसे पश्चिम एशिया के साथ सम्बन्ध मजबूत करने में योगदान दिया। छठी शताब्दी में, एलेक्जेण्ड्रिया के विद्वान कोस्मोस, भारत और श्रीलंका, दोनों जगह के ईसाई समुदाय के विस्तार के बारे में लिखते हैं। फारस से नियुक्त बिशप ने आधुनिक मुम्बई के निकट कल्याण के ईसाइयों की सेवा की थी। कहा जा सकता है कि पश्चिमी भारत में, ईसाई, जैन, बौद्ध और हिन्दू समुदायों एक साथ रहते थे।
दक्षिणपूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति
भारतीय संस्कृति भी दक्षिण पूर्व एशिया तक फैली, लेकिन बौद्ध धर्म के माध्यम से नहीं। बर्मा को छोड़कर यह ज्यादातर ब्राह्मणवादी सम्प्रदायों के माध्यम से फैला। बर्मा में पेगु और मौलमेनको सुवर्णभूमि को नाम दिया गया है। भड़ौच, बनारस और भागलपुर के व्यापारी बर्मा से कारोबार करते थे। बर्मा में गुप्त काल के बौद्ध अवशेष काफी संख्या में पाए गए हैं। पहली शताब्दी से भारत ने इण्डोनेशिया में जावा के साथ करीबी व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित किए, जिसे प्राचीन भारतीयों द्वारा सुवर्णद्वीप या सोने का द्वीप कहा जाता था। सन् 56 में जावा में सबसे पहले भारतीय बस्तियाँ ही स्थापित हुई थीं। दूसरी शताब्दी में, कई छोटे-छोटे भारतीय राज्य स्थापित किए गए। पाँचवीं शताब्दी में जब चीनी तीर्थयात्री फा-हियान ने जावा का दौरा किया, तो उन्हें वहाँ ब्राह्मणवादी संस्कृति का चलन दिखा। ईस्वी सन् की प्रारम्भिक शताब्दियों में, पल्लवों ने सुमात्रा में अपने उपनिवेशों की स्थापना की। अन्ततः यह श्री विजय राज्य के रूप में विकसित हुआ, जो पाँचवीं से दसवीं शताब्दी तक एक महत्त्वपूर्ण शक्ति और भारतीय संस्कृति का केन्द्र बना रहा। जावा और सुमात्रा में भारतीय बस्तियाँ, भारतीय संस्कृति के प्रसार का माध्यम बनीं। साथ में, नई बस्तियों को स्थापित करने का सिलसिला भी चलता रहा।
हिन्द-चीन में, जो वर्तमान में वियतनाम, कम्बोडिया और लाओस में विभाजित है, भारतीयों ने कम्बोज और चम्पा में दो शक्तिशाली राज्य स्थापित किए। आधुनिक कम्बोडिया के साथ कम्बोज के शक्तिशाली साम्राज्य को छठी शताब्दी में स्थापित किया गया था। इसके शासक शिव के भक्त थे। उन्होंने कम्बोज को संस्कृत सीखने के केन्द्र के रूप में विकसित किया, यहाँ कई अभिलेख संस्कृत भाषा में रचे गए।
कम्बोज के पड़ोस चम्पा में, व्यापारियों ने अपनी बस्तियाँ बसाई, जिसमें दक्षिणी वियतनाम तथा उत्तरी वियतनाम के तट शामिल हैं। चम्पा के राजा भी शैव थे और राजकीय भाषा संस्कृत थी। यह देश वेद और धर्मशास्त्रों की शिक्षा के लिए एक महान केन्द्र माना जाता था।
हिन्द महासागर में तेरहवीं शताब्दी तक भारतीय बस्तियों का बसना जारी रहा और इस अवधि के दौरान, भारतीय लोग यहाँ के निवासियों और स्थानीय लोगों के साथ घुल-मिल गए। जिससे एक नए प्रकार की कला, भाषा और साहित्य का जन्म हुआ। हम इन देशों में ऐसी कई कला की वस्तुएँ देखते हैं, जो भारतीय और स्वदेशी दोनों तत्त्वों के मिश्रित स्वरूप को दर्शाती हैं। यह भी आश्चर्यजनक ही है कि सबसे बड़ा बौद्ध मन्दिर भारत में नहीं, बल्कि जावा के बोरोबुदुर में है। दुनिया में सबसे बड़ा माना जाने वाला, यह बौद्ध मन्दिर आठवीं शताब्दी में निर्मित किया गया था और इस पर उत्कीर्ण बुद्ध के 436 चित्र उनके पूरे जीवन को दर्शाते हैं।
कम्बोडिया में अन्कोरवाट का मन्दिर बोरोबुदुर से बड़ा है। यद्यपि यह मन्दिर मध्ययुगीन काल का है, लेकिन इसकी तुलना मिस्त्र और यूनानियों की सर्वोत्तम कलात्मक उपलब्धियों से की जा सकती है। मन्दिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत की कहानियाँ उभरी हुई मूर्तियों में उकेरी गई हैं। रामायण की कहानी इण्डोनेशिया में इतनी लोकप्रिय है कि इस पर आधारित कई लोक नाटक किए जाते हैं। इण्डोनेशिया की भाषा, बहासा इण्डोनेशिया में कई संस्कृत के शब्द मिलते हैं।
सांस्कृतिक आदान-प्रदान
मूर्तिकला के सम्बन्ध में, थाईलैण्ड एवं कम्बोज से उपलब्ध बुद्ध के सिर और जावा की शानदार काँस्य प्रतिमाएँ, दक्षिण-पूर्व एशिया की स्थानीय कला परम्पराओं के साथ भारतीय कला के संगम के सर्वोत्तम उदाहरण माने जाते हैं। इसी तरह चित्रकारी के सुन्दर उदाहरण, जिनकी तुलना अजन्ता की चित्रकारी से की जाती है न केवल श्रीलंका, बल्कि चीनी सीमा पर टुं हुंग गुफाओं में भी पाए जाते हैं।
यह सोचना गलत होगा कि अकेले धर्म ने भारतीय संस्कृति के प्रसार में योगदान दिया। धर्म प्रचारकों को व्यापारियों और विजेताओं का समर्थन प्राप्त था। व्यापार ने स्पष्ट रूप से मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत के सम्बन्धों को स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। दक्षिणपूर्व एशिया में प्रदेशों को दिए जाने वाले नाम सुवर्णभूमि और सुवर्णद्वीप हैं, जो भारतीयों द्वारा सोने की खोज का संकेत देते हैं। व्यापार ने न केवल वस्तुएँ बल्कि सांस्कृतिक तत्त्वों का भी आदान-प्रदान हुआ। यह मानना गलत होगा कि अकेले भारतीयों ने अपने पड़ोसियों की संस्कृतिक विकास में योगदान दिया; बल्कि ऐसा दोनों तरफ से हुआ। भारतीयों ने यूनानियों और रोम से सोने के सिक्कों के ढाँचे लिए, चीन से रेशम उगाने की कला ली, इण्डोनेशिया से पान के पत्ते उगाने की कला सीखी और पड़ोसी देशों के कई अन्य उत्पादों को अपनाया। तो दूसरी तरफ, कपास उगाने की विधि भारत से चीन और मध्य एशिया तक फैली। हालाँकि, कला, धर्म, लिपि और भाषा में भारतीय योगदान महत्त्वपूर्ण रहा। फिर भी, पड़ोसी देशों में जो संस्कृति विकसित हुई, वह भारतीय संस्कृति की प्रतिकृति नहीं थी। जैसे भारत ने विदेशी प्रभावों के बावजूद अपनी मूल पहचान को सुरक्षित और विकसित किया, उसी तरह, दक्षिण पूर्व एशिया में प्रत्येक देश ने अपने स्वदेशी तत्त्वों के साथ भारतीय तत्त्वों को सम्मिलित करते हुए अपनी विशिष्ट संस्कृति का विकास किया।
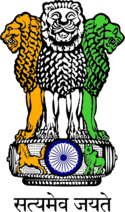
Alright, 33win39bet’s not bad ya know. Got a decent selection of stuff to bet on. Could be better, but it’s solid. Give it a shot if you’re looking for something new 33win39bet