दर्शन का विकास (प्राचीन भारत का इतिहास)
जीवन का लक्ष्य
जब राज्य और वर्णभेद आधारित सामाजिक व्यवस्था मजबूती से स्थापित हो गए तो प्राचीन विचारकों ने व्यक्ति को चार लक्ष्यों की प्राप्ति का सन्देश दिया। ये नियम थे-सामाजिक व्यवस्था का अनुपालन, अर्थात् धर्म, आर्थिक संसाधनों का प्रबन्धन, अर्थात् अर्थ, शारीरिक सुख, अर्थात् काम, और मुक्ति क मार्ग, अर्थात् मोक्ष। इन सभी उद्देश्यों को लिखित रूप में समझाया गया। अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित मामले कौटिल्य रचित प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र में हैं। राज्य और समाज संचालन की व्यवस्था धर्मशास्त्र के विषय बन गए और शारीरिक सुख यानि काम पर चर्चा कामसूत्र में हुई। ज्ञान की ये तीनों शाखाएँ प्राथमिक रूप से भौतिक दुनिया और इसकी समस्याओं से सम्बन्धित थीं, इनमें मुक्ति के सवाल को कभी नहीं छुआ गया। इसलिए मोक्ष या मुक्ति दर्शन ग्रन्थों का मुख्य विषय बन गया। इसका मतलब जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति है, जिस पर पहली बार गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया और बाद में कुछ ब्राह्मणवादी दार्शनिकों ने इसे आगे बढ़ाया।
ईस्वी सन् की शुरुआत तक, दर्शन की छह शाखाएँ विकसित हो चुकी थीं। इन्हें सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदान्त के रूप में जाना जाता था।
सांख्य
सांख्य, जिसका अर्थ ‘संख्या या गिनती’ होता है, पहले उत्पन्न हुआ लगता है। प्रारम्भिक सांख्य दर्शन के अनुसार, दुनिया के निर्माण के लिए दिव्य शक्ति आवश्यक नहीं है। दुनिया के निर्माण का श्रेय भगवान की तुलना में प्रकृति को अधिक जाता है। यह तर्कसंगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। चौथी शताब्दी के आस-पास प्रकृति के अलावा पुरुष या आत्मा को सांख्य प्रणाली में एक तत्त्व के रूप में पेश किया गया और दुनिया का निर्माण इन दोनों से मिलकर बताया गया। नए दृष्टिकोण के अनुसार, प्रकृति और आध्यात्मिक तत्त्व एक साथ दुनिया का निर्माण करते हैं। इस प्रकार, शुरुआत में दर्शन की सांख्य शाखा भौतिकवादी थी, लेकिन बाद में यह अध्यात्मवादी बन गई। प्रारम्भ में, इस शाखा के अनुसार, एक व्यक्ति वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति के माध्यम से उद्धार प्राप्त कर सकता है और उसका दुःख हमेशा के लिए समाप्त हो सकता था। इस ज्ञान को अनुभूति (प्रत्यक्ष), अवधारणा (अनुमान), और श्रवण (शब्द) के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। आज यहीं तीनों तरीके आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति की भी विशेषताएँ है।
योग
योग शाखा के अनुसार, एक व्यक्ति ध्यान और शारीरिक व्यायाम के माध्यम से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों पर नियन्त्रण का अभ्यास इस प्रणाली का मूल आधार है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए, विभिन्न मुद्राओं में शारीरिक व्यायाम किया जाता है, जिसे आसन कहते हैं और श्वास व्यायाम को प्राणायाम कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन तरीकों के माध्यम से, मन सांसारिक मामलों से दूर हटकर एकाग्रचित्त होता है। ये अभ्यास महत्त्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये न केवल प्राचीन काल में शरीर विज्ञान और शरीर रचना विज्ञान के ज्ञान के कुछ विकास की कल्पना करते हैं, बल्कि ये सांसारिक कठिनाइयों से दूर होने की प्रवृत्ति को भी दर्शाते हैं।
न्याय
न्याय, या विश्लेषण की शाखा, तर्क की एक प्रणाली, तर्कशास्त्र के रूप में विकसित हुई। इसके अनुसार, ज्ञान प्राप्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इसमें सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है कि तर्क या कथन की सच्चाई का परीक्षण अनुमान, श्रवण (शब्द), और सादृश्यानुमान या उपमान से किया जा सकता है। उन्होंने तर्क का इस्तेमाल निम्नांकित पद्धति से किया :
1. पहाड़ में आग है
2. क्योंकि वहाँ धुआँ है;
3. जहाँ-जहाँ धुआँ होता है, वहाँ-वहाँ आग होती है।
इस दर्शन में तर्क के उपयोग पर बल दिया गया, जिससे भारतीय विद्वान भी प्रभावित होकर व्यवस्थित और तार्किक सोच एवं विमर्श पर ध्यान दिए।
वैशेषिक
वैशेषिक शाखा भौतिक तत्त्वों या द्रव्य की चर्चा को महत्त्व देता है। वे विशेष और सामान्य के बीच एक रेखा खींचते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और गगन (आकाश) मिलकर नई वस्तुओं को जन्म देते हैं। वैशेषिक शाखा ने परमाणु सिद्धान्त की स्थापना की। इसने माना कि सभी भौतिक वस्तुएँ परमाणु से बनी होती हैं। इस प्रकार वैशेषिक ने ही भारत में भौतिकी की शुरुआत की, लेकिन यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ईश्वर और अध्यात्मवाद में विश्वास के कारण कमजोर पड़ गया और बाद में इस शाखा ने स्वर्ग और मुक्ति दोनों को माना।
भीमांसा
मीमांसा का शाब्दिक अर्थ है तर्क और व्याख्या की कला। यहाँ विभिन्न वैदिक अनुष्ठानों को जायज सिद्ध करने के लिए तर्क का इस्तेमाल किया जाता था और मुक्ति की प्राप्ति उनके प्रदर्शन पर निर्भर था। मीमांसा शाखा के अनुसार, वेदों में ही शाश्वत सत्य है। इस दर्शन का मुख्य उद्देश्य स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करना था। एक व्यक्ति अपने कमाए गए पुण्यों के हिसाब से ही स्वर्ग प्राप्ति का आनन्द लेता है। जब उसके अर्जित पुण्य समाप्त हो जाते हैं, तो वह पृथ्वी पर लौट आता है। किन्तु अगर वह मुक्ति प्राप्त करता है, तो वह दुनिया में जन्म और मृत्यु के चक्र से पूरी तरह मुक्त हो जाता है।
मीमांसा शाखा ने मोक्ष प्राप्त करने के लिए, वैदिक यज्ञ का समर्थन किया, जिसके लिए पुजारियों की सेवा करना और विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक स्तर बनाए रखना आवश्यक था। मीमांसा दर्शन के प्रचार के माध्यम से, ब्राह्मणों ने धार्मिक अनुष्ठानों में अपने अधिकार और ब्राह्मण प्रधान सामाजिक स्तरीकरण को बनाए रखने की कोशिश की।
वेदान्त
वेदान्त का अर्थ है वेद का अन्त। ई.पू. दूसरी शताब्दी में संकलित बादरायण का ब्रह्मसूत्र इस दर्शन का मूल आधार ग्रन्थ है। बाद में, इस पर दो प्रसिद्ध टीकाएँ भी लिखी गईं, पहला नौवीं शताब्दी में शंकर द्वारा और दूसरा बारहवीं शताब्दी में रामानुज द्वारा। शंकर ने ब्रह्म को किसी विशेष गुण से रहित माना, लेकिन रामानुज के ब्रह्म गुण सम्पन्न हैं। शंकर ने ज्ञान को मुक्ति का मुख्य साधन माना, लेकिन रामानुज की मुक्ति का मार्ग भक्ति/प्रेम विश्वास का अभ्यास है।
वेदान्त दर्शन का मूल प्राचीन उपनिषदों में मिलता है। इसके अनुसार, ब्रह्म ही सत्य है और बाकी सब कुछ माया है। आत्मा और ब्रह्म अभेद हैं। इसलिए, यदि किसी व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है, तो उसे ब्रह्म का ज्ञान भी प्राप्त होता है और वह अन्ततः मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म और आत्मा दोनों ही शाश्वत और अविनाशी हैं। ऐसे दृष्टिकोण से स्थिरता और अपरिवर्तन के विचार को बढ़ावा मिलता है। जो आध्यात्मिक रूप से सत्य है, वही किसी व्यक्ति के लिए सामाजिक और भौतिक स्थिति में भी सत्य हो सकता है।
कर्म का सिद्धान्त वेदान्त दर्शन से जुड़ा हुआ था। इसका अर्थ है कि अपने वर्तमान जन्म में एक व्यक्ति को अपने पूर्वजन्म में किए गए कार्यों के परिणाम भुगतने पड़ते हैं। पुनर्जन्म में विश्वास न केवल वेदान्त प्रणाली में, बल्कि हिन्दू दर्शन की कई अन्य प्रणालियों में भी महत्त्वपूर्ण बन गया। इसका अर्थ है कि लोग सामाजिक या सांसारिक कारणों से नहीं, बल्कि उन अनभिज्ञ कारणों से ग्रस्त होते हैं, जिन्हें वे न तो जानते हैं और न ही नियन्त्रित कर सकते हैं।
चार्वाक और जीवन के भौतिक विचार
दार्शनिक शिक्षा की छह शाखाओं ने जीवन के आदर्शवादी दृष्टिकोण को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया। वे सभी मोक्ष प्राप्ति के रास्ते बन गए। सांख्य और वैशेषिक शाखाओं ने जीवन के भौतिक विचारों को समृद्ध किया। सांख्य के सबसे मूल प्रवर्तक कपिल के अनुसार व्यक्ति का जीवन प्राकृतिक शक्तियों से निर्मित होता है न कि किसी दैवीय शक्ति से। इसी प्रकार भौतिक विचार का वर्णन बुद्ध के समय में भी एक असनातनी/नास्तिक सम्प्रदाय आजीवक के सिद्धान्तों में किया गया है। हालाँकि, भौतिकवादी दर्शन के मुख्य प्रतिपादक चार्वाक हुए। और उनके इस दर्शन को लोकायत के रूप में जाना जाने लगा, जिसका अर्थ है आम लोगों से प्राप्त विचार। इसमें वर्तमान दुनिया (लोक) के साथ गहरे सम्बन्ध के महत्त्व पर बल दिया गया और दूसरी दुनिया यानि परलोक में अविश्वास दिखाया गया। चार्वाक को कई शिक्षाओं का श्रेय जाता है। वे आध्यात्मिक मोक्ष प्राप्ति के विरोधी थे। उन्होंने किसी भी दिव्य या अलौकिक शक्ति के अस्तित्व/वास्तविकता को नहीं स्वीकारा। उन्होंने केवल उन्हीं चीजों के अस्तित्व को स्वीकार किया, जिसे इन्द्रियों और अंगों द्वारा मानव अनुभव कर सके। वे ब्रह्म और ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे। चार्वाक के अनुसार, ब्राह्मणों ने उपहार (दक्षिणा) प्राप्त करने के लिए अनुष्ठानों का निर्माण किया। चार्वाक को बदनाम करने के लिए, उनके विरोधियों ने उनके केवल इस मत को खूब प्रचारित किया कि व्यक्ति को जीवन भर आनन्द लेना चाहिए; चाहे उधार लेकर ही सही, मगर अच्छा भोजन (घी) करना चाहिए। हालाँकि, चार्वाक का असली योगदान उनके भौतिकवादी दृष्टिकोण में निहित है। वे दिव्य और अलौकिक शक्तियों को नकार कर मानव को सारे गतिविधियों का केन्द्र मानते थे।
ई.पू. 500 और सन् 300 के बीच विस्तृत अर्थव्यवस्था और समाज में भौतिकवादी दर्शन पर बल दिया गया। जब गंगा के मैदानों पर बसावट एवं दिन-प्रतिदिन की जीवनचर्या में प्रकृति प्रदत्त कठिनाइयों के साथ संघर्ष करने में लौह आधारित कृषि प्रौद्योगिकी की उत्पत्ति और विकास हुआ। धातुओं की मुद्रा एवं व्यापार के साथ ही हस्तशिल्पों का उदय हुआ। नए पर्यावरण ने वैज्ञानिक और भौतिक दृष्टिकोण को जन्म दिया, जो मुख्यतः चार्वाक के दर्शन में परिलक्षित हुए हैं और अन्य कई पारम्परिक दार्शनिक धाराओं में भी पाए गए।
पाँचवीं शताब्दी तक, आदर्शवादी दर्शन के प्रतिपादकों ने भौतिकवादी दर्शन की खूब आलोचना की और अनुष्ठानों एवं आध्यात्मिकताओं के जरिए मोक्ष प्राप्ति पर बल दिया; उन्होंने अलौकिक शक्तियों को सांसारिक घटनाओं का कारण माना। इस विचार ने वैज्ञानिक जाँच और तर्कसंगत सोच की प्रगति को रोक दिया। यहाँ तक कि प्रबुद्ध वर्ग के लिए भी पादरियों और क्षत्रियों के विशेषाधिकारों पर सवाल करना मुश्किल हो गया। आदर्शवादी और मोक्षवादी दर्शन में घिरे लोगों का ध्यान वर्ण आधारित सामाजिक व्यवस्था की असमानताओं और राजा के प्रतिनिधित्व वाले राज्य की मजबूत सत्ता को नकारने की तरफ कभी नहीं गया।
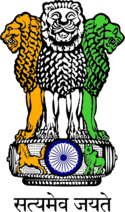
789pvip looks interesting, gotta say. Their VIP program seems enticing. Anyone here a member? Wanna hear your experiences with using 789pvip!