गुप्त काल में जनजीवन (प्राचीन भारत का इतिहास)
शासन प्रणाली
मौर्य शासकों के विपरीत, गुप्त राजवंशों ने परमेश्वर, महाराजाधिराज और परमभट्टारक मौ || जैसी आडंबरयुक्त उपाधियाँ अपनाईं। जिनसे यह विदित होता है कि उन्होंने अपने साम्राज्य में कई छोटे-छोटे राजाओं पर शासन किया। राजपद वंशानुगत था, लेकिन राजशाही में ज्येष्ठाधिकार के दृढ़ अनुपालन की कमी थी। उत्तराधिकार हमेशा सबसे बड़े पुत्र को नहीं दिया जाता था, इस कारण अनिश्चितता व्याप्त रहती थी। जिसका लाभ प्रमुख एवं उब्ब अधिकारियों को मिल सकता था। गुप्त शासक ब्राह्मणों को भरपूर उपहार देते थे। फलस्वरूप वे देवताओं से राजाओं की तुलना करके अपना आभार व्यक्त करते थे। राजाओं को विष्णु, रक्षक, संरक्षक… देवता जैसा माना जाता था। धन की देवी लक्ष्मी नियमित रूप से गुप्त सिक्कों पर विष्णु की पत्नी के रूप में अंकित होती रही। गुप्त सेना का संख्या बल ज्ञात नहीं है। राजा के पास अपनी एक स्थायी सेना होती थी, जिसमें कभी-कभी सामन्तों की सेनाएँ भी शामिल होती थीं। घोड़े वाले रथों का प्रचलन कम हो गया था। घुड़सवार सेना की महत्ता बढ़ने लगी थी। अब तक सैन्य रणनीति में घोड़े पर से तीरन्दाजी महत्त्वपूर्ण तत्त्व बन गई थी।
गुप्त काल में भूमि करों की संख्या बढ़ गई, जबकि व्यापार और वाणिज्य में करों की संख्या घटी। सम्भवतः राजा ने कृषि उपज का एक चौथाई से लेकर छठे हिस्से तक का कर वसूला। इसके अलावा, जब भी शाही सेना ग्रामीण इलाकों से गुजरती तो स्थानीय लोगों को उन सैनिकों को खिलाना-पिलाना पड़ता। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले राजकीय अधिकारियों के दैनिक उपयोग की वस्तुएँ जैसे पशु, अनाज, फर्नीचर आदि की आपूर्ति भी किसानों को ही करनी पड़ती थी। इसके अतिरिक्त मध्य और पश्चिमी भारत में, ग्रामीणों को राजकीय सेना एवं अधिकारियों की सेवा भी, निःशुल्क रूप से करनी पड़ती थी, ऐसे मजदूर विष्टि कहलाते थे।
पहले की तुलना में गुप्त काल में न्यायिक व्यवस्था अधिक विकसित थी। इस अवधि के दौरान कई विधि ग्रंथ रचे गए। पहली बार दीवानी और फौजदारी कानून स्पष्ट रूप से अलग-अलग परिभाषित किए गए। चोरी और व्यभिचार, फौजदारी कानून के अधीन आते थे और विभिन्न प्रकार के सम्पत्ति विवाद से सम्बन्धित मामले दीवानी कानून के अधीन आते थे। उत्तराधिकार से प्राप्त सम्पत्ति के बारे में विस्तृत कानून निर्धारित किए गए। चूंकि प्राचीन समय में कई कानून वर्ण विभेद पर आधारित थे इसलिए इन कानूनों का आधार भी वर्ण भेद ही रहा और कानूनों को बनाए रखना एवं ब्राह्मण पुजारियों की सहायता से मामलों की सुनवाई करना राजा का दायित्व माना जाता था। कारीगरों, व्यापारियों और अन्य लोगों के संगठन, स्वयं निर्मित अपने कानूनों द्वारा संचालित होते थे। वैशाली एवं इलाहाबाद के निकट स्थित भीटा से प्राप्त मुहरों से यह संकेत मिलता है कि गुप्त काल के दौरान ऐसे संगठन समृद्ध अवस्था में थे।
गुप्त काल का अधिकारी वर्ग मौर्यों की तरह बड़ा नहीं था। गुप्त साम्राज्य के सबसे महत्त्वपूर्ण अधिकारी कुमारामात्य होते थे। उन्हें अपने प्रान्तों में ही राजा द्वारा नियुक्त किया जाता था इसके लिए सम्भवतः उन्हें नकद भुगतान होता था। चूँकि गुप्त शायद वैश्य थे, इसलिए प्रशासनिक भर्ती केवल उच्च वर्णों तक ही सीमित नहीं थी, लेकिन कई कार्यालयों का दायित्व एक ही व्यक्ति को सौंप दिया जाता था जिससे आगे चलकर यह पद वंशानुगत हो गए, परिणामस्वरूप राजकीय नियन्त्रण स्वाभावतः कमजोर होता गया।
गुप्तों ने प्रान्तीय और स्थानीय शासन की एक प्रणाली बनाई। साम्राज्य को मण्डलों में विभाजित किया जाता था, जिसे भुक्ति कहा जाता था। हर भुक्ति को एक-एक उपरिक के प्रभार में रखा जाता था। ये भुक्तियाँ जिलों (विषयों) में विभाजित होती थीं और प्रत्येक जिले या विषय का प्रभारी विषयपति होता था। पूर्वी भारत में, इन विषयों को कई वीथियों में विभाजित किया जाता था, वीथियाँ फिर गाँवों में उप-विभाजित होती थीं।
गुप्त काल में गाँव के मुखिया का महत्त्व बढ़ गया, वह ग्राम के बड़ों-बुजुर्गों की सहायता से ग्रामीण मामलों को सुलझाते थे। गाँव या छोटे शहर के प्रशासन से, प्रमुख स्थानीय लोग जुड़े होते थे। उनकी सहमति के बिना भूमि का कोई भी लेन-देन नहीं किया जा सकता था।
नगरीय प्रशासन में, संगठित व्यावसायिक निकाय या संगठन महत्त्वपूर्ण होते थे। वैशाली के मुहरों से पता चलता है कि कारीगर, व्यापारी और संगठन के प्रमुख एक ही निगमित निकाय के अन्तर्गत काम करते थे, जिसके तहत वे स्पष्टतः शहरी मामले सुलझाते थे। उत्तरी बंगाल (बांग्लादेश) के कोटिवर्षा जिले के प्रशासनिक बोर्ड में मुख्य व्यापारी, मुख्य बिक्रेता और मुख्य कारीगर शामिल होते थे। भूमि की लेन-देन के लिए उनकी सहमति आवश्यक होती थी। कारीगर और बैंक कर्मियों के अपने अलग-अलग संगठन होते थे। भीटा और वैशाली में कारीगरों, व्यापारियों आदि के कई संगठनों के बारे में सुना गया है। मालवा के मन्दसौर में तथा इन्दौर में रेशम बुनकरों के अपने संगठन थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर जिले में, तेल निकालने वाले, तेलियों के अलग संगठन होते थे। ऐसा लगता है कि इन संगठनों को कुछ छूट एवं सुविधाएँ प्राप्त थीं, विशेष रूप से व्यापारियों के संगठनों को। ये संगठन अपने सदस्यों की देखभाल करते थे और संगठन के कानूनों और रीति-रिवाजों का उल्लंघन करने वालों को दण्डित भी करते थे।
प्रशासन की उल्लिखित व्यवस्था केवल उत्तर बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ आस-पास के इलाकों में थी, जहाँ गुप्त राजाओं द्वारा नियुक्त अधिकारी शासन करते थे। साम्राज्य का प्रमुख हिस्सा सामन्ती प्रमुखों के अधिकार क्षेत्र में था, जिनमें से कइयों को समुद्रगुप्त ने अपने अधीन कर लिया था। साम्राज्य से दूर सीमावर्ती सामन्तों को तीन दायित्व दिए गए थे। अधीनस्थ शासकों के रूप में, वे महाराज के दरबार में स्वयं उपस्थित होकर निवेदन कर सम्मान दिखाते, नजराना पेश करते और विवाह हेतु उन्हें अपनी बेटियाँ प्रस्तुत करते थे। प्रतीत होता है कि इसके बदले उन्हें अपने इलाकों पर शासन का विशेषाधिकार के रूप में प्राप्त होता था। इन सामन्तों को गरुड़ चिह्नित शाही मुहर जारी की जाती थी। इस प्रकार मध्य प्रदेश एवं अन्य क्षेत्रों के अधीनता स्वीकार कर चुके शासकों को गुप्त नियन्त्रित करते थे।
ग्राम अनुदान के द्वारा पुजारियों एवं प्रशासकों को कर संग्रह एवं शासन करने की रियायत, गुप्त काल का दूसरा महत्त्वपूर्ण सामन्ती विकास है। यह प्रथा सातवाहनों द्वारा दक्कन में शुरू की गई थी, जिसे गुप्त के समय काल में, विशेष रूप से मध्य प्रदेश में, नियमित बना दिया गया। धार्मिक कार्यकर्ताओं और पुरोहितों के लिए कर-मुक्त भूमि दी गई और जो कर सीधे राजा को दिए जाते थे, किसानों से उसकी वसूली का अधिकार उन्हें दिया गया। इन दिए गए गाँवों में कोई शाही अधिकारी, प्रशासक या अन्य, कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। यहाँ अपराधियों को दण्डित करने का भी अधिकार इन्हीं पुरोहितों के पास था।
गुप्त काल में अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि मिलती थी या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। किन्तु उत्खनन से प्राप्त सोने के सिक्कों की प्रचुरता का अर्थ है कि उच्च अधिकारियों को वेतन नकद भुगतान द्वारा ही किया जाता रहा होगा। जिनमे से कुछ को भूमि भी दी जाती होगी।
अधिकतर राजकीय प्रशासन चूँकि सामन्तों एवं अनुदानभोगियों की देख-रेख में होता था, इसलिए गुप्त शासकों को मौर्यों की तरह अधिक अधिकारियों की आवश्यकता नहीं होती थी; मौर्य साम्राज्य की तरह गुप्त साम्राज्य में किसी बड़े पैमाने पर आर्थिक गतिविधियाँ भी नहीं होती थीं। ग्रामीण और शहरी प्रशासन में अग्रणी कारीगरों, व्यापारियों, बुजुर्गों और अन्य लोगों की भागीदारी से बड़ी संख्या में अधिकारियों की आवश्यकता को कम कर दिया। इसीलिए गुप्तों का मौर्यों की तरह विस्तृत प्रशासनिक तन्त्र नहीं था और न ही इसकी जरूरत। कहा जा सकता है कई मायनों में उनकी राजनीतिक व्यवस्था सामन्ती थी।
व्यापार और कृषि अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति
गुप्त काल के लोगों के आर्थिक जीवन की कुछ जानकारी हमें चीनी बौद्ध यात्री फा-हियान से मिलती है, जिन्होंने गुप्त साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया था। चीनी यात्री हमें बतलाता है कि मगध सम्पन्न शहरों का राज्य था; वहाँ के लोग अमीर थे और बौद्ध धर्म के संरक्षण के लिए दान देते थे।
प्राचीन भारत में, गुप्तों ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए, जिन्हें उनके अभिलेखों में दीनार कहा जाता था। एक ही आकार और वजन के सिक्कों के कई प्रकार और उप-प्रकार होते थे। उनमें गुप्त राजाओं के युद्ध और कला प्रेम को चित्रित किया गया था। हालाँकि गुप्त काल के सिक्के कुषाणों के सिक्कों से कम शुद्ध थे, जिसका इस्तेमाल वे सेना और प्रशासन के अधिकारियों को भुगतान के साथ-साथ जमीन की खरीद-बिक्री के लिए भी करते थे। गुजरात विजय के बाद, स्थानीय विनिमय के लिए गुप्तों ने बड़ी संख्या में चाँदी के सिक्के भी जारी किए, क्योंकि चाँदी के सिक्कों का विनिमय पश्चिमी क्षत्रपों के मध्य बहुतायत में होता था। कुषाणों की तुलना में, गुप्त काल के ताम्र सिक्कों की संख्या बहुत कम है। इससे यह संकेत मिलता है कि कुषाण काल की तरह गुप्त काल के आम लोग पैसों का इस्तेमाल कम करते थे।
पहले के मुकाबले इस दौरान लम्बी दूरी के व्यापार में गिरावट आई। सन् 550 तक भारत ने पूर्वी रोम या बाइजेण्टाइन साम्राज्य के साथ कुछ व्यापार किए, जिसमें ये रेशम का निर्यात करते थे। सन् 550 के आस-पास, पूर्वी रोम साम्राज्य के लोगों ने चीनियों से रेशम उत्पादन की कला सीखी, जिससे भारतीय निर्यात व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। छठी शताब्दी के मध्य में भी, विदेशों में भारतीय रेशम की माँग में कमी आई। पाँचवीं शताब्दी के मध्य में, रेशम बुनकरों के एक दल ने पश्चिमी भारत के गुजरात की लता राज्य में अपना घर छोड़ दिया और मालवा के मन्दसौर चले गए, जहाँ उन्होंने अपना मूल व्यवसाय छोड़कर दूसरे व्यवसाय अपना लिए।
गुप्त काल में स्थानीय किसानों की जगह पुरोहित जमीन्दारों का उद्भव आश्चर्यजनक घटना थी। जिसका मुख्य केन्द्र पूर्वी और केन्द्रीय मध्य प्रदेश रहा। पुरोहितों को दिए गए भूमि अनुदान से बंजर पड़ी नई जमीनों पर भी कृषि की शुरुआत हुई, लेकिन इन्हें ऊपर से स्थानीय किसानों के ऊपर जबरन थोपा गया था, जिससे किसानों का स्तर काफी नीचे चला गया। मध्य और पश्चिम भारत में, किसानों को बन्धुआ मजदूर बनाए जाने के भी साक्ष्य मिलते हैं। इसके बावजूद इस प्रक्रिया में व्यापक स्तर पर परती जमीनों को कृषियुक्त बनाया गया, ब्राह्मण लाभार्थियों द्वारा मध्य भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि के नए ज्ञान का इस्तेमाल और प्रचार किया गया।
सामाजिक विकास
गुप्त काल में ब्राह्मणों को बड़े पैमाने पर दी गई भूमि से ब्राह्मण वर्चस्व की वृद्धि का अंदाजा लगाया जा सकता है। गुप्त मूल रूप से वैश्य थे, जिन्हें ब्राह्मणों ने क्षत्रिय कहना शुरू किया और गुप्त राजाओं को भगवान के रूप में प्रस्तुत किया। इससे गुप्त राजकुमारों को धर्मसम्मत वैधता में मदद मिली और वे वर्ण व्यवस्था के बड़े समर्थक एवं प्रतिपालक बन गए। ब्राह्मणों ने अनुदान से मिली जमीनों के माध्यम से अकूत सम्पत्ति जमा कर ली और इसलिए उन्हें कई विशेषाधिकार भी मिले। जिसका उल्लेख पाँचवीं शताब्दी में रचित नारद के विधान-ग्रन्थ नारद-स्मृति में है।
वर्ण कई जातियों-उपजातियों में बंट गए, जिसके दो कारण थे। बड़ी संख्या में आए विदेशी लोग भारतीय समाज में ही घुल-मिल गए, जिससे विदेशियों के प्रत्येक समूह अलग-अलग जाति बन गए। चूंकि विदेशी बडे पैमाने पर विजेता के तौर पर आए थे इसलिए उन्हें समाज में क्षत्रिय का दर्जा दिया गया। पाँचवीं शताब्दी के करीब भारत आए हूण समूह को अन्ततः राजपूतों के छत्तीस वंशों में से एक मान लिया गया। आज भी कुछ राजपूत हूण उपाधि धारण करते हैं। जातियों की संख्या में वृद्धि का दूसरा कारण भूमि अनुदान के माध्यम से कई जनजातीय लोगों को ब्राह्मण समाज में समावेशन था। इनके प्रमुखों को सम्मानजनक स्थान दिया गया था, लेकिन उनके अधिकांश रिश्तेदारों को निम्न माना गया था। फलतः प्रत्येक जनजाति अपने नए अवतार में एक प्रकार की जाति बन गई। यह प्रक्रिया वर्तमान समय में भी किसी न किसी रूप में चल रही है।
इस काल में शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ, उन्हें रामायण, महाभारत और पुराण सुनने की अनुमति मिल गई थी। महाकाव्यों और पुराणों में क्षत्रिय परम्परा का उल्लेख था, जिनके मिथकों और किंवदन्तियों ने सामाजिक व्यवस्था के प्रति निष्ठा स्थापित की। शूद्र भी कृष्ण नामक एक नए देवता की पूजा कर सकते थे; उन्हें कुछ घरेलू प्रथा को मनाने की अनुमति भी मिल गई थी; जिसमें स्वाभाविक रूप से पुजारियों को दक्षिणा देने का नियम जुड़ा था। सामाजिक स्थिति में सुधार, शूद्रों की आर्थिक स्थिति सुधरने का ही संकेत था। सातवीं शताब्दी से उनकी मुख्य पहचान कृषक की हो गई थी, इससे पहले, वे आम तौर पर नौकर, दास और कृषि श्रमिकों के रूप में तीन उच्च वर्णों के लिए काम करने वाले ही माने जाते थे।
हालाँकि, इस अवधि के दौरान, अछूतों की संख्या में वृद्धि हुई, विशेषकर चाण्डाल में। चाण्डाल को पाँचवीं शताब्दी में समाज में प्रवेश मिला। पाँचवीं शताब्दी तक, उनकी संख्या और अपात्रताएँ इतनी बढ़ गई कि चीनी तीर्थयात्री फा-हियान का इस तरफ ध्यान आकर्षित हुआ। वे लिखते हैं कि चाण्डाल गाँव के बाहर रहते थे और माँस बेचते /खाते थे। जब भी वे शहर में प्रवेश करते थे, वे अपने आगमन की घोषणा लकड़ी का एक टुकड़ा फेंक कर करते थे ताकि अन्य लोग उनके स्पर्श से बच सकें। गुप्त काल में, शूद्रों की भाँति, महिलाओं को भी रामायण, महाभारत और पुराण सुनने की अनुमति और कृष्ण की पूजा करने की सलाह दी गई। हालाँकि, उच्च वर्ण की महिलाओं को गुप्त काल और उससे पूर्व में भी आजीविका के स्वतन्त्र स्रोत नहीं थे। यह तथ्य है कि निचले दोनों वर्षों की महिलाओं को अपनी आजीविका स्वयं अर्जित करने की छूट थी, जिससे सामाजिक जीवन में उन्हें काफी हद तक स्वतन्त्रता मिली, इसके विपरीत, ऊपरी वर्णों की महिलाएँ अभी भी इससे वंचित थीं। इसके लिए यह तर्क दिया गया था कि वैश्य और शूद्र महिलाएँ कृषि संचालन और घरेलू सेवाएँ देती थीं, इसलिए उनका अपने पतियों के पूर्ण नियन्त्रण में रहना सम्भव नहीं था। गुप्त काल में, उच्च वर्णों ने अधिक से अधिक भूमि एवं धन अर्जित किए और अत्यधिक धनवान हो गए। वह एक से अधिक पत्नियाँ रखने में सक्षम हो गए। आगे चलकर पितृसत्तात्मक व्यवस्था दृढ़ होती गई और भूमि आदि की तरह ही वह महिलाओं को भी सम्पत्ति जैसी वस्तु समझने लगे। यह प्रचलन इतना अधिक बढ़ गया कि महिलाओं से यह अपेक्षा की जाने लगी कि पति की मृत्यु के बाद भी वह अगले जन्म में भी अपने पति की सेवा करने के लिए उनके साथ आत्मदाह करे। पति की मृत्यूपरान्त विधवा के आत्मदाह का पहला उदाहरण सन् 510 में गुप्त काल में ही मिलता है। हालाँकि गुप्त काल के कुछ विधान-ग्रन्थों के अनुसार कोई महिला पति की मृत्यु होने, उसके नपुंसक होने, संन्यासी एवं समाज बहिष्कृत होने के बाद पुनर्विवाह कर सकती थी।
ऊपरी वर्णों की महिलाओं की अधीनता का मुख्य कारण आजीविका के लिए पुरुषों पर उनकी पूरी निर्भरता और सम्पत्ति पर मालिकाना अधिकार पुरुषों के हाथ में होना था। हालाँकि, सबसे प्राचीन स्मृतियों या विधान-ग्रन्थों के अनुसार दुल्हन को विवाह के अवसर पर प्राप्त गहने, आभूषण, वस्त्र और इस तरह के अन्य उपहार, उनकी सम्पत्ति होती थी। गुप्त और उत्तरवर्ती गुप्त काल के विधान-ग्रन्थों में इन उपहारों के बारे में विस्तार से उल्लेख है। उनके अनुसार, न केवल दुल्हन के माता-पिता, बल्कि विवाहोपरान्त ससुराल से और अन्य त्यौहार के मौकों पर प्राप्त धन को भी स्त्रीधन माना जाता है। छठी शताब्दी के विधान-निर्माता कात्यायन ने कहा था कि एक महिला अपनी अचल सम्पत्ति के साथ-साथ स्त्रीधन को गिरवी रख सकती थी, या बेच सकती थी। इससे स्पष्ट है कि ऐसे विधान-निर्माता के अनुसार सम्पति में महिलाओं को हिस्सा प्राप्त था, लेकिन भारत के पितृसत्तात्मक समुदायों में पुत्री को सम्पत्ति का अधिकार देने की अनुमति नहीं थी।
वैदिक काल में ब्राह्मणों और क्षत्रियों द्वारा मानी जाने वाली प्रथा नियोग, द्वारा छोटा भाई या रिश्तेदार अपने बड़े भाई की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी से विवाह कर सकते थे। लेकिन उन्हें गुप्त और उसके पहले के विधान-ग्रन्थों में इसकी अनुमति नहीं दी गई थी। इसी तरह, उच्च वर्णों को भी विधवा पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी, लेकिन इस काल में भी शूद्र लोग नियोग या देवर विवाह दोनों प्रथा का पालन करते थे।
बौद्ध धर्म की स्थिति
गुप्त काल के दौरान बौद्ध धर्म को शाही संरक्षण मिलना बन्द हो गया था। फा-हियान के अनुसार यह एक उभरता हुआ धर्म था, लेकिन वास्तविकता में यह गुप्त काल में इतना महत्त्वपूर्ण नहीं रहा गया था, जितना कि अशोक और कनिष्क के समय में। फिर भी इस दौरान कुछ स्तूप और विहारों का निर्माण किया गया था और नालन्दा बौद्ध शिक्षा का केन्द्र बन गया।
भगवत सम्प्रदाय की उत्पत्ति और विकास
भगवतवाद उत्तरवर्ती मौर्य काल में उत्पन्न हुआ। यह विष्णु या भगवत की पूजा पर आधारित था।
वैदिक काल में विष्णु बहुत महत्त्वपूर्ण भगवान नहीं थे। वे सूर्य और उर्वरता के द्योतक थे। ई.पू. दूसरी शताब्दी तक उन्हें नारायण नामक एक देवता के साथ मिला दिया गया और वह नारायण-विष्णु के रूप में माने जाने लगे। मूल रूप से नारायण, एक गैर-वैदिक कबीलाई देवता थे, जिन्हें भगवत कहा जाता था और उनके उपासक को भागवत कहा जाता था। ये भगवान कबीलाई समुदायों के प्रमुख के समतुल्य माने जाते थे। जिस प्रकार एक कबीलाई प्रमुख को अपने रिश्तेदारों से उपहार मिलता था और वह उस उपहार को उन्हीं लोगों के बीच हिस्से लगाकर वापस बाँट देता है उसी प्रकार नारायण से भी उनके भक्त या पुजारी अच्छे भाग्य (भाग या हिस्सा) की कामना करते थे। बदले में, भक्त उनके प्रति अपनी भक्ति दिखाते थे। विष्णु और नारायण के उपासकों को विष्णु और नारायण के साथ मिलाकर एक साथ लाया गया। पहले वाले विष्णु वैदिक ईश्वर थे और बाद वाले विष्णु गैर-वैदिक। लेकिन यह दोनों संस्कृतियाँ, दो प्रकार के लोग और दो देवता आपस में घुल-मिलकर एक हो गए।
इसके अलावा, विष्णु को पश्चिम भारत में रहने वाले वृश्नी जनजाति के एक महान नायक के रूप में पहचाना जाने लगा, जिसे कृष्ण-वासुदेव नाम से जाना जाता था। महान महाकाव्य महाभारत में कृष्ण और विष्णु को एक दिखाने के लिए महाभारत को नया रूप दिया गया। इस प्रकार, ई.पू. 200 तक आते-आते देवताओं की यह तीन धाराएँ और उनके उपासक मिलकर एक हो गए; जिसका परिणाम भगवतवाद या वैष्णववाद का उद्भव था।
भगवतवाद की मुख्य पहचान भक्ति और अहिंसा है। भक्ति का तात्पर्य प्रेमयुक्त समर्पण था। यह एक प्रकार की निष्ठा थी, जो एक कबीलाई अपने प्रमुख या उसकी प्रजा अपने राजा के प्रति रखती थी। अहिंसा, या पशु-वध के विरोध का सिद्धान्त, कृषि समाज के अनुकूल था और इसे विष्णु की पुरानी उर्वरता एवं जनन-संस्कृति से जोड़ दिया गया। लोग विष्णु-मूर्ति की पूजा करते थे और इस पर चावल, जौ, तिल इत्यादि चढ़ाते थे। पशु-वध से घृणा करने के कारण, कुछ उपासक पूरी तरह शाकाहारी हो गए।
नया धर्म, विदेशियों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त उदार था। इसने कारीगरों और व्यापारियों को भी आकर्षित किया, जो सातवाहनों और कुषाणों के समय प्रबल बन गए थे। कृष्ण ने भगवद्गीता में उपदेश दिया कि अनैतिक रूप से पैदा हुई महिलाएँ, वैश्य एवं शूद्र भी उनके शरण में जा सकते हैं। इस धार्मिक ग्रन्थ में वैष्णव शिक्षाओं का प्रतिपादन किया गया। इसी के साथ-साथ विष्णु-पुराण में और कुछ हद तक विष्णु-स्मृति में भी वैष्णव धर्म को मजबूत किया गया है।
भगवतवाद या वैष्णववाद ने गुप्त काल तक महायान बौद्धवाद को पीछे कर दिया। इसने अवतारवाद के सिद्धान्त का प्रचार किया और इतिहास को विष्णु के दस अवतारों के चक्र के रूप में प्रस्तुत किया गया। ऐसी धारणा थी कि जब भी सामाजिक व्यवस्था में संकट उत्पन्न हुआ, तो विष्णु इसे बचाने के लिए मानव रूप में प्रकट हुए। धर्म के उद्धार के लिए विष्ण के प्रत्येक अवतार को आवश्यक माना गया। धर्म को वर्णों में विभाजित समाज और राज्य संरक्षित पितृसत्तात्मक परिवार की संस्था मान लिया गया।
छठी शताब्दी तक शिव और ब्रह्मा के साथ विष्णु भी त्रिदेव के सदस्य बन गए, लेकिन तब भी वे स्वयं में एक प्रमुख देवता बने रहे। छठी शताब्दी के बाद, उनकी पूजा से प्राप्त पुण्यों को लोकप्रिय बनाने हेतु कई ग्रन्थ लिखे गए, जिनमें सबसे महत्त्वपूर्ण भगवत पुराण था। इसकी कहानी पुजारियों द्वारा कई दिनों तक पढ़ी जाती थी। मध्य काल में पूर्वी भारत में भगवतघरों या विष्णु पूजन-स्थलों की स्थापना होनी शुरू हुई, जहाँ उनसे जुड़ी लीलाएँ या कहानियाँ गाई जाती थीं। इसी दौरान विष्णु उपासकों हेतु विष्णुसहस्त्रनाम सहित कई धार्मिक ग्रन्थ रचे गए।
इसके अतिरिक्त कुछ गुप्त राजा संहार के देवता, शिव के उपासक थे, लेकिन वे बाद में उजागर हुए। क्योंकि गुप्त शासन की शुरुआत में शिव को विष्णु की तरह महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं था।
गुप्त काल से मन्दिरों में मूर्ति पूजा हिन्दू धर्म की सामान्य विशेषता बन गई, जिनसे सम्बन्धित कई त्यौहार भी मनाए जाने लगे। विभिन्न वर्गों के लोगों द्वारा मनाए जाने वाले कृषि त्योहार भी धार्मिक रंग में रंग गए और पुजारियों के लिए आय के उपयोगी स्स्रोत बन गए।
गुप्त राजाओं ने विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई। बौद्ध एवं जैन धर्मावलम्बियों के उत्पीड़न का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। इसका एक कारण बौद्ध धर्म के चरित्र में कुछ परिवर्तन भी था, जिसने ब्राह्मणवाद या हिन्दू धर्म की कई विशेषताएँ धारण कर ली थी।
कला
गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण-युग कहा जाता है। यह आर्थिक दृष्टि से सच नहीं हो सकता, क्योंकि इस काल में उत्तर भारत के कई शहरों का पतन हुआ। हालाँकि, स्रोत चाहे जो भी हो, गुप्तों के पास सोना बहुत था, उन्होंने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। राजा एवं धनी व्यक्ति अपनी आय का एक हिस्सा कला और साहित्य में रत लोगों की आजीविका में खर्च करते थे। समुद्रगुप्त और चन्द्रगुप्त द्वितीय, दोनों कला और साहित्य के संरक्षक थे। समुद्रगुप्त अपने सिक्कों में वीणा बजा रहे हैं और चन्द्रगुप्त द्वितीय को अपने दरबार में नौरत्न रखने का श्रेय दिया जाता है।
प्राचीन भारत में, कला आम तौर पर धर्म से प्रेरित होती थी। प्राचीन भारत में धर्म निरपेक्ष कला बहुत कम ही संरक्षित हो पाई। मौर्य और उत्तरवर्ती मौर्य काल में बौद्ध धर्म ने कला को बहुत बढ़ावा दिया। ढेरों शिलास्तम्भ बनवाए, सुन्दर गुफाओं का निर्माण कराया और ऊँचे स्तूप या स्मृति मीनार खड़े करवाए। गोलाकार आधार पर पत्थर निर्मित स्तुपों की संरचना गुम्बदनुमा थी। इसके अलावा बुद्ध की अनगिनत मूर्तियाँ भी बनाई गई।
गुप्त काल में बुद्ध की आदमकद प्रतिमा बनाई गई, ताम्बे से निर्मित इस प्रतिमा की ऊँचाई 6 फीट से भी अधिक थी। इसे भागलपुर के निकट सुलतानगंज में खोजा गया था, जो कि अब बर्मिंघम में है। गुप्त काल में ही सारनाथ और मथुरा में बुद्ध की सुन्दर मूर्तियाँ बनाई गईं, किन्तु बौद्ध कला के सबसे बेहतरीन नमूने अजन्ता के चित्र हैं। यद्यपि ये चित्र ई.पू. पहली शताब्दी से ईस्वी सन् सातवीं शताब्दी तक निर्मित हुए फिर भी इनमें से ज्यादातर गुप्त काल से सम्बन्धित हैं। यह चित्र गौतम बुद्ध और बुद्ध के पूर्व जन्म की विभिन्न घटनाओं को चित्रित करते हैं। यह जन्म-कथाएँ जातक से सम्बन्धित हैं। आज भी अजन्ता के चित्र प्राकृतिक और सजीव लगते हैं, चौदह शताब्दियों के बाद भी उनकी चमक बरकरार है। हालाँकि, गुप्त शासक अजन्ता चित्रकला के संरक्षक नहीं थे।
चूँकि गुप्त राजाओं ने ब्राह्मण धर्म का समर्थन किया, इसलिए पहली बार विष्णु, शिव, एवं कुछ अन्य हिन्दू देवताओं की प्रतिमाएँ इसी काल में प्रचलन में आईं। कई जगहों पर सभी देवताओं को एक ही पट पर एक साथ दिखाया गया है, जहाँ गौण देवताओं से बने घेरे के मध्य मुख्य देवता बैठे हुए हैं। मुख्य देवता बड़े आकार में और अन्य देवताओं की प्रतिमाएँ छोटे आकार में दर्शाई गई हैं। स्पष्ट रूप से यह सामाजिक स्तरीकरण और सामाजिक भेदभाव को दर्शाता है।
वास्तुकला के मामले में गुप्त काल पीछे था। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में ईंट से बने कुछ मन्दिर और एक पत्थर के मन्दिर मिलते हैं। जिनमें कानपुर के भीतरगाँव के ईंट मन्दिर, गाजीपुर के भितरी और झाँसी के देवगढ़ मन्दिर का उल्लेख किया जा सकता है। नालन्दा में बौद्ध महाविहार (विश्वविद्यालय) पाँचवीं शताब्दी में स्थापित किया गया था; ईंट से बनी इसकी प्राचीनतम संरचना इसी गुप्त काल से सम्बन्धित है।
साहित्य
गुप्त काल धर्मनिरपेक्ष साहित्य रचना हेतु उल्लेखनीय है, जिसमें उच्च कोटि की दरबारी कविता शामिल थी। गुप्त काल की प्रारम्भिक अवस्था में भास एक महत्त्वपूर्ण कवि थे; उन्होंने तेरह नाटक लिखे। यद्यपि उन्होंने नाटकों की रचना संस्कृत में की थी, लेकिन उनमें प्राकृत पर्याप्त मात्रा में है। वे द्रदिरचारुदत्त नाटक के लेखक थे, जो बाद में शूद्रक के मृच्छकटिक या लिटिल क्ले कार्ट (माटी की खिलौना गाड़ी) के रूप में पुनःप्रस्तुत हुआ। यह नाटक एक ब्राह्मण व्यापारी और एक सुन्दर वेश्या के प्रेम प्रसंग पर आधारित है जिसे प्राचीन नाटकों में उत्कृष्ट रचना मानी जाती है। भास ने अपने नाटकों में पर्दे के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग किया, जिससे यूनानी सम्पर्क का पता चलता है। हालांकि, गुप्त काल की साहित्यिक प्रसिद्धि कालिदास की रचना से हुई, जिनका काल चौथी शताब्दी का उत्तरार्ध और पाँचवीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। वे संस्कृत साहित्य के महान कवि थे; उनकी कृति अभिज्ञानशकुन्तलम का विश्व साहित्य में शीर्ष स्थान है। यह राजा दुष्यन्त और शकुन्तला की प्रेम कहानी से सम्बन्धित है, जिनका पुत्र भरत बहुत बड़ा शासक बना। यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद होने वाले प्राचीनतम भारतीय साहित्य अभिज्ञानशकुन्तलम और उसके बाद भगवद्गीता ही थे। गुप्त काल के दौरान भारत में प्रस्तुत नाटकों की दो सामान्य विशेषताएँ हैं। सबसे पहली, कि वे सभी सुखांत नाटक थे; उनमें कोई त्रासदी नहीं पाई जाती। दूसरी, कि उनमें उच्च और निम्न वर्ण के पात्र समान भाषा नहीं बोलते; इन नाटकों में महिलाएँ और शूद्र प्राकृत और उच्च वर्ग संस्कृत भाषा बोलते हैं। याद रहे कि अशोक और सातवाहन, प्राकृत भाषा को राज्य भाषा के रूप में इस्तेमाल करते थे।
इस काल में धार्मिक साहित्य की रचना में भी वृद्धि हुई। इस समय के अधिकांश साहित्य में धार्मिक पूर्वाग्रहों का रुझान दिखता है। दो महान महाकाव्य, रामायण और महाभारत, लगभग चौथी शताब्दी ईस्वी में पूर्ण हुए थे। महाकाव्यों और पुराणों को ब्राह्मणों द्वारा संकलित किया गया जो कि क्षत्रिय परम्परा को दर्शाते हैं। यह काव्य मिथकों, किंवदन्तियों और अतिरंजनाओं से परिपूर्ण हैं। इनमें सामाजिक विकास का प्रतिबिम्ब मिलता हैं, लेकिन राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से ये विश्वसनीय नहीं हैं। रामायण राम की कहानी से सम्बन्धित है, जिन्होंने सौतेली माँ कैकेयी की साजिश के कारण, पिता दशरथ की आज्ञा से चौदह वर्षों के लिए अयोध्या को त्याग दिया था। उन्होंने ईमानदारी से अपने पिता के आदेश का पालन किया और जंगल चले गए, जहाँ से लंका के राजा रावण ने उनकी पत्नी सीता का हरण कर लिया। आखिरकार सुग्रीव की मदद से सीता को बचाने में राम सफल हुए। कहानी में दो महत्त्वपूर्ण नैतिक शिक्षा हैं- सबसे पहले तो यह परिवार की संस्था को आदर्श बनाता है, जिसमें एक बेटे को अपने पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, छोटे भाई को अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करना चाहिए और पत्नी को सभी परिस्थितियों में अपने पति के प्रति विश्वास योग्य होना चाहिए। दूसरा, कि रावण बुराई का प्रतीक है, जबकि राम, धार्मिकता की शक्ति का उदाहरण। अन्त में, बुराई पर धार्मिकता की विजय; अच्छाई से बुराई का नाश एक अच्छा सन्देश है। महाभारत की मुख्य कथा की तुलना में रामकथा में व्यापक सामाजिक और धार्मिक अपील थी। आज सभी महत्त्वपूर्ण भारतीय भाषाओं एवं दक्षिण पूर्व एशिया में भी रामायण के कई संस्करण हैं।
महाभारत मुख्यतः, कौरव-पाण्डव भाइयों के आपसी संघर्ष की कहानी है। इससे पता चलता है कि शासन में कोई रिश्तेदारी नहीं होती। हालाँकि, पाण्डव, धृतराष्ट्र द्वारा शासित राज्य में हिस्से के हकदार थे, कौरवों ने उन्हें क्षेत्र का एक इंच भी देने से इनकार कर दिया। इससे, कौरवों और कृष्ण द्वारा संरक्षित पाण्डवों के बीच लम्बे समय तक युद्ध चला।
अन्ततः पाण्डवों ने कौरवों को युद्ध में हरा दिया और पाण्डव विजयी हो गए। यह कहानी भी बुराइयों की शक्तियों पर धार्मिकता की जीत का प्रतीक है। भगवद्गीता, महाभारत का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। यह सिखाता है कि फल की लालसा रखे बिना व्यक्ति को अपनी जाति और स्थिति के हिसाब से प्रदत्त हर कर्म पूरा करना चाहिए।
पुराणों का संकलन गुप्त काल में पूरा हुआ था। इन पुराण महाकाव्यों का अनुसरण करने पर पता चलता है कि वे मिथकों, किंवदन्तियों, उपदेशों आदि से भरे पड़े हैं, जो सामान्य लोगों की शिक्षा और विवेक के संवर्धन के लिए लिखे गए। इस काल में विभिन्न स्मृतियों या विधान-पुस्तकों का संकलन भी किया गया, जिसमें सामाजिक और धार्मिक मानदण्ड कविता के रूप में लिखे थे। हालांकि स्मृतियों पर टीका लेखन गुप्त काल के बाद शुरू हुआ।
गुप्त काल में पाणिनी और पतंजलि की रचनाओं के आधार पर संस्कृत व्याकरण का भी विकास हुआ। यह काल विशेष रूप से चन्द्रगुप्त द्वितीय के दरबार में अमरसिम्हा द्वारा संकलित अमरकोश के लिए स्मरणीय है। इस शब्दकोश को पारम्परिक तरीके से संस्कृत सीखने वाले विद्यार्थी कंठस्थ कर लेते थे। कुल मिलाकर, गुप्त काल शास्त्रीय साहित्य के इतिहास में एक स्वर्णिम काल था, जिसमें एक अलंकृत शैली विकसित हुई, जो पुराने सरल संस्कृत शैली से बिलकुल अलग थी। इस काल के बाद से गद्य की तुलना में पद्म पर अधिक जोर दिया जाने लगा था, जिससे कुछ टीका ग्रन्थों की भी प्राप्ति होती है। गुप्तों की राजकीय भाषा निःसन्देह संस्कृत थी, हालाँकि इस काल में बहुत अधिक ब्राह्मणवादी धार्मिक साहित्य लिखे गए, किन्तु यही वह काल भी है जब कुछ प्रारम्भिक धर्मनिरपेक्ष साहित्यों की भी रचना हुई।
विज्ञान और तकनीक
पाँचवीं शताब्दी में, पाटलिपुत्र के आर्यभट्ट ने आर्यभटीय नामक एक गणितीय पुस्तक लिखी। प्रतीत होता है कि यह गणितज्ञ विभिन्न प्रकार की गणनाओं से भली-भाँति परिचित थे। आर्यभट्ट, शून्य और दशमलव प्रणाली दोनों के ज्ञाता दिखते हैं। इलाहाबाद जिले के सन् 448 के एक गुप्तकालीन अभिलेख से पता चलता है कि पाँचवीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में दशमलव प्रणाली अस्तित्व में थी। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में, रोमक सिद्धान्त नामक एक ग्रन्थ की रचना हुई थी, इसके शीर्षक से ही पता चलता है कि यह ग्रीक और रोमन विचारों से प्रभावित था।
गुप्त काल के शिल्पकारों ने लोहे और काँसे के कामों में अपनी प्रतिभा दिखाई। शिल्पकारों की धातु तकनीक की जानकारी उन्नत अवस्था में पहुँच चुकी थी, जिसके कारण बड़े पैमाने पर बुद्ध की काँस्य मूर्तियों का निर्माण शुरू हुआ। लौह-शिल्पकारी का सबसे अच्छा उदाहरण दिल्ली के मेहरौली में पाया गया लौह-स्तम्भ है। चौथी शताब्दी में निर्मित इस स्तम्भ में पन्द्रह शताब्दियों के बाद भी जंग नहीं लग पाया। यह कारीगरों के तकनीकी कौशल का प्रमाण है। हालाँकि दिल्ली में शुष्क मौसम ने भी इसके संरक्षण में योगदान दिया होगा। एक शताब्दी पहले तक पश्चिम में किसी भी लोहे के कारखाने में इस तरह के स्तम्भ बनाना असम्भव था। विडम्बना ही है कि उत्तरवर्ती समय के भारतीय कारीगर इस ज्ञान को आगे विकसित नहीं कर सके।
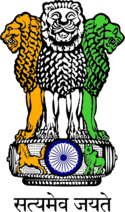
Downloaded the sv66apps a few days back and I like it! Much easier to play on my phone. Pretty smooth too. Give it a try at sv66apps. May your odds be forever in your favour.