हर्ष एवं उनका काल (प्राचीन भारत का इतिहास)
हर्ष का साम्राज्य
बिहार और उत्तर प्रदेश स्थित केंद्र से, गुप्त ने उत्तर एवं पश्चिम भारत पर लगभग बि 160 साल तक, अर्थात् छठी शताब्दी के मध्य तक शासन किया। उसके बाद उत्तर भारत फिर से कई राज्यों में विभाजित हुआ। श्वेत हूणों ने कश्मीर, पंजाब और पश्चिमी भारत पर सन् 500 से अपना वर्चस्व कायम कर लिया। उत्तर एवं पश्चिम भारत लगभग आधे दर्जन सामन्तों के नियन्त्रण में चला गया, जिन्होंने गुप्त साम्राज्य को आपस में बाँट लिया। धीरे-धीरे हरियाणा के राजवंशों में से थानेसर के एक शासक ने अन्य सभी सामन्तों पर अपनी सत्ता कायम कर ली, उसका नाम हर्षवर्धन (सन् 606-47) था। थानेसर में ‘हर्ष के टीले’ की खुदाई से कुछ ईंट की इमारतों की खोज हुई है, लेकिन वे किसी महल के हिस्से जैसी नहीं प्रतीत होतीं।
हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और वहाँ से उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। सातवीं शताब्दी तक पाटलिपुत्र का पतन होने के समय कन्नौज उभरती हुई शक्ति थी। यह कैसे हुआ? पाटलिपुत्र की सत्ता और उसका महत्त्व व्यापार एवं वाणिज्य से था। यहाँ पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की चारों तरफ की नदियों से आने वाले व्यापारियों से चुंगी ली जाती थी, जो उनका मुख्य आय स्त्रोत था।
व्यापार में गिरावट के कारण धन की कमी हो गई, जिससे अधिकारियों एवं सैनिकों को वेतन के बदले भूमि दान से भुगतान होने लगा था। इसलिए शहर का भी महत्त्व घट गया। सत्ता सैन्य शिविरों (स्कन्धावारों) एवं दूर-दूर फैले सामरिक महत्व के स्थानों में स्थानान्तरित हो गई। ऐसा ही एक क्षेत्र कन्नौज था। इसलिए उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित इस स्थान की राजनीतिक महत्ता, छठी शताब्दी के उत्तरार्ध से बढ़ गई। हर्ष के शासनकाल से राजनीतिक सत्ता के केन्द्र के रूप में इसका उदय, उत्तर भारत में सामन्ती काल के प्रादुर्भाव को दर्शाता है और पाटलीपुत्र मुख्यतः पूर्व-सामन्ती व्यवस्था पर ही कायम रहा। मैदानी इलाकों की किलाबन्दी अधिक मुश्किल होती थी, लेकिन कन्नौज ऊँचे स्थान पर स्थित था, जिसकी किलाबन्दी आसानी से हो सकती थी। दोआब के ठीक केन्द्र में स्थित कन्नौज क्षेत्र की व्यवस्थित किलाबन्दी की गई। अब दोआब के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों पर नियन्त्रण बनाए रखने के लिए सैनिकों को जमीन और जल दोनों मागों से भेजा जा सकता था।
हर्ष के शासन के प्रारम्भिक इतिहास को बाणभट्ट की कृतियों के अध्ययन से बेहतर समझा जा सकता है। बाणभट्ट, हर्ष के दरबारी कवि थे, उन्होंने हर्षचरित शीर्षक से एक ग्रन्थ लिखा। चीनी तीर्थयात्री व्हेन त्सांग के दस्तावेज से भी इसकी पुष्टि होती है, जो सातवीं शताब्दी में भारत आए और लगभग 15 वर्षों तक यहीं रहे। हर्ष के अभिलेख विभिन्न प्रकार के करों और अधिकारियों के बारे में भी बताते हैं।
हर्ष को भारत का अन्तिम महान हिन्दू सम्राट कहा जाता है, लेकिन वे न तो एक कट्टर हिन्दू थे और न ही पूरे देश के शासक। उनका अधिकार कश्मीर को छोड़कर उत्तर भारत तक सीमित था। राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा उनके प्रत्यक्ष नियन्त्रण में थे, लेकिन उनका प्रभाव बहुत व्यापक क्षेत्रों तक था। ऐसा लगता है कि सीमावर्ती राज्यों ने उनकी सम्प्रभुता स्वीकार कर ली थी। पूर्वी भारत में उन्होंने गौड़ के शैव राजा शशांक से सामना किया, जिसने कि बोधगया में बोधि वृक्ष को काट कर गिरा दिया था। हालाँकि, सन् 619 में शशांक की मृत्यु ने इस शत्रुता का अन्त कर दिया। दक्षिणी मोर्चे पर हर्ष के विजयी अभियान को आधुनिक कर्नाटक और महाराष्ट्र के शासक, चालुक्य राजा, पुलकेशिन ने नर्मदा नदी पर रोका। पुलकेशिन की राजधानी आधुनिक बीजापुर जिले में बादामी में थी। इसके अलावा, हर्ष को किसी भी गम्भीर विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। वे भारत के एक बड़े हिस्से में राजनीतिक एकता बनाने में सफल रहे।
प्रशासन
हर्षवर्धन का साम्राज्य प्राचीन और मध्ययुगीन संक्रमण काल का उदाहरण है। हर्ष ने अपने साम्राज्य पर गुप्त की तरह शासन किया, लेकिन अपेक्षाकृत हर्ष का प्रशासन अधिक सामन्ती और विकेन्द्रीकृत था। कहा जाता है कि हर्ष के पास 1,00,000 घोड़े और 60,000 हाथी थे। यह आश्चर्यजनक प्रतीत होता है, क्योंकि सुदूर दक्षिण के सिवाय पूरे देश पर शासन करने वाले मौर्य के पास, केवल 30,000 घुड़सवार और 9000 हाथी थे। हालांकि युद्ध के समय अपने सभी सामन्तों के समर्थन को जुटाने की स्थिति में हर्ष होते, तो उनके पास इतनी बड़ी सेना हो सकती थी। हर सामन्त अपने हिस्से के पैदल सिपाहियों और घोड़ों के साथ आते थे और इस तरह उन्हें शाही सेना में जोड़ा जाता था। शाही सेना में वृद्धि, आबादी में बड़ी वृद्धि का संकेत है।
राज्य के लिए विशेष सेवाएँ प्रदान करने के लिए पुजारियों को भूमिदान जारी रखा गया। उल्लेखनीय है कि, दस्तावेज जारी कर अधिकारियों को भूमि अनुदान देने का श्रेय हर्ष को जाता है। इन अनुदानों में भी पहले के अनुदानों की तरह ही रियायतें दी गई थी। चीनी तीर्थयात्री व्हेन त्सांग बताते हैं कि हर्ष का राजस्व चार भागों में विभाजित था। इनमें पहला हिस्सा राजा, दूसरा विद्वान, तीसरा अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों और चौथा धार्मिक उद्देश्यों पर व्यय के लिए निर्धारित किया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य के मन्त्री और अधिकारी भूमि सम्पन्न थे। हर्ष काल में ही अधिकारियों को सामन्तों द्वारा भूमि दान और पुरस्कृत करने का चलन शुरू हुआ था। इसीलिए राजा हर्ष द्वारा जारी सिक्के कम मिलते हैं।
हर्ष के साम्राज्य में, कानून व्यवस्था अच्छी नहीं थी। व्हेन त्सांग की सुरक्षा हेतु, राजा ने विशेष देखभाल की व्यवस्था की होगी, फिर भी उनके सामान लूट लिए गए थे; यद्यपि वे बताते हैं कि यहाँ के कानून के अनुसार अपराध के लिए गम्भीर दण्ड दिए जाते थे। डकैती को दसरा देशद्रोह माना जाता था, जिसके लिए डाकू का दायाँ हाथ काट दिया जाता था। ऐसा लगता है कि बौद्ध धर्म के प्रभाव में सजा की कठोरता कम हई और अपराधियों को आजीवन कारावास मिलने लगा।
सन् 629 में चीन छोड़कर भारत आने वाले और पूरे भारत का दौरा करने वाले व्हेन त्सांग के कारण हर्ष का शासन ऐतिहासिक रूप से महत्त्वपूर्ण है। भारत में लम्बे समय तक रहने के बाद, वे सन् 645 में चीन लौटे। वे बिहार में स्थित बौद्ध विश्वविद्यालय, नालन्दा में अध्ययन करने और बौद्ध साहित्य का संग्रह करने आए थे। उन्होंने हर्ष के दरबार में कई वर्ष बिताए और भारत में व्यापक यात्रा की। उनके प्रभाव में हर्ष बौद्ध धर्म के एक महान समर्थक बन गए और इसके लिए खूब दान दिए। उन्होंने हर्ष के दरबार और उनके जीवन के बारे में स्पष्ट रूप से वर्णन किया है, यह दस्तावेज फाहियान की तुलना में अधिक समृद्ध और अधिक विश्वसनीय है। यह यहाँ के सामजिक और आर्थिक जीवन के साथ-साथ धार्मिक सम्प्रदायों पर भी प्रकाश डालता है।
चीनी दस्तावेज बताते हैं कि पाटलिपुत्र पतन की ओर था, साथ ही वैशाली में भी ऐसा ही था। दूसरी तरफ, दोआब में प्रयाग और कन्नौज महत्त्वपूर्ण थे। कहा जाता है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय लोगों का जीवन सरल था। लेकिन अमीर सामन्त और पुजारी लोग विलासी जीवन बिताते थे। इससे इन दोनों उच्च वर्षों के बीच स्तर-भेद का आना स्पष्ट होता है। ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण के अधिकांश लोग कृषि कार्य करने लगे थे। व्हेन त्सांग शूद्रों को कृषक कहते हैं, जो महत्त्वपूर्ण है। क्योंकि पहले के ग्रन्थों में शूद्रों को इन तीन उच्च वर्णों के सेवक के रूप में ही दर्शाया गया है। चीनी तीर्थयात्री अछूत और सफाई करने वालों और जल्लादों की स्थितियों का वर्णन करते हैं। अछूत लोग, गाँवों के बाहर रहते थे और लहसुन, प्याज खाते थे, शहर में प्रवेश करने से पहले उन्हें जोर से चिल्लाते हुए प्रवेश की घोषणा करनी पड़ती थी, ताकि लोग उनसे दूर रहें।
बौद्ध धर्म और नालन्दा
जब चीनी तीर्थयात्री भारत में थे तो बौद्ध अठारह सम्प्रदायों में विभाजित थे। बौद्ध धर्म के पुराने केन्द्रों का पतन हो रहा था। सबसे प्रसिद्ध केन्द्र नालन्दा था, जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक महान बौद्ध विश्वविद्यालय था। कहा जाता है कि यहाँ लगभग 10,000 बौद्ध भिक्षु छात्र थे। उन्हें महायान परम्परा का बौद्ध दर्शन सिखाया जाता था। यद्यपि नालन्दा के सभी टीलों का उत्खनन नहीं हुआ है, किन्तु उत्खनन से इसके बहुत प्रभावशाली परिसर मिले हैं। इसे पाँचवीं शताब्दी से 700 वर्षों तक संरक्षित किया गया और इसका जीर्णोद्धार किया गया। खुदाई में मिली इमारतों में 10,000 भिक्षुओं को रखने की क्षमता नहीं है। सन् 670 में, एक अन्य चीनी तीर्थयात्री, इत्सिंग नालन्दा आए और उन्होंने केवल 3000 भिक्षुओं के रहने का उल्लेख किया। यह सम्भव जान पड़ता है। क्योंकि यदि शेष टीलों की भी खुदाई हो जाए तो भी 10,000 भिक्षुओं को रहने की क्षमता नहीं हो सकती। व्हेन त्सांग के अनुसार, नालन्दा विश्वविद्यालय 100 गाँवों के राजस्व से चलता था। इत्सिंग इस संख्या को 200 बताते हैं। इस प्रकार हर्षवर्धन के शासनकाल में नालन्दा विशाल विहार था।
हर्ष ने सहिष्णु धार्मिक नीति का पालन किया। वह अपने प्रारम्भिक जीवन वर्षों में शैव थे, किन्तु धीरे-धीरे वे बौद्ध धर्म के एक महान संरक्षक बन गए। एक निष्ठावान बौद्ध के रूप में उन्होंने महायान के सिद्धान्तों को व्यापक रूप से प्रचारित करने के लिए कन्नौज में एक भव्य सभा आयोजित की। इस सभा में न केवल व्हेन त्सांग और कामरूप शासक भास्करवर्मन, बल्कि बीस राज्यों के राजाओं और विभिन्न सम्प्रदायों के कई हजार पुजारी भी शामिल हुए। एक हजार व्यक्तियों को समाहित करने योग्य दो झोपड़ीनुमा सभा का निर्माण किया गया था। हालाँकि, सबसे महत्त्वपूर्ण निर्माण एक विशाल टॉवर था, जिसके बीच में बुद्ध की एक स्वर्ण मूर्ति थी, जो राजा जैसा ही लम्बा था। हर्ष ने मूर्ति की पूजा की और सार्वजनिक रात्रिभोज कराया। व्हेन त्सांग ने सभा में चर्चा शुरू की और महायान बौद्ध धर्म के गुणों को बताया और श्रोताओं से अपने तर्क को खण्डन करने की चुनौती दी। हालाँकि, पाँच दिनों तक कोई भी आगे नहीं आया; फिर उनके धार्मिक प्रतिद्वन्द्वियों ने उनकी हत्या की साजिश रची। इसका पता चलते ही, हर्ष ने व्हेन त्सांग को जरा भी हानि पहुँचाने पर सर कटवाने की चेतावनी दी। अचानक महान टॉवर में आग लग गई और हर्ष की हत्या करने का प्रयास किया गया। हर्ष ने तब 500 ब्राह्मणों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने उनमें से अधिकतर को निर्वासित और कुछ को मृत्यु की भी सजा दी। इससे यह पता चलता है कि हर्ष उतने सहिष्णु नहीं थे, जितना उनके बारे में बताया गया है। कन्नौज के बाद, उन्होंने प्रयाग में एक बड़ी सभा आयोजित की, जिसमें सभी सहायक शासक, मन्त्री, रईस आदि शामिल थे। इस अवसर पर, बुद्ध की प्रतिमा की पूजा की गई और व्हेन त्सांग ने व्याख्यान दिए। अन्त में, हर्ष ने पर्याप्त दान किया और एक परम्परा के अनुसार, उन्होंने अपने व्यक्तिगत कपड़ों को छोड़कर सब कुछ दे दिया। व्हेन त्सांग ने हर्ष की खूब प्रशंसा की। उनके लिए राजा दयालु, विनम्र और कृपालु थे, तभी यह तीर्थयात्री साम्राज्य के विभिन्न भागों का दौरा करने में सक्षम हुआ।
हर्षचरित में बाणभट्ट ने अपने संरक्षक हर्ष के शुरुआती वर्षों का अलंकृत शैली में अतिरंजित वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसकी शैली उत्तरवर्ती लेखकों के लिए अनुकरणीय साबित हुई। हर्ष न केवल विद्वानों के संरक्षण और शिक्षा के लिए, बल्कि तीन नाटकों के लेखन के लिए भी याद किए जाते हैं: प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनन्द। बाणभट्ट अपने काव्यात्मक कौशल का श्रेय हर्ष को देते हैं और कुछ उत्तरवर्ती लेखक उन्हें साहित्यिक सम्राट भी मानते हैं। हालाँकि, हर्ष के तीन नाटकों के लेखन पर कई मध्ययुगीन विद्वानों ने सन्देह व्यक्त किया है। ऐसी मान्यता है कि धावक नामक व्यक्ति द्वारा इन तीनों की रचना हुई, जो विचारार्थ हर्ष को दी गई और सम्भवतः हर्ष ने कुछ अंश लिखे हों। कहावत है कि राजा लेखक केवल आधे लेखक होते हैं। प्राचीन और मध्ययुगीन भारत, दोनों ही में, राजा की छवि को बढ़ाने के लिए, अन्य उपलब्धियों के साथ-साथ उच्च साहित्यिक उपलब्धियों को भी दर्शाया जाता था। समुद्रगुप्त के समय हरिशेना द्वारा शुरू की गई संरक्षक की प्रशंसा का चलन हर्ष के समय तक सामान्यतः और मजबूती से स्थापित हो चुका था। स्पष्ट है, कि इसका उद्देश्य केवल राजा का विश्वास जीतना ही नहीं था, बल्कि प्रतिद्वन्द्वियों और प्रजा की दृष्टि में उनका महिमा मण्डन करना भी होता था।
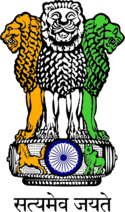
Heard good buzz about 9096betvip and gave it a shot. They’re super legit and professional. Definetly a place to check out! Get your game on at 9096betvip!