पूर्वी भारत में सभ्यता का प्रसार (प्राचीन भारत का इतिहास)
सभ्यता के लक्षण
किसी क्षेत्र को तभी सभ्य माना जाता है जब वहाँ पर कुछ बुनियादी विशेषताएँ विकसित ‘हों, जैसे लिखने का ज्ञान, कर संचय की विकसित प्रणाली, धार्मिक, प्रशानिक और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के निपटाने हेतु सामाजिक वर्गों की व्यवस्था और उसी के अनुरूप विशेषज्ञों की उपस्थिति। कुल मिलाकर एक सभ्य समाज इतना उद्यमशील होता है, जिसके उत्पादन से न केवल वास्तविक उत्पादन करने वाले कारीगरों और किसानों की बल्कि उन उपभोक्ताओं के हितों की भी रक्षा की जा सके जो उत्पादन में शामिल नहीं हैं। इन सभी तत्त्वों के संयोजन से ही सभ्यता का निर्माण होता है। किन्तु पूर्वी भारत के एक बड़े हिस्से में इन तत्वों की उपस्थिती काफी देर से दर्ज हो पायी। पूर्वी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और असम के अधिकतर हिस्सों में लगभग चौथी शताब्दी से पहले के कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं।
चौथी से लेकर सातवीं शताब्दी तक की अवधि उल्लेखनीय है। इस दौरान उन्नत ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रसार, राज्य व्यवस्थाओं के गठन और पूर्वी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पूर्वी बंगाल, दक्षिण-पूर्वी बंगाल और असम में सामाजिक वर्गों की स्थापना हुई। इसका संकेत इन क्षेत्रों से बहुतायत में पाए गए गुप्त काल के संस्कृत अभिलेखों से मिलता है। इन अभिलेखों का काल निर्धारण गुप्त संवत में हुआ है। इनका अधिकतर इस्तेमाल धार्मिक उद्देश्यों के लिए ब्राह्मण, वैष्णव मन्दिर और बौद्ध मठों के लिए सामन्तों द्वारा भूमि अनुदान के शासनादेश के रूप में किया गया है। इन लाभार्थियों ने संस्कृति के उन्नत तत्त्वों को फैलाने और मजबूत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रक्रिया को क्षेत्रों के सर्वेक्षण के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है।
उड़ीसा, पूर्वी और दक्षिणी मध्य प्रदेश
महानदी के दक्षिण का क्षेत्र, कलिंग या तटीय उड़ीसा अशोक के समय में अचानक बहुत महत्त्वपूर्ण हो गया, हालाँकि ई. पू. पहली शताब्दी के बाद ही उस क्षेत्र में एक मजबूत राज्य स्थापित हुआ। इसके शासक, खारवैल मगध तक बढ़ आए थे। पहली और दूसरी शताब्दी तक उड़ीसा के बन्दरगाहों से मोती, हाथी दाँत और मलमल का अच्छा व्यापार होता था। भुवनेश्वर से 60 किलोमीटर की दूरी पर खारवेल की राजधानी के कलिंगनगरी के शिशुपालगढ़ में उत्खनन से रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक सम्पकों को दर्शाने वाली कई रोमन वस्तुओं के संकेत मिलते हैं। हालाँकि, उड़ीसा, विशेषकर उत्तर उड़ीसा का अधिकतर हिस्सा, न तो राज्य में गठित हुआ और न ही वाणिज्यिक गतिविधि में, चौथी शताब्दी में समुद्रगुप्त द्वारा विजित क्षेत्रों की सूची में कोसल और महाकांतार शामिल थे। इसमें उत्तरी एवं पश्चिमी उड़ीसा के कुछ हिस्से शामिल होते हैं। चौथी शताब्दी के उत्तरार्ध से छठी शताब्दी तक, उड़ीसा में कई राज्यों का गठन हुआ। उनमें से कम से कम पाँच स्पष्टतः पहचाने जा सकते हैं। उनमें सबसे महत्त्वपूर्ण राज्य माठर का था, जिन्हें पितृभक्त के रूप में भी जाना जाता था, जिनका शासन महानदी और कृष्णा के बीच चरम पर था। उनके समकालीन पड़ोसियों में वसिष्ठ, नल और मान थे। वसिष्ठों ने आन्ध्र की सीमाओं पर दक्षिणी कलिंग में शासन किया; वहीं नलों ने महकणतारा के वन क्षेत्र और मनों ने महानदी से परे उत्तर में तटीय इलाके में। प्रत्येक राज्य ने अपने कर, प्रशासन और सैन्य प्रणाली की व्यवस्था की। नलों और सम्भवतः मनों ने अपने सिक्के भी विकसित किए। प्रत्येक राज्य ने ब्राह्मणों को भूमि दान किया और बाहर से आमन्त्रित भी किया। अधिकांश राजाओं ने वैदिक यज्ञ भी किए, जिनका कारण केवल आध्यात्मिक नहीं था बल्कि शक्ति, प्रतिष्ठा और वैधता के लिए भी था।
इस अवधि के दौरान उन्नत संस्कृति के तत्त्व कलिंग के तटीय क्षेत्र तक तो विस्तृत थे ही। साथ ही उड़ीसा के अन्य हिस्सों में भी विद्यमान थे। मध्य प्रदेश के कबीलाई क्षेत्र बस्तर में नल के समय के सोने के सिक्कों की खोज उल्लेखनीय है। यह एक आर्थिक व्यापार को दर्शाता है, जिसमें बड़ी संख्या में लेन-देन के लिए और उच्च अधिकारियों को सेवा के भुगतान हेतु स्वर्ण मुद्राओं का उपयोग होता था। इसी प्रकार, मनों ने ताम्बे के सिक्के जारी किए, जो कारीगरों और किसानों द्वारा धातु के पैसे के उपयोग को दर्शाता है। विभिन्न राज्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों में नई राजकोषीय इकाई बनाकर अपनी आय में वृद्धि की। मठारों ने महेन्द्र पर्वत क्षेत्रों में महेन्द्र भोग नामक एक जिला बनाया और द्वंतयवागुभोग नामक जिले पर शासन भी किया, जो अपने प्रशासकों को हाथी दाँत और चावल की आपूर्ति करते थे। हालाँकि यह पिछड़े क्षेत्र में आता था। मठारों ने अग्रहार नामक एक कोष बनाया था, जिसमें गाँवों की कुछ जमीन और कुछ आय शामिल की जाती थी, जिसका प्रयोग धार्मिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों में लगे ब्राह्मणों को सहायता देने के लिए होता था। इस क्षेत्र के कुछ अग्रहारों से कर उगाहा जाता था जबकि देश के अन्य क्षेत्र का अग्रहर कर-मुक्त होते थे। ब्राह्मणों के आगमन से भूमि अनुदान द्वारा कबीलाई क्षेत्र, जंगल और लाल मिट्टी के इलाकों में भी कृषि का आरम्भ हुआ। जिससे मौसम की बेहतर समझ के साथ नई भूमि में बेहतर कृषि का आरम्भ हुआ। पूरे वर्ष को चार-चार महीनों की तीन इकाइयों में विभाजित किया गया था, तीन ऋतुओं के आधार पर समय का निर्धारण किया जाता था। मठारों के समय में, पाँचवीं सदी के मध्य में, लोगों ने वर्ष को बारह चन्द्र महीनों में विभाजित करने की प्रथा शुरू की। इसका तात्पर्य मौसम की स्थिति को ठीक से जानने से था, जो आगे चलकर कृषि कार्यों के लिए उपयोगी सिद्ध हुई।
उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में, ई.पू. तीसरी शताब्दी के बाद से ही लेखन की जानकारी हो चुकी थी। चौथी शताब्दी के उत्तरार्ध में अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे, लेकिन सन् 350 से संस्कृत का उपयोग शुरू हो गया था। उल्लेखनीय है कि इस भाषा के दस्तावेज महानदी से परे उत्तरी तटीय क्षेत्र से बाहर भी मिले है। जिससे पता चलता है कि लेखन कौशल एवं संस्कृत भाषा उड़ीसा के बहुत बड़े हिस्से तक फैल चुकी थी। उस अवधि के अभिलेखों में संस्कृत के कुछ उत्कृष्ट श्लोक भी मिले हैं। संस्कृत भाषा धर्म और संस्कृति के प्रसार का माध्यम तो थी ही साथ ही नए क्षेत्रों में, सम्पत्ति सम्बन्धी कानूनों और सामाजिक नियमों की भी माध्यम बनी। संस्कृत के शासनपत्रों एवं दस्तावेजों में पुराणों एवं धर्मशास्त्रों की सूक्तियों को उद्धृत किया गया है। राजा वर्ण व्यवस्था के संरक्षक माने जाते थे। गंगा और यमुना के संगम स्थल प्रयाग में गंगा में डुबकी लगाना पवित्र माना जाता था; विजयी राजा यहाँ आकर पुण्यलाभ लेते थे।
बंगाल
बंगाल के परिप्रेक्ष्य में, उत्तर बंगाल के कुछ हिस्से, जो अब बोगरा जिले में हैं, से अशोक के शासनकाल में लेखन के प्रसार के साक्ष्य मिलते हैं। एक अभिलेख में बौद्ध भिक्षुओं के भरण-पोषण हेतु सिक्कों और अनाज से भरे भण्डार घर का वर्णन है। जाहिर है कि स्थानीय किसान इतना उत्पादन कर लेते थे कि उसके एक हिस्से से करों का भुगतान कर सकें और दान-दक्षिणा भी दे सकें। इस क्षेत्र के लोग प्राकृत भाषा जानते थे और बौद्ध धर्म के अनुयाई थे। इसी प्रकार, दक्षिण-पूर्व बंगाल में नोआखली में मिले एक अभिलेख से संकेत मिलता है कि ई.पू. दूसरी शताब्दी में यहाँ के लोग प्राकृत और ब्राह्मी लिपि जानते थे। हालाँकि, चौथी शताब्दी तक बंगाल के बड़े हिस्से के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। चौथी शताब्दी के मध्य में, ‘महाराज’ की पदवी वाले एक राजा ने बाँकुरा जिले के दामोदर के पोखराना में शासन किया। वे संस्कृत जानते थे और विष्णु-भक्त थे। विष्णु-पूजा के लिए उन्होंने सम्भवतः एक गाँव दान में दिया था।
गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच स्थित क्षेत्र, जो अब बांग्लादेश तक फैला है, पाँचवीं और छठी शताब्दियों में भली-भाँति बसाहट वाले क्षेत्र थे और वहाँ संस्कृत भाषा एवं उसकी शिक्षा का प्रारम्भ हो चुका था। सन् 550 के बाद स्वतन्त्र हो गए गुप्त काल के राज्यशासकों ने, उत्तरी बंगाल पर कब्जा कर लिया। और इसके कुछ हिस्सों को कामरूप के शासकों ने हथिया लिया। इसी समय सामन्त महाराज कहलाने वाले स्थानीय सामन्त राजवंशों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता कायम कर ली और स्थानीय किसानों से लड़ने के लिए घोड़ा, हाथियों, पैदल सेनाओं और नौकाओं से युक्त अपने सैन्य संगठन का निर्माण किया। सन् 600 तक यह क्षेत्र गौड़ के रूप में जाना जाने लगा और हर्ष के शत्रु शशांक ने यहाँ स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की।
सन् 432-33 से लेकर एक शताब्दी तक लगभग पूरे उत्तर बंगाल तक फैले पुण्ड्ववर्धन भुक्ति में, जिसका अधिकतर भाग अब बांग्लादेश में है, ताम्र-पत्र पर दर्ज भूमि विक्रय और अनुदान के दस्तावेज मिलते हैं। भूमि के लेन-देन की अधिकांश प्रक्रिया से संकेत मिलता है कि स्वर्ण मुद्रा या दीनार देकर भूमि खरीदी जाती थी। हालांकि, धार्मिक उद्देश्यों के लिए दी गई भूमि पर कोई कर का भुगतान नहीं करना पड़ता था। भूमि लेन-देन में प्रमुख लिप्यकार, व्यापारी, कारीगर, जमीन्दार वर्ग और स्थानीय प्रशासन की भागीदारी दिखती है, जिन्हें गुप्त काल के राजाओं द्वारा नियुक्त शासक संचालित करते थे। भूमि बिक्री के दस्तावेज न केवल विभिन्न सामाजिक वर्गों एवं स्थानीय कार्यकर्ताओं के अस्तित्व का संकेत देते हैं, बल्कि कृषि के विस्तार पर उल्लेखनीय प्रकाश भी डालते हैं। सामान्यतः, धार्मिक अनुदान के लिए खरीदी गई भूमि को क्रमशः बंजर और गैर-आबाद बताया गया है इसलिए, अनुदान वाले भू-खण्डों को खेती और बसावट के दायरे में लाने के उद्देश्य से इस पर कर नहीं लगाया जाता था।
बंगाल में बने ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र को समतट कहा जाता है, जिसे समुद्रगुप्त ने चौथी सदी में जीतकर अपने अधीन कर लिया था, उस समय यह क्षेत्र दक्षिण-पूर्व बंगाल तक फैला था। इस क्षेत्र के एक हिस्से की आबादी घनी थी, जिसने गुप्त सम्राट को अपनी तरफ आकर्षित किया होगा। हालाँकि, यह क्षेत्र सम्भवतः ब्राह्मणवादी शासकों द्वारा शासित नहीं था, क्योंकि यहाँ पर उत्तरी-बंगाल की तरह न तो संस्कृत का इस्तेमाल होता था, न ही वर्ण व्यवस्था का प्रचालन था। सन् 525 से, इस क्षेत्र में समतट और समतट की पश्चिमी सीमा तक फैले वंगा के एक हिस्से व्यवस्थित एवं संगठित राज्य विकसित हुआ, जिसे समतट या वंगा का राज्य कहा जाता है, जिसके शासक साम हरदेव ने, छठी शताब्दी के उत्तरार्ध में पर्याप्त संख्या में सोने के सिक्के जारी किए।
सातवीं शताब्दी में, ढाका क्षेत्र में खड्गों अर्थात् तलवारबाजों का राज था। इसके अलावा, कोमिला क्षेत्र में लोकनाथ नामक एक ब्राह्मण सामन्त का राज्य औरराट वंश का राज्य था। दक्षिण-पूर्व और मध्य बंगाल के इन सभी शासकों ने छठी-सातवीं शताब्दियों में जमीनें दान की। उड़ीसा के राजाओं की तरह उन्होंने भी अग्रहारों की व्यवस्था की। भूमि दस्तावेजों में संस्कृत का विकास देखने को मिलता है। जिसमें सातवीं सदी के उत्तरार्ध में कुछ परिष्कृत छन्दों का भी उपयोग किया गया है। साथ ही, वे खेती और ग्रामीण बस्तियों के विस्तार की भी पुष्टि करते हैं। बंगाल और उड़ीसा के बीच सीमावर्ती इलाकों में दण्डभुक्ति नामक एक राजकोषीय और प्रशासनिक इकाई का गठन किया गया। दण्ड का मतलब सजा और भक्ति का मतलब आनन्द है। प्रतीत होता है कि यह इकाई उस क्षेत्र के आदिवासियों के सजा देने और सुधारने के उद्देश्य से बनाई गई थी। इन क्षेत्रों में संस्कृत और संस्कृति के अन्य तत्त्वों को बढ़ावा मिला। यह बात वर्धमानभुक्ति (बर्दवान) के बारे में भी सच प्रतीत होती है, जिन्हें हम छठी शताब्दी में ही जान पाते हैं। दक्षिण-पूर्व बंगाल के फरीदपुर क्षेत्र में, बौद्ध विहार को दी गई पाँच किता भूखण्ड को बंजर और जल में डूबी रहने वाली बताया गया, जिससे उन्होंने इसके लिए राज्य को कोई कर नहीं दिया। इसी तरह, कोमिल्ला जिले में, हिरनों, सुअरों, भैंसों, बाघों, साँपों एवं अन्य जन्तुओं से भरे वन-क्षेत्र में, 200 ब्राह्मणों को एक बड़ा क्षेत्र दिया गया। ऐसे सारे उदाहरण नए क्षेत्रों बसाहट और सभ्यता की प्रगति के पर्याप्त प्रमाण देते हैं।
पाँचवीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लगभग दो शताब्दियों तक का समय बंगाल के इतिहास में बहुत महत्त्वपूर्ण है। ब्राह्मणवाद की प्रगति और बौद्ध धर्म का उदय इसी दौरान हुआ। प्रारम्भिक शताब्दियों में बुद्ध की मूर्तियाँ नहीं के बराबर दिखतीं हैं; बाद में वे बोधगया, साँची, मथुरा और गान्धार में पाई गईं और पाँचवीं शताब्दी में बंगाल के कई स्थानों पर प्रतिमाएँ स्थापित की गईं। मध्ययुग के प्रारम्भिक काल में, न केवल बिहार बल्कि उत्तरी बंगाल में भी बौद्ध विहारों की स्थापना हुई। पाँचवीं और सातवीं शताब्दी के बीच लगभग आधे दर्जन बड़े-छोटे राज्यों का गठन हुआ, जिनमें कुछ स्वतन्त्र, कुछ सामन्तवादी थे। हालाँकि, इनमें से प्रत्येक का अपना विजय या सैन्य शिविर होता था, जहाँ उनके पैदल सेना, घुड़सवार, हाथी और नौकाएँ थीं। प्रत्येक के पास राजकोषीय और प्रशासनिक जिलों में कर संचय और कानून व्यवस्था के रख-रखाव के तन्त्र थे। युद्ध द्वारा और बौद्धों एवं ब्राह्मणों को भूमिदान देकर राज्य अपना विस्तार करते थे। इनकी सम्पत्ति में इतनी बढ़ोतरी हुई कि अन्ततः उसकी देखभाल के लिए एक अधिकारी अग्रहारिका नियुक्त करना पड़ा। भूमिदान से गाँवों का विस्तार हुआ और नए-नए भूमि अधिकार बने। आम तौर पर, भूमि पर व्यक्तिगत परिवारों का स्वामित्व था, लेकिन इसकी बिक्री एवं खरीद स्थानीय समुदायों के प्रमुख कारीगरों, व्यापारियों, जमीन्दारों और शासकों के पूर्ण नियन्त्रण में थी। यह वर्चस्वशाली समूह राजा के स्थानीय अधिकारियों की भी सहायता करता था। हालाँकि, गाँव में जमीन की बिक्री के लिए सामान्य किसानों से भी परामर्श लिया जाता था। ऐसा लगता है कि मूल रूप से भूमि की खरीद-बिक्री समुदाय की सहमति के बिना सम्भव नहीं थी। इसलिए, जब भूमि के वास्तविक मालिक यानि स्थानीय व्यक्ति भी किसी को धार्मिक उद्देश्यों के लिए भूमि उपहार में देता था तो भी समुदाय की सहमति आवश्यक होती थी, जो कि समुदाय का हक माना जाता था। प्राचीन समय में सम्भवतः, लोगों ने धार्मिक सेवाओं के लिए पुरोहितों को भूमिदान और सैन्य एवं राजनीतिक सेवाओं के लिए शासकों को कर का भुगतान किया। बाद में राजा ने इन समुदायों से जमीन का अधिकांश हिस्सा अपने अधीन कर लिया जिससे भूमि दान का अधिकार स्वयं के हाथ में आने से राजा दम्भ से भर उठे। अब न सिर्फ अधिकतर जमीनों के कर पर राजा का अधिकार था बल्कि वे खाली और बंजर भूमि के भी मालिक होते थे। हर राज्य के प्रशासनिक अधिकारी अधिकारिक भाषा संस्कृत जानते थे। वे पुराणों और धर्मशास्त्रों की शिक्षा से भी परिचित थे। इस क्षेत्र की सभ्यता के विकास के साक्षी के रूप में यह समय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।
असम
पूरब से पश्चिम तक फैली ब्रह्मपुत्र घाटी के किनारे बसा कामरूप, सातवीं शताब्दी में प्रकाश में आया। हालाँकि, गुवाहाटी के पास अम्बरी के उत्खनन में पता चला है कि यहाँ पर बस्तियाँ, ईसा युग की चौथी शताब्दी से ही बस चुकी थीं। उसी शताब्दी में समुद्रगुप्त ने डवाक और कामरूप से कर वसूल किए थे। सम्भवतः डवाक नवगाँव जिले का और कामरूप ब्रह्मपुत्र घाटी के मैदान का नाम था। समुद्रगुप्त को कर सौंपने वाले शासक, कबीलाई किसानों से कर वसूलने वाले प्रमुख थे।
गुवाहाटी के पास अम्बरी में हुए उत्खनन से स्पष्ट होता है कि छठी-सातवीं शताब्दी में बस्तियाँ काफी विकसित थीं, जिसके प्रमाण अभिलेखों से भी मिलते हैं। छठी शताब्दी की शुरुआत तक, संस्कृत भाषा और लेखन कला के उपयोग के प्रमाण मौजूद हैं। कामरूप राजाओं ने अपनी उपाधि वर्मन रखी, जिसे न केवल उत्तरी, मध्य और पश्चिमी भारत में, बल्कि बंगाल, उड़ीसा, आन्ध्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी अंगीकार किया गया। इस उपाधि या पदवी का अर्थ हथियारबन्द या कवच होता था; जो योद्धा होने का प्रतीक था। यह पदवी मनु द्वारा क्षत्रियों को दी गई थी। क्षत्रिय लोगों ने ब्राह्मणों को भूमि दान के माध्यम से अपनी स्थिति को और मजबूत किया। सातवीं शताब्दी में भास्करवर्मन एक राजा के रूप में उभरे, जो ब्रह्मपुत्र घाटी के एक बड़े हिस्से और इसके आगे के कुछ इलाकों को भी नियन्त्रित करते थे। यहाँ बौद्ध धर्म ने भी अपनी पकड़ मजबूत की और चीनी यात्री व्हेनत्सांग ने इस राज्य का दौरा किया।
रचनात्मक काल
पूर्वी भारत के विभिन्न हिस्सों को बेशक अलग-अलग समय पर महत्त्व मिला, किन्तु चौथी से सातवीं शताब्दी तक का समय रचनात्मक काल का चरण था। इस दौरान, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के कुछ हिस्सों और असम में लेखन, संस्कृत शिक्षण, वैदिक अनुष्ठान, ब्राह्मणवादी सामाजिक वर्ग और राज्य प्रणाली आदि फैले और विकसित हुए। गुप्त साम्राज्य के साथ सांस्कृतिक सम्पर्क ने पूर्वी क्षेत्र में सभ्यता के प्रसार को और अधिक बढ़ाया। उस समय उत्तर बंगाल और उत्तर-पश्चिम उड़ीसा में गुप्त शासन था। इन प्रदेशों के अभिलेखों में गुप्तसंवत के उपयोग से गुप्त शासन से इनके संपर्क एवं गुप्त के प्रभाव का अनुमान लगाया जा सकता है। सामन्तवादियों ने बंगाल में नए राज्यों का गठन किया, जिन्होंने अपने सैन्य शिविरों में पर्याप्त संख्या में हाथी, घोड़े, नौकाएँ आदि की व्यवस्था की। इन वेतनभोगी सेनाओं के संचालन हेतु उन्होंने स्पष्ट रूप से ग्रामीण समुदायों से नियमित कर संचय किए। पहली बार, पाँचवीं और छठी शताब्दियों में स्पष्ट रूप से बड़े पैमाने पर लेखन हुआ, जिसमें संस्कृत का इस्तेमाल वर्ण आधारित समाज के गठन के साथ बौद्ध धर्म के विकास हुआ। इसके अलावा इस क्षेत्र में ब्राह्मणवाद के विकास के रूप में शैववाद एवं वैष्णववाद को भी बढ़ावा मिला। हालाँकि, भूमि पर सामुदायिक प्रभाव जारी थे किन्तु निजी भूमि की व्यवस्था का प्रचलन था, जिसे सोने के सिक्कों से इसे खरीदा जा सकता था। यह सब एक उन्नत खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था के परिचायक हैं। स्पष्टतः यह हल की जुताई से और धान को रोप कर की जाने वाली खेती के साथ ही विभिन्न प्रकार के शिल्प ज्ञान पर आधारित था। कालिदास ने वंगा में धान की रोपनी का वर्णन किया है लेकिन हमें यह नहीं पता चल पाता है कि यह पद्धति स्थानीय थी या मगध से आई हुई। उत्तर बंगाल ने उच्च गुणवत्ता वाले गन्ना का उत्पादन किया। जिससे नागरिक और सरकार, दोनों का सम्पोषण हुआ। अपेक्षाकृत कम आबादी वाली जगहों में बड़े पैमाने पर ग्रामीण बस्तियों को बढ़ावा दिया। यद्यपि उस समय के राजकुमारों, राजवंशों, सामन्तों और केन्द्रीय सत्ता की स्पष्ट रूपरेखा बताना सम्भव नहीं है, लेकिन पूर्वी क्षेत्र के बाहरी प्रान्तों में संस्कृति और सभ्यता के विकास के बारे में कोई सन्देह नहीं है।
गुप्त साम्राज्य के पतन के साथ ही इन बाहरी प्रान्तों में काफी प्रगति हुई। कई अनजान क्षेत्र, जो कि सम्भवतः कबीलाई प्रमुखों द्वारा शासित थे और कम आबादी वाले थे, उभरकर सामने आए। जैसे पश्चिम बंगाल, उत्तर उड़ीसा और मध्य प्रदेश के आस-पास लाल मिट्टी वाले इलाकों में हुआ। जो झारखण्ड का हिस्सा था और यहाँ खेती करने और जीवन बसाने में कठिनाई थी। बाद में समृद्ध क्षेत्र बनकर उभरा। ऐसा ही जलोढ़ मिट्टी और भारी वर्षा वाले जंगली क्षेत्रों पर भी देखा गया।
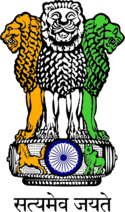
Hey guys, just tried out fortunegodsvn. Seeing some decent action there! Definitely worth checking out if you’re looking for something new to play. Link is fortunegodsvn