प्राचीन काल से मध्यकाल (प्राचीन भारत का इतिहास)
संकट और कृषि परिवर्तन
चीन भारतीय समाज को मध्ययुगीन समाज में बदलने की मुख्य कारक अन्ततः प्राभूमि अनुदान प्रथा ही थी। यह सहाज में बदलने की मुख्य कारक अन्ततः के दस्तावेज बताते हैं कि दान करने वाले मुख्यतः राजा होते थे जो पुण्य प्राप्ति समाज में धार्मिक स्वीकृति चाहते थे और दान प्राप्तकर्ता मुख्यतः भिक्षु एवं पुजारी होते थे जिन्हें धार्मिक अनुष्ठानों हेतु संसाधनों की आवश्यकता होती थी। यह प्रथा वस्तुतः एक प्राचीन सामाजिक व्यवस्था के गम्भीर संकट के कारण अस्तित्व में आई। वर्णभेद समाज उत्पादक गतिविधियों पर आधारित था, किसान वैश्य एवं श्रमिक शूद्र कहलाते थे। राजकीय अधिकारियों द्वारा वैश्यों से संगृहीत करों से राजा अपने अधिकारियों और सैनिकों को वेतन, पुजारियों को पुरस्कार तथा व्यापारियों एवं समृद्ध कारीगरों से विलासी एवं अन्य वस्तुएँ खरीदने में सक्षम हुए। हालाँकि, इस व्यवस्था को तीसरी-चौथी शताब्दियों में, पुराणों में वर्णित एक गहरे सामाजिक संकट कलियुग ने घेर लिया। समकालीन पौराणिक ग्रन्थों में एक ऐसी स्थिति का वर्णन है, जिसमें विभिन्न वर्ण या सामाजिक वर्गों ने जाति आधारित किए जाने वाले कार्य करने से मना कर दिया। निम्न वर्ग उच्च वर्गों जैसा बनने के लिए अपने पेशेवर काम को छोड़ने लगे। दूसरे शब्दों में, उन्होंने करों के भुगतान और मुफ्त श्रमदान से इनकार कर दिया। इस कारण वर्णसंकर या सामाजिक वर्गों के मिश्रण की स्थिति आ गई। ऐसे विभिन्न वर्गों पर हमले किए गए, क्योंकि भारी करों और लगानों के द्वारा उत्पादन से जुड़े हुए लोगों का दमन हो रहा था और उनकी सुरक्षा के लिए राजाओं का संरक्षण भी प्राप्त नहीं था। तीसरी-चौथी शताब्दियों के पुराणों में इसे कलियुग कहा गया है।
इस संकट से उबरने के लिए कई उपाय किए गए। मनु के लगभग सभी समकालीन विधान-ग्रन्थ का कहना था कि वैश्यों और शूद्रों को उनके कर्तव्यों से हटने नहीं देना चाहिए। लिहाजा ऐसे समुदायों के दुबारा उनके काम में लगाने के लिए दमनकारी कदम उठाए गए। किन्तु ऐसी स्थिति को सँभालने का सबसे कारगर तरीका पुजारियों और अधिकारियों को वेतन और पारिश्रमिक के बदले भूमिदान देना था। इस प्रथा के अन्तर्गत, दान दिए गए क्षेत्र में, कर एवं लगान वसूलने तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व सीधे अनुदान भोगियों के हाथ में आ गया जो मौके पर ही विरोधी किसानों से निपट सकते थे। दूसरा इससे बंजर पड़ी जमीनों को भी कृषि योग्य बनाया गया। इसके अलावा, विजित कबीलाई क्षेत्रों में ब्राह्मणों को बसाया गया। और इन ब्राह्मणों द्वारा कबीलाई लोगों को ब्राह्मणवादी जीवन शैली, राजा द्वारा दिए गए आदेशों का अनुपालन तथा निर्धारित करों का भुगतान सिखाया जाने लगा।
जमीन्दारी प्रथा का उदय
पाँचवीं शताब्दी में भूमि अनुदान की प्रथा ने जोर पकड़ा और इस प्रथा के अनुसार, ब्राह्मणों को राजा द्वारा कर-मुक्त गाँव दिए जाते थे, जहाँ पहले राजा कर वसूलते थे। किन्तु अनुदान में मिलने के बाद इन ब्राह्मणों को गाँवों में रहने वाले लोगों को नियन्त्रित करने का अधिकार स्वतः मिल जाता था। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को इन अनुदानित गाँवों में प्रवेश की अनुमति नहीं होती थी। पाँचवीं शताब्दी तक, चोरों को दण्डित करने का जो अधिकार राजा के पास होता था, अपराधियों को दण्डित करने का वही अधिकार लाभार्थियों को दे दिया गया। इस प्रकार, ब्राह्मणों ने दान में प्राप्त गाँवों में, न केवल किसानों एवं कारीगरों से कर संग्रह किए, बल्कि कानून व्यवस्था का भी संचालन किया। इस प्रकार अनुदान में गाँव देने की प्रक्रिया यहाँ तक पहुँच गई कि जिसके परिणामस्वरूप राजा की शक्ति गुप्त काल के आखिर तक बहुत कमजोर हो गई थी। मौर्य काल में राजा के अधिकारियों द्वारा कर-निर्धारण एवं कर-संग्रह किया जाता था और वे ही कानून व्यवस्था बनाते और चलाते थे। भूमि अनुदान राजा की बढ़ती शक्ति का प्रमाण था। इसके अतिरिक्त वैदिक काल में भी, राजा को मवेशियों का मालिक या गोपति माना जाता था, लेकिन गुप्त काल और उसके बाद उन्हें भूपति या भूमि का मालिक माना जाने लगा। हालाँकि, भूमि अनुदान ने राजा के अधिकार और शक्ति को अन्ततः कमजोर ही किया और राजकीय नियन्त्रण से मुक्त व्यवस्था का उदय हुआ।
सरकारी अधिकारियों को भूमि अनुदान दिए जाने से शाही नियन्त्रण में और ह्रास आया। जबकि मौर्य काल में, राज्य के अधिकारियों को सामान्यतः नकद भुगतान होता था। कुषाणों ने भी बड़ी संख्या में ताम्बे एवं सोने के सिक्के जारी किए; जाहीर है उनके राज्य में भी ऐसा ही था। गुप्त काल में भी, सोने के सिक्के सेना एवं उच्च अधिकारियों के भुगतान के लिए ही होते थे। किन्तु यह स्थिति, छठी शताब्दी के बाद बदल गई। उस समय के दस्तावेजों में सेवाओं के बदले पुरस्कार में जमीन दिए जाने का प्रावधान दिखाई देता है। तदनुसार, हर्षवर्धन के शासनकाल में, राजकीय अधिकारियों को भूमि राजस्व द्वारा भुगतान किया जाता था और एक चौथाई राजकीय राजस्व राज्य में जनता की भलाई के लिए निर्धारित किया जाता था। राज्यपाल, मन्त्री, न्यायिक अधिकारी जैसे अन्य अधिकारियों को उनकी व्यक्तिगत सुविधाओं की पूर्ति के लिए जमीन के हिस्से दिए जाने लगे। जिससे बाद में इन नए उभरे जमीन्दारों पर राज्य को दरकिनार कर स्वार्थ हावी होने लगे। इस प्रकार, सातवीं शताब्दी तक, जमीन्दारी प्रथा का भरपूर विकास और केन्द्रीय राज्य सत्ता का हास हो गया।
नई कृषि अर्थव्यवस्था
कृषि अर्थव्यवस्था में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव दिखा। भूमि के लाभार्थी खुद न तो जमीन पर खेती कर सकते थे, न ही राजस्व की वसूली। खेती यथार्थतः किसानों को सौंप दी गई, जो जमीन से जुड़े तो थे, लेकिन कानूनन वे उसके मालिक नहीं थे। चीनी तीर्थयात्री इत्सिंग लिखते हैं कि ज्यादातर भारतीय विहारों ने अपनी भूमि पर मजदूरों और अन्य लोगों द्वारा खेती करवाई। व्हेन त्सांग शूद्रों का वर्णन कृषिकर्मियों के रूप में करते हैं, जिससे पता चलता है कि वे भूमि पर खेती दास या कृषि मजदूरों के रूप में नहीं, बल्कि बाद में अस्थायी तौर पर मालिक के रूप में खेती करने लगे। यह स्पष्ट रूप से उत्तर भारत के पुराने बसे क्षेत्रों में हुआ।
कबीलाई क्षेत्रों में जब गाँव दान किए गए थे, तो कृषकों को धार्मिक लाभार्थियों, विशेषकर ब्राह्मणों के नियन्त्रण में रखा गया था, क्योंकि पाँचवीं-छठी शताब्दी के बाद से बड़े पैमाने पर ब्राह्मणों को भूमिदान देने की शुरुआत हुई। छठी शताब्दी के बाद से, किसानों को खास तौर पर उड़ीसा और दक्कन के उस पिछड़े एवं पहाड़ी इलाकों में रहने को कहा गया, जहाँ की जमीन लाभार्थियों को दी गई थी। वहाँ से यह प्रथा गंगा घाटी तक फैली। उत्तर भारत में भी, कारीगरों और किसानों को कहा गया, कि वे अनुदान में मिले गाँवों में ही निवास करें। इस तरह उन्हें एक गाँव से दूसरे गाँव जाने पर रोक लग गई। स्पष्टतः इससे लोगों की गतिशीलता बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई।
व्यापार और शहरों का पतन
छठी शताब्दी से, व्यापार में तेज गिरावट शुरू हुई। यद्यपि तीसरी शताब्दी में ही, रोमन साम्राज्य के मुख्य हिस्से से व्यापार बन्द हो गया। छठी शताब्दी के मध्य में, ईरान एवं बायजेन्टियम के साथ भी रेशम-व्यापार बन्द हो गया। हालांकि भारत ने चीन और दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ कुछ व्यापार कायम रखे, किन्तु बिचौलियों के रूप में इसका ज्यादातर लाभ अरब को ही हुआ। सामन्ती व्यवस्था में, सैन्य जरूरतों के हिसाब से घोड़े का व्यापार अधिक महत्त्वपूर्ण हो गया। छठी शताब्दी में, फारस से घोड़े का आयात किया गया। इसके लिए व्यापारियों को आयात कर नहीं देना पड़ता था। इस्लाम के उदय से पहले, भारत के निर्यात व्यापार पर अरबों का लगभग एकाधिकार सा हो गया था। भारत में इस दौरान के सोने के सिक्के की अनुपस्थिति से अनुमान लगाया जा सकता है कि छठी शताब्दी के बाद 300 से भी अधिक वर्षों तक व्यापार में आश्चर्यजनक गिरावट हुई थी। छठी शताब्दी के बाद धातु के सिक्कों की कमी न केवल उत्तर भारत, बल्कि दक्षिण भारत के लिए भी यथार्थ है।
व्यापार के पतन से नगरों का भी पतन शुरू हो गया। जबकि सातवाहनों और कुषाणों के काल में पश्चिम और उत्तर भारत के नगरों का विकास हुआ था। कुछ नगरों का विकास गुप्त काल में भी हुआ। हालांकि, उत्तर-गुप्त काल के बाद उत्तर भारत के कई पुराने व्यापारिक नगर नष्ट हो गए। खुदाई से पता चलता है कि हरियाणा और पूर्वी पंजाब, पुराना किला (दिल्ली), मथुरा, हस्तिनापुर (मेरठ जिला), श्रावस्ती (यूपी), कौशाम्बी (इलाहाबाद के पास), राजघाट (वाराणसी), चीरन्द (सारण जिला), वैशाली और पाटलीपुत्र का पतन गुप्त काल से ही शुरू हुआ और उत्तरवती गुप्त काल में ये लगभग गायब ही हो गए। चीनी तीर्थयात्री व्हेन त्सांग ने बुद्ध से जुड़े होने के कारण पवित्र माने जाने वाले इनमें से कुछ शहरों का दौरा किया, जो कि उस समय तक निर्जन और खण्डहरों में तब्दील हो गए थे। भारतीय उत्पादन के निर्यात के लिए बाजार सीमित हो गए थे। जिसके कारण इन नगरों में रहने वाले कारीगर और व्यापारी ग्रामीण इलाकों में जाकर खेती करने लगे। पाँचवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, पश्चिमी तट से रेशम बुनकरों का एक समूह मालवा के मन्दसौर चला गया और अपना परम्परागत रेशम बुनाई कार्य को छोड़कर अन्य दूसरे व्यवसायों को अपना लिया। व्यापार और नगरों के पतन के कारण, ग्रामीणों को स्वयं तेल, नमक, मसाले, कपड़े, आदि की अपनी जरूरतों को पूरा करना होता था। जिससे आगे चलकर, इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उत्पादन की छोटी इकाइयों का जन्म हुआ।
इस स्थिति में अधिकांश व्यापारी कृषक हो गए, लेकिन कुछ लोगों को राजा द्वार भूमि प्रशासन के लिए प्रबन्धक भी नियुक्त किया गया। मन्दिरों और ब्राह्मणों की तरह, कुछ व्यापारियों को राजा द्वारा गुप्त और उत्तरवर्ती गुप्त काल में जमीन भी दी गई थी। ऐसे मामलों में, वे अपनी जमीन की देखभाल के साथ मन्दिरों और विहारों की भूमि अनुदान की भी देख-रेख करते थे, जिसका उन्हें न्यासी या प्रबन्धक नियुक्त किया गया था। इस प्रकार जमीन्दारों के रूप में व्यापारियों के उदय का एक कारण व्यापार एवं शहरों का पतन भी था।
वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन
छठी शताब्दी से, सामाजिक संगठन में कुछ परिवर्तन हुए। उत्तर भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में, वैश्यों को स्वतन्त्र किसान माना जाता था। लेकिन भूमि अनुदान ने किसान और राजा के बीच जमीन्दारों की एक श्रेणी पैदा की। लिहाजा किसान वैश्य, शूद्र के स्तर पर चले गए। इससे पुरानी ब्राह्मणवादी व्यवस्था में तब्दीली आई। ब्राह्मणों के लिए किए गए भूमिदान के ही परिणामस्वरूप यह व्यवस्था पाँचवीं-छठी शताब्दी में, उत्तर भारत से फैलकर बंगाल और दक्षिण भारत पहुँची। और इस तरह विस्तृत क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर दो ही श्रेणियाँ रह गई थीं-ब्राह्मण और शूद्र।
सत्ता एवं भूमि अनुदान की निरन्तर गतिविधियों से कई भू-धारक समुदायों का उदय हुआ। व्यक्ति को ज्योंही भूमि और सत्ता मिली, स्वभावतः उन्होंने समाज में उच्च स्थान की अपेक्षा की। जबकि वे निम्न वर्ण के थे, किन्तु मालिकों से उन्हें पर्याप्त भूमि अनुदान भी मिला। इससे समस्या उत्पन्न हुई, क्योंकि वे आर्थिक रूप से सम्पन्न तो थे, मगर सामाजिक, पारम्परिक रूप से निम्न वर्ण के ही थे। धर्मशास्त्रों के अनुसार, सामाजिक व्यवस्था का संचालन वर्ण व्यवस्था से ही नियन्त्रित था। लोगों को चार वर्षों में विभाजित किया गया था, जिसमें ब्राह्मण सबसे ऊँचे और शूद्र सबसे निम्न थे। व्यक्ति का आर्थिक अधिकार भी उसके वर्ण से निर्धारित किया जाता था। इसलिए नए भू-धारक समुदायों को उपयुक्त स्थान देने के लिए पूर्व लिखित ग्रन्थों में कुछ बदलाव जरूरी समझे गए। छठी शताब्दी के एक ज्योतिषी, वराहमिहिर ने वर्षों के अनुसार घरों के आकारों का निर्णय किया, जैसे प्राचीन काल में होते थे साथ ही उन्होंने शासकीय प्रमुखों के विभिन्न वर्गों के घरों के आकार भी उनके पद के अनुसार तय किए। इस प्रकार, पूर्वकालीन समाज में सभी चीजों का वर्गीकरण
वर्ण पर आधारित था, लेकिन यहाँ यह व्यक्ति की भूमि सम्पन्नता के अनुसार तय होने लगा। हालाँकि, कुछ कानून संहिताओं ने नियोग या विधवा पुनर्विवाह की अनुमति दी थी, किन्तु ये रियायतें निम्न वर्ग की महिलाओं तक ही सीमित थी। शुरू से ही, महिलाओं को सम्पत्ति के अधिकारों से वंचित किया गया था और अचल सम्पत्ति पर उनका कोई अधिकार नहीं था।
सातवीं शताब्दी के बाद से कई जातियों का निर्माण हुआ। आठवीं शताब्दी का एक पुराण बताता है कि वैश्य महिलाओं के निम्न जातियों के पुरुषों से सम्बन्ध के फलस्वरूप हजारों मिश्रित जातियाँ उत्पन्न हुईं। इसका अर्थ था कि शूद्र और अछूत अनगिनत उप-जातियों में बँटे हुए थे, सातवीं शताब्दी के आस-पास ऐसा ही ब्राह्मणों और राजपूतों के साथ भी था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकने कि वजह से भी अर्थव्यवस्था की प्रकृति के अनुसार जातियों की संख्या में वृद्धि हुई। यद्यपि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने एक ही व्यवसाय का पालन किया, फिर भी वे अपने इलाकों के प्रभाव में विभिन्न उप-जातियों में विभाजित हुए। इसके अलावा, भूमि अनुदान के बाद कबीलाई क्षेत्रों में बसे ब्राह्मण समाज में कबीलाई समूहों का मिश्रण हुआ। जिनमें से ज्यादातर लोग शूद्र और मिश्रित जातियों के रूप में जाने जाते थे। अब प्रत्येक जनजाति या कुटुम्ब समूह को ब्राह्मण समाज में एक अलग जाति का दर्जा मिल गया।
क्षेत्रीय अस्मिताओं का उदय
छठी-सातवीं सदी के आस-पास, देश में कई सांस्कृतिक इकाइयों का निर्माण शुरू हुआ, जिसे बाद में कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु आदि के रूप में जाना जाने लगा। विभिन्न सांस्कृतिक समूहों की पहचान भारतीय और विदेशी दोनों में स्वीकारी गई है। चीनी यात्री व्हेन त्सांग ने कई उपराष्ट्रीय समूहों या लोगों का उल्लेख किया है। आठवीं सदी के उत्तरार्ध में जैन ग्रन्थों ने अठारह प्रमुख उपराष्ट्रीयताओं के अस्तित्व की चर्चा की है। जिनमें से सोलह की शारीरिक विशेषताओं का भी वर्णन है। नौवीं शताब्दी के आस-पास के लेखक विशाखदत्त ने अलग-अलग क्षेत्रों के आधार पर लोगों या समूहों के रीति-रिवाजों, वस्त्र, भाषा और स्वभाव आदि में भिन्नता का जिक्र किया है।
सातवीं शताब्दी के बाद, भारत के भाषाई इतिहास में एक उल्लेखनीय विकास हुआ, अपभ्रंश का जन्म। यह भाषा पहले की तरह की आधी प्राकृत थी और आधी बाद में आई आधुनिक इण्डो-आर्यन। यह सन् 600 से 1000 के बीच फैली थी। इस काल के अन्त में इस भाषा में व्यापक जैन साहित्य लिखा गया। आधुनिक भाषाओं की झलकियाँ अपभ्रंश में लिखे गए इन जैन एवं बौद्ध साहित्य, दोनों में मिलती हैं। पूर्वी भारत के बौद्ध लेखन में बंगाली, असमिया, मैथिली, ओड़िया और हिन्दी की झलकें दिखाई पड़ती हैं। इसी प्रकार, इस काल के जैन साहित्य गुजराती और राजस्थानी की भी शुरुआत को दर्शाते हैं।
दक्षिण में, तमिल सबसे पुरानी भाषा थी, लेकिन कन्नड़ का विकास इस समय शुरू हो गया था। तेलुगु और मलयालम बहुत बाद में विकसित हुआ। ऐसा लगता है कि एक दूसरे से अलग होने के कारण, प्रत्येक क्षेत्र ने अपनी अलग भाषा विकसित की। जब गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, तो कई स्वतन्त्र अधिराज्यों में बढ़ोतरी हुई और इसने स्वाभाविक रूप से देशव्यापी सम्पर्क और संचार में बाधा पहुँचाई। व्यापार में गिरावट का मतलब विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के बीच संचार की कमी थी और इसने क्षेत्रीय भाषाओं के विकास को बढ़ावा दिया होगा।
सातवीं शताब्दी में, एवं उसके बाद, क्षेत्रीय लिपि अधिक प्रमुख हो गई। मौर्य काल से गुप्त काल तक, कमोवेश एक ही लिपि का प्रयोग भारत के बड़े हिस्से में होता रहा। इस प्रकार, जिस व्यक्ति ने गुप्त काल की लिपि का अध्ययन किया हो, वह देश के विभिन्न हिस्सों में उस अवधि के अभिलेख पढ़ सकते हैं, लेकिन सातवीं शताब्दी के बाद से हर क्षेत्र की अपनी अलग लिपि है और इसलिए उत्तरवर्ती गुप्त काल के विभिन्न भागों के अभिलेखों को, क्षेत्रीय लिपियों को सीखे बिना पढ़ पाना सम्भव नहीं है।
साहित्य की प्रवृत्तियाँ
साहित्य के इतिहास में, छठी और सातवीं शताब्दी समान रूप से महत्त्वपूर्ण हैं। दूसरी शताब्दी से शासक वर्ग द्वारा संस्कृत का प्रयोग होता रहा। सामन्तों की शानो-शौकत, दिखावा और भव्यता के अनुरूप ही संस्कृत पद्य और गद्य की शैली अलंकृत हुई। लेखन रूपकों, कल्पनाओं, विशेषणों और क्रिया-विशेषों से परिपूरित हो गया, जिससे पाठक के लिए इसके गूढ़ अर्थों को समझना मुश्किल हो गया। बाण के गद्य इसके विशिष्ट उदाहरण हैं। कविता में, नई अलंकृत, शब्दबाहुल्य, उन्नत शैली की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कई छन्दों का आविष्कार हुआ। सामाजिक पदानुक्रम एवं धनाढ्यों के प्रभुत्व के अनुसार, कृत्रिम गद्य और पद्य, अभिजात वर्ग के लेखकों की जीवन शैली बन गई। जिन्होंने जमीन्दारों और किसानों के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया। कौशाम्बी ने लैंगिकता एवं धर्म के संयोजन से उत्पन्न सामन्ती साहित्य की विशेषताओं पर विचार किया है। भू-धारकों के एक वर्ग द्वारा लैंगिकता एवं तन्त्रवाद पर लिख रहे लेखकों का समर्थन किया गया। जिसमें लैंगिक सम्मिलन में परम दिव्य शक्ति से मिलन की स्थिति देखी जाने लगी। वज्रयानी तान्त्रिकों के अनुसार, पुरुष एवं स्त्री के यौन सम्मिलन से ही, चरम आनन्द देने वाले सर्वोच्च ज्ञान की अनुभूति हो सकती है। इस प्रकार कला और साहित्य में कामुकता को स्थान देने के लिए अध्यात्मवाद का भी सहारा लिया गया।
मध्यकाल में संस्कृत, पाली और प्राकृत में प्राचीन ग्रन्थों पर पर्याप्त टीकाएँ हुई ये सभी पाँचवीं और अठारहवीं शताब्दियों के बीच लिखी गईं। इनमें न केवल धर्मसूत्रों एवं स्मृतियों की व्याख्या है, बल्कि पाणिनी के व्याकरण, गृह्यसूत्र, स्रौतसूत्र, सुल्वसूत्र और चिकित्सकीय और दार्शनिक ग्रन्थ भी शामिल हैं। पाली ग्रन्थों की टीकाओं को अट्ठकथा कहा जाता है; और प्राकृत ग्रन्थों की टीकाओं को करनी, भाष्य और नियुक्ति। ऐसे साहित्य ने बौद्धिक जीवन में शासनात्मक प्रवृत्ति को मजबूत किया, जिससे राज्य और वर्ण आधारित पितृसत्तात्मक समाज को बनाए रखने तथा इन्हें नई स्थितियों में अनुकूलित करने की कोशिश की गई। सन् 600 से 900 के बीच कई कानून संहिताएँ लिखी गईं। स्वयं को स्वीकार्य बनाने के लिए, कुछ कानून निर्माताओं ने खुद को वृद्ध मनु या बृहत् पराशर कहा। कुल मिलाकर, इन टीकाओं ने सामाजिक असमानता की अनिवार्यताओं को बनाए रखने और भूमि एवं शक्ति के असमान वितरण से उत्पन्न नियमों एवं अनुष्ठानों की नई असमानताओं को उजागर करने में भी मदद की। ऐसी टीकाएँ अठारहवीं शताब्दी तक जारी रहीं। इन्हें आगे भी निरंतर बनाए रखने के लिए कोशिश की गई किन्तु मध्य काल की संकीर्ण मानसिक प्रवृत्ति और संकीर्ण अर्थव्यवस्था से जुड़ी होने के कारण इनमें रचनात्मकता का ह्रास होने लगा था।
दैवीय पदानुक्रम
सातवीं-आठवीं शताब्दी के बाद प्रत्येक क्षेत्र ने मूर्तिकला और मन्दिरों के निर्माण में अपनी शैली विकसित की। दक्षिण भारत, विशेष रूप से, प्रस्तर मन्दिरों की भूमि बन गया। पत्थर और काँसे से देवताओं की मूर्तियों को साकार किया गया। इस दौरान बड़े पैमाने पर पत्थर और काँस्य प्रतिमाओं का निर्माण शुरू हो गया। यद्यपि ये मूर्तियाँ हिमालयी क्षेत्र में भी मिलती हैं, किन्तु दक्षिण भारत में काफी प्रभावशाली संख्या में थीं। दक्षिण में उनका उपयोग, ब्राह्मण मन्दिरों में, पूर्वी भारत में बौद्ध मन्दिरों एवं विहारों में किया गया था। यद्यपि पूरे भारत में देवी-देवताओं की पूजा की जाती थी, लेकिन हर क्षेत्र के लोग उन्हें अपने तरीके से चित्रित करते थे।
उत्तरवती गुप्त काल के बाद दैवीय पदानुक्रम दिखना प्रारम्भ हो जाता है। सार्वजनिक मन्दिरों में महत्ता के अनुसार विभिन्न देवताओं को भी स्तरों में व्यवस्थित किया गया था। जिस तरह अनुष्ठान, भू-सम्पत्ति, सैन्य शक्ति आदि के आधार पर समाज कई वर्गों में विभाजित था उसी तरह देवताओं को भी असमान श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया। विष्णु, शिव और दुर्गा सर्वोच्च देवता थे, ये अन्य सभी देवी-देवताओं से श्रेष्ठ थे, अन्य सभी की महत्ता इनसे कम थी, सब के सब इनके अनुचर, अनुगामी थे। सर्वोच्च देवता को सबसे बड़े आकार में और अधीनस्थ देवी-देवताओं को अपेक्षाकृत छोटे आकारों में चित्रित किया जाता था। इससे पता चलता है कि विभिन्न जनजातियों और निम्न श्रेणियों द्वारा पूजे गए देवताओं को मजबूरीवश दैवीय पदानुक्रम में लाया गया था। पंचदेव कहे जाने वाले ब्रह्मा, गणपति, विष्णु, शक्ति एवं शिव के पूजन की प्रथा थी। मुख्य देवता शिव या कुछ अन्य देवता को मुख्य मन्दिर में स्थापित किया जाता था, जिनके चारों ओर अन्य चार देवताओं के चार सहायक देवस्थानों का निर्माण किया जाता था। ऐसे मन्दिरों को पंचायतन के रूप में जाना जाता था। इन्द्र, वरुण, एवं यम जैसे वैदिक देवता निचले क्रम के लोकपाल या सुरक्षाकर्मी होते थे। शुरुआती मध्ययुगीन देवताओं से हमें सांसारिक पदानुक्रम पर आधारित दैवीय पदानुक्रम का विचार दिखाई देता है। उनमें से कई में, देवी माता को अन्य देवी देवताओं की तुलना में सर्वोच्च दिखाया गया है। हमें ऐसे देवता केवल शैववाद, शक्तिवाद और वैष्णववाद में ही नहीं, जैन और बौद्ध धर्म में भी देखने को मिलते हैं, जिनमें देवताओं को उनके पदानुक्रम के मद्देनजर चित्रित और प्रदर्शित किया जाता था।
जैनों, शैवों, वैष्णवों और अन्य धर्मावलम्बियों के विहारों के संगठन भी पाँच श्रेणियों में विभाजित थे। आचार्य का पद सर्वोच्च होता था, जिनकी ताजपोशी राजकुमार की तरह होती थी, उपाध्याय और उपासक उनसे कमतर पदों पर अपना अधिकार रखते थे।
भक्ति पन्थ
सातवीं शताब्दी के बाद से, भक्ति पन्थ पूरे भारत में फैला, विशेष रूप से दक्षिण में। भक्ति का अर्थ था कि लोग भगवान को सभी प्रकार के चढ़ावा चढ़ाते थे, जिसके बदले उन्हें प्रसाद या भगवान् का आशीर्वाद मिलता था। इसमें भगवान के प्रति भक्त का सम्पूर्ण समर्पण होता है। यह प्रथा किसानों एवं उनके मालिक जमीन्दारों के सम्बन्धों की तरह ही थी। जैसे काश्तकार या किसान अपने मालिक समर्पण भाव से सेवाएँ प्रदान कर बदले में उनसे जमीन और संरक्षण प्राप्त करने की कामना करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य और उनके देवता के बीच भी वैसे ही सम्बन्ध स्थापित हुए। जिस प्रकार सामन्तवाद के तत्त्व देश में लम्बे समय तक बने रहे, वैसे ही भारतीय लोकाचारों में भक्ति भी गहराई से समाई रही।
तन्त्रवाद
छठी शताब्दी के बाद भारत के धार्मिक क्षेत्र में सबसे उल्लेखनीय विकास तन्त्रवाद का फैलाव था। भक्ति पन्थ की तरह, तन्त्रवाद भी सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों के सन्दर्भ में देखे जा सकते हैं। पाँचवीं-सातवीं शताब्दी में, कई ब्राह्मणों ने नेपाल, असम, बंगाल, उड़ीसा, मध्य भारत और दक्कन में भूमि प्राप्त की और इसी काल में तान्त्रिक ग्रन्थ, तान्त्रिक तीर्थस्थल एवं तान्त्रिक प्रथाएँ अस्तित्व में आईं। तान्त्रिक प्रथाओं में महिला एवं शूद्र, दोनों का प्रवेश हुआ; जादुई अनुष्ठानों पर बहुत जोर दिया गया। पहले से ही चलन में रहे कुछ अनुष्ठानों को भी, छठी शताब्दी के बाद से तान्त्रिक ग्रन्थों में व्यवस्थित रूप से दर्ज किया गया। वे भक्तों की भौतिक सम्पत्तियों, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने; उनकी पीड़ाओं का निवारण करने के लिए जाने जाते थे। ब्राह्मण समाज में कबीलाई लोगों के बड़े पैमाने पर प्रवेश के परिणामस्वरूप ही तान्त्रिकता स्पष्ट रूप से पैदा हुई। ब्राह्मणों ने कई कबीलाई अनुष्ठानों, टोटके और प्रतीकों को अपनाया, जिसे उन्होने बाद में आधिकारिक रूप से संकलित, प्रायोजित और प्रचारित किया। समय के साथ पुजारियों द्वारा इस पद्धति में सुविधानुसार परिवर्तन भी किया गया। तन्त्रवाद जैन, बौद्ध, शैव एवं वैष्णववाद में भी समाहित हुआ। सातवीं शताब्दी के बाद से, यह पूरे मध्यकाल में खूब प्रचलन में रहा। भारत के विभिन्न हिस्सों से प्राप्त कई मध्ययुगीन पाण्डुलिपियों में कहा गया कि तन्त्रवाद का प्रसार इतना फैल चुका था कि इस समय तक ज्योतिष और तंत्र को अलग-अलग करना मुश्किल हो गया था।
सारांश
संक्षेप में, छठी और सातवीं शताब्दी में राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, भाषा, साहित्य, लिपि और धर्म में कुछ बड़े परिवर्तनों के साक्ष्य मिलते हैं। इस अवधि के दौरान, प्राचीन भारतीय जीवन के प्रमुख तत्वों के स्थान पर मध्ययुगीन जीवन के तत्व सामने आने लगे थे। कुल मिलाकर, इन परिवर्तनों से समाज में एक विशेष प्रकार की अर्थव्यवस्था सामने आई, जिसमें राज्य और किसानों के बीच जमीन्दारों का प्रभुत्व था। वे प्रशासन चलाते थे और जहाँ अधिकारियों को राज्य द्वारा नियुक्त किया जाता था। यह परिवर्तन यूरोप में हुए परिवर्तन जैसा ही था, जहाँ रोमन साम्राज्य के पतन के बाद, छठी शताब्दी से महत्वपूर्ण अधिकार जमीन्दारों के हाथ जा चुके थे। यद्यपि रोम और गुप्त साम्राज्य, दोनों पर हूणों के हमले हुए थे, लेकिन दोनों के परिणाम भिन्न-भिन्न थे। रोमन साम्राज्य पर हूणों और अन्य जनजातियों का इतना अधिक दबाव था कि स्वतन्त्र किसान को आत्मरक्षा और संरक्षण हेतु जमीन्दारों के समक्ष अपनी स्वधीनता अर्पित करनी पड़ी। भारत में हूणों के हमलों का इतना अधिक प्रभाव नहीं था।
रोमन समाज के विपरीत, प्राचीन भारतीय समाज ने किसी भी स्तर पर उत्पादन में गुलामों को नहीं लगाया यहाँ उत्पादन और कर-संग्रह का मुख्य भार किसानों, कारीगरों, व्यापारियों एवं कृषि मजदूरों पर ही था, जिन्हें वैश्य एवं शूद्र श्रेणी में रखा गया था। हमें इस व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह के संकेत मिलते हैं, जिससे राज्य अधिकारियों को सीधे उत्पादकों से कर संग्रह करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसीलिए, विभिन्न अधिकारियों को वेतन भुगतान के बदले जमीन देने का प्रचलन शुरू किया गया। यूरोप में चर्च को दिए जाने वाले अनुदानों की तरह ही भारत के प्राचीनतम अनुदान ब्राह्मणों और मन्दिरों को दिए गए थे।
छठी शताब्दी के बाद भारत और यूरोप, दोनों जगह कुटीर उद्योग और वाणिज्यिक गतिविधियों में स्पष्ट गिरावट दिखती है। पाँचवीं छठी शताब्दी में, भारत और रोमन साम्राज्य, दोनों जगह में शहर पूरी तरह नष्ट हो गए। भारत और यूरोप दोनों में कृषि का विस्तार हुआ, जिससे कई ग्रामीण बस्तियाँ बसाई गई। भारत में इसे भूमि अनुदान प्रथा के माध्यम से बढ़ाया गया। प्राचीन काल की समाप्ति के बाद, यूरोप और भारत दोनों जगह, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में शक्तिशाली जमीन्दार वर्ग का उदय हुआ। भूमि अनुदान भले ही धार्मिक या अन्य उद्देश्यों के लिए हुआ हो, लेकिन जमीन्दारों ने सातवीं शताब्दी के बाद से भारत में समाज, धर्म, कला, वास्तुकला और साहित्य को एक आकार प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
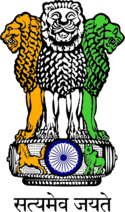
Apostascaixa tá interessante, viu? Já fiz uns palpites e tô curtindo a plataforma. Fácil de usar e com boas opções. Bora ver se a sorte tá do meu lado! Dá uma olhada aqui: apostascaixa