प्रायद्वीप में ब्राह्मणीकरण, ग्रामीण विस्तार और किसान प्रतिरोध (प्राचीन भारत का इतिहास)
नया चरण
सन् 300-750 की अवधि विन्ध्य के दक्षिणी क्षेत्रों में दूसरे ऐतिहासिक चरण को सदश सदर्शाती है। इस चरण में भी प्रथम ऐतिहासिक चरण (ई.पू. 200 से सन् 300) की कुछ प्रक्रियाएँ चल रही थीं। हालाँकि इनमें इस समय कुछ ऐसी विशेषताएँ भी देखने को मिलती हैं, जो पहले चरण में महत्त्वपूर्ण नहीं थीं। पहला चरण, दक्कन और तमिलनाडु के दक्षिणी तमिल राज्यों पर सातवाहनों की विजयगाथा के रूप में दर्ज है। उस अवधि में, उत्तरी तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र के एक अंश और गोदावरी एवं महानदी के बीच के क्षेत्रों पर इनसे बाहर के राज्यो का शासन था। उनके खुद के अपने राज्य नहीं थे। इन क्षेत्रों के साथ ही साथ विदर्भ में भी, सन् 300 से 600 के बीच लगभग दो दर्जन राज्य उभरे, जिनकी जानकारी उस समय के भूमि दस्तावेजों से मिलती है। सातवीं शताब्दी की शुरुआत में, काँची के पल्लव, बदामी के चालुक्य और मदुरै के पाण्ड्या तीन प्रमुख राज्य स्थापित हुए। पहले ऐतिहासिक चरण में पर्याप्त शिल्प, विदेशी और आंतरिक व्यापार, सिक्कों के व्यापक इस्तेमाल और शहरों की बढ़ती संख्या उल्लेखनीय है। किन्तु दूसरे चरण में इनका पतन हो गया। इसी काल में मन्दिरों और ब्राह्मणों को कर-मुक्त जमीनें दान में दी गईं। इन अनुदानों से पता चलता है कि कृषि एवं बसावट के विकास हेतु कई नए क्षेत्रों को उपयोग में लाया गया। इस अवधि में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ।
इसी दौरान हमें समृद्ध ब्राह्मणवाद की स्पष्ट झलक भी दिखाई पड़ती है। पहले चरण में, आन्ध्र और महाराष्ट्र दोनों क्षेत्रों में कई बौद्ध स्मारक मिलते हैं। इसी काल के गुफा अभिलेख शायद तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में जैन और बौद्ध धर्म के प्रभाव का संकेत देते हैं। हालाँकि, अभी जैन धर्म कर्नाटक तक ही सीमित था, जबकि पूरे प्रायद्वीप में राजाओं द्वारा वैदिक यज्ञ-अनुष्ठान के प्रदर्शन के कई उदाहरण मिलते थे। इस चरण में, पल्लवों और बदामी के चालुक्यों के शासन काल में तमिलनाडु और कर्नाटक क्षेत्र में शिव और विष्णु के पाषाण मन्दिरों के निर्माण की शुरुआत भी हुई। द्वितीय चरण में ऐसी स्थिति बनी कि दक्षिण भारत महापाषाणों के देश से परिवर्तित होकर मन्दिरों का देश बन गया।
सांस्कृतिक रूप से देखा जाए तो पहले चरण में द्रविड़ तत्त्व प्रभावी थे, लेकिन दूसरे चरण में आर्याकरण और ब्राह्मणीकरण का प्रभुत्व बढ़ने लगा था। जिसका मुख्य कारण शासकों द्वारा ब्राह्मणों या उनके समर्थकों को अनुदान में भूमि देने की प्रथा का विकास था। मन्दिरों की जमीनों का प्रबंधन भी ब्राह्मणों के हाथों में थी, जहाँ पर उन्होने सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों को आगे बढ़ाया। उन्होने संस्कृत भाषा का प्रचार-प्रसार किया। जो आगे चलकर आधिकारिक भाषा बन गई। आन्ध्र और कर्नाटक में पाए गए अशोक के अभिलेखों से पता चलता है कि लोग ई.पू. तीसरी शताब्दी में प्राकृत जानते थे। इतना ही नहीं, ई.पू. दूसरी और ईस्वी सन् की तीसरी शताब्दी के लेख मुख्यतः प्राकृत में ही लिखे गए थे। तमिलनाडु में पाए गए ब्राह्मी अभिलेखों में भी प्राकृत शब्द हैं, लेकिन सन् 400 के बाद प्रायद्वीप में संस्कृत आधिकारिक भाषा बन गई और इसमें सबसे अधिक दस्तावेज लिखे गए।
दक्कन और दक्षिण भारत के राज्य
उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ (बेरार) में, सातवाहनों को जीतकर एक स्थानीय शासक वाकाटकों ने अपनी सत्ता स्थापित की। वाकाटक, स्वयं ब्राह्मण थे, उनकी ताम्रपट्टिकाओं से यह पता चलता है कि उन्होने बड़ी संख्या में भूमि अनुदान दिया। वे ब्राह्मणवादी धर्म के प्रणेता थे और बहुतायत में वैदिक यज्ञ करते थे। उनका राजनीतिक इतिहास दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत में अधिक महत्वपूर्ण है। स्मरणीय है कि चन्द्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक के शाही परिवार में किया था और उनके समर्थन से चौथी शताब्दी की आखिरी तिमाही में शक क्षत्रपों से मालवा और गुजरात को जीत लिया था। हालाँकि, सांस्कृतिक रूप से वाकाटक राज्य, दक्षिण में ब्राह्मणवादी विचारों एवं सामाजिक संस्थानों को प्रसारित करने हेतु एक माध्यम के रूप में कार्य करता था।
वाकाटक शासन के बाद सत्ता बदामी के चालुक्यों के अधीन आई, जिन्होंने लगभग दो शताब्दियों के दौरान सन् 757 तक दक्कन और दक्षिण भारत के इतिहास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसके बाद उनके सामन्त राष्ट्रकूटों ने उन्हें उखाड़ फेंका। चालुक्यों ने अपने आप को ब्रह्मा, मनु या चन्द्रमा का वंशज माना। उन्होंने दावा किया कि उनके पूर्वजों ने अयोध्या पर शासन किया था, लेकिन यह सब सामाजिक वैधता और सम्मान पाने के लिए किया गया था। वास्तव में वे एक स्थानीय कन्नड जाति के थे, जिन्हें ब्राह्मणों ने क्षत्रिय के वर्ण में शामिल कर लिया गया था।
चालुक्य ने अपने राज्य की स्थापना छठी शताब्दी की शुरुआत में पश्चिमी दक्कन में की। उन्होंने बीजापुर जिले के वातापी (आधुनिक बदामी) में अपनी राजधानी स्थापित की, जो आज कर्नाटक का हिस्सा है। बाद में वे कई स्वतन्त्र राज घरानों में विभाजित हो गए। लेकिन मुख्य शाखा दो शताब्दियों तक वतापी पर शासन करती रही। परवर्ती मध्यकाल में विजयनगर के पहले तक, दक्कन में उस दौरान कोई अन्य शक्ति बदामी के चालुक्यों से अधिक मजबूत नहीं थी।
प्रायद्वीप के पूर्वी हिस्से में सातवाहन ताकतों के ध्वंस के बाद, कृष्णा-गुण्ट्रर क्षेत्र में इक्ष्वाकुओं का उभार हुआ। वे एक स्थानीय जनजाति थे, जिन्होंने अपने वंश की प्राचीनता प्रदर्शित करने हेतु अपना नाम इक्ष्वाकु कर लिया था। और ब्राह्मण होने का दावा भी करने लगे। उन्होंने नागार्जुनकोण्डा और धरानीकोटा में कई स्मारक बनवाए, कृष्णा-गुण्ट्रर क्षेत्र में भूमि अनुदान की प्रथा शुरू की। कृष्णा-गुण्टूर क्षेत्र से ताम्रपट्ट पर उनके कई अभिलेखों की खोज की गई है।
इक्ष्वाकुओं को हटाकर पल्लवों ने अपनी सत्ता कायम की। पल्लव शब्द का अर्थ है लता, जो कि तमिल शब्द तोण्डई का संस्कृत संस्करण है, जिसका अर्थ भी लता का ही पर्यायवाची है। पल्लव सम्भवतः एक स्थानीय जनजाति थे, जिन्होंने तोण्डइनाडु या लता की भूमि में अपना अधिकार स्थापित किया। हालाँकि, उन्हें तमिल में पूरी तरह ढलने और स्वीकार्य होने में कुछ समय लगा, क्योंकि तमिल में पल्लव शब्द का पर्याय लुटेरा भी है। पल्लवों का प्रभाव दक्षिणी आन्ध्र और उत्तरी तमिलनाडु दोनों में फैला। उन्होंने काँची, वर्तमान काँचीपुरम, में अपनी राजधानी की स्थापना की, जो उनके शासनकाल में वैदिक शिक्षा और मन्दिरों का शहर बना।
आरम्भ में पल्लवों का कदम्बों के साथ संघर्ष हुआ, जिन्होंने चौथी शताब्दी में उत्तरी कर्नाटक और कोंकण पर अपनी सत्ता स्थापित की थी। उन्होंने ब्राह्मण होने का दावा किया और उदारतापूर्वक अपनी ब्राह्मणों को पुरस्कृत किया।
कदम्ब राज्य की स्थापना मयूरशर्मन ने की थी। ऐसा कहा जाता है कि वे काँची में शिक्षा प्राप्त करने आए थे, परन्तु उन्हें अपमानित कर अनैतिक रूप से बाहर निकाल दिया गया। इस अपमान के बाद, कदम्ब प्रमुख मयूरशर्मन ने जंगल में अपना शिविर स्थापित किया और जनजातियों की सहायता से पल्लवों को पराजित किया। पल्लवों ने भी अपनी पराजय का बदला तो लिया, लेकिन मयूरशर्मन को औपचारिक रूप से राजचिन्ह देखर कदम्ब को एक स्वतंत्र राज्य स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि मयूरशर्मन ने अठारह अश्वमेधों या घोड़ों की बलि चढ़ाई और कई गाँव ब्राह्मणों को दान में दिए। कदम्बों ने कर्नाटक के उत्तर कनाड़ा जिले में वैजयन्ती या बनवासी में अपनी राजधानी स्थापित की।
पल्लवों का एक और महत्त्वपूर्ण समकालीन राजवंश गंग था। उन्होंने चौथी शताब्दी के आस-पास दक्षिणी कर्नाटक में अपना राज्य स्थापित किया। यह राज्य पूर्व में पल्लवों और पश्चिम में कदम्बों के बीच स्थित था। पूर्वी गंगा से अलग होने के कारण, जो पाँचवीं शताब्दी के बाद कलिंग में शासन करते थे, उन्हें पश्चिमी गंग या मैसूर का गंग कहा जाता है। अपने शासनकाल के अधिकतम समय में, पश्चिमी गंग पल्लवों के सामन्त बने रहे। उनकी प्राचीनतम राजधानी कोलार में स्थित थी, जो सोने की खानों के लिए जाना जाता है, निश्चित ही यह इसके विकास में सहायक हुई होगी।
पश्चिमी गंगों ने ज्यादातर भूमि अनुदान जैनों को दिया था। कदम्बों ने भी जैनों को ही अनुदान दिया, हालाँकि वे ब्राह्मणों को अधिक पसन्द करते थे। पल्लवों ने ब्राह्मणों को दिए गाँवों को कर-मुक्त कर दिया था। शुरुआती पल्लवों की जमीन के सोलह दस्तावेज उपलब्ध हैं। जो पुराने हैं, वे प्राकृत में पत्थर पर लिखे गए थे, लेकिन उनमें से अधिकतर ताम्रपत्र पर संस्कृत में लिखे गए थे। ब्राह्मणों को दिए गए गाँवों को सभी करों और बन्धुआ मजदूरी (बेगार) से मुक्त कर दिया गया था। इसका अर्थ था कि किसानों से ब्राह्मणों द्वारा उनके व्यक्तिगत उपयोग और लाभ के लिए कर संग्रह किया जाता था। चौथी शताब्दी के पल्लवों के अनुदान में ब्राह्मणों को अठारह प्रकार की छूट दी गई थी। उन्हें जमीन के सारे लाभों की अनुमति थी और जमीन के कर, बलात् श्रम, शहर में रहने वाले राजकीय अधिकारियों एवं सिपाहियों के अंकुश और हस्तक्षेप से मुक्त किया गया था।
पल्लव, कदम्ब, बदामी के चालुक्य और उनके अन्य समकालीन; सभी वैदिक यज्ञ के बड़े समर्थक थे। वे अश्वमेध और वाजपेय यज्ञ करते थे, जिससे उन्हें वैधता एवं प्रतिष्ठा प्राप्त हुई और पुजारी वर्ग की आय में भारी वृद्धि हुई। इसलिए जिन किसानों से वे अपना बकाया सीधे वसूलते थे, उनकी जगह ब्राह्मण एक महत्त्वपूर्ण वर्ग के रूप में उभरे। उन्हें उपहार के रूप में राजा द्वारा संग्रहित करों का एक बड़ा हिस्सा भी प्राप्त होता था।
कलभ्र विद्रोह
हालाँकि सन् 300 से 700 के बीच का काल प्रायद्वीप में राज्य के गठन और कृषि विस्तार के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण था; किन्तु चोलों, चेरों और पण्ड्याओं के पतन के बाद प्रायद्वीप की सीमाओं पर क्या हुआ, इस बारे में बहुत ही कम जानकारी है। छठी शताब्दी की एकमात्र महत्त्वपूर्ण घटना कलभ्र विद्रोह है। कलभ्र कबीलाई लोग थे, जिन्होंने चोलों से सत्ता हथियाई और पचहत्तर वर्षों तक शासन किया। उनके शासन से पल्लव और उनके पड़ोसी समकालीन भी प्रभावित हुए। कलभ्र को अत्याचारी शासक के रूप में जाना जाता था, जिन्होंने असंख्य राजाओं को उखाड़ फेंका और तमिल भूमि पर अपनी पकड़ स्थापित की। कलभ्र विद्रोह ब्राह्मणों के विरुद्ध एक शक्तिशाली किसान विरोध था। ‘भूमि अनुदान पर हमला करने वाले साठ हजार वर्षों तक नरक में रहेंगे’ जैसी शिक्षा भी उनके मनोवृति बदलने में विफल रही। उन्होंने कई गाँवों में ब्रह्मदेय अधिकारों को समाप्त कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि कलभ्र बौद्ध अनुयायी थे, क्योंकि उन्होंने बौद्ध विहारों का संरक्षण किया। कलभ्र का विद्रोह इतना व्यापक था कि उन्हें पण्ड्यों, पल्लवों और बदामी के चालुक्यों के संयुक्त प्रयासों से ही हराया जा सकता था। एक परम्परा के अनुसार, छठी शताब्दी के आखिरी तिमाही तक, कलभ्र ने चोल, पण्ड्या और चेरा राजाओं को जेल में डाल दिया था, जिससे उनके विद्रोह के शक्तिशाली होने का अनुमान लगता है। ब्राह्मणों के भूमि अनुदान रद्द कर देने वाले कलभ्र के विरुद्ध संगठित राजाओं के संघ से स्पष्ट दिखता है कि वह विद्रोह सीधे-सीधे दक्षिण भारत में व्याप्त सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के प्रति था।
इसलिए, ऐसा लगता है कि सुदूर दक्षिण के राजाओं द्वारा ब्राह्मणों को सन् 300 से 500 के बीच कुछ भूमि अनुदान दिया गया था। संगम ग्रन्थों से पता चलता है कि क्षत्रियों को उनके बहादुर कृत्यों के लिए प्रमुखों द्वारा गाँव अनुदान दिया गया था। तीसरी शताब्दी के अन्त से भूमि अनुदान के कारण दक्षिणी आन्ध्र और उत्तर तमिलनाडु में पल्लवों के अधीन कृषि विस्तार को बढ़ावा मिला, लेकिन इससे सम्भवतः किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
पल्लवों और चालुक्यों का संघर्ष
छठी से आठवीं शताब्दी के आस-पास प्रायद्वीपीय भारत के राजनीतिक इतिहास का मुख्य हित काँची के पल्लव और बदामी के चालुक्यों के बीच वर्चस्व के लम्बे संघर्ष पर केन्द्रित था। पण्ड्या, जिनका तमिलनाडु के मदुरै और तिरुनेलवेली जिलों पर नियन्त्रण था, इस संघर्ष में एक कमजोर तृतीय शक्ति के रूप में शामिल हुए। हालाँकि पल्लवों और चालुक्यों, दोनों ने ब्राह्मणवाद अपनाया, वैदिक यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनुदान दिया, किन्तु दोनों एक दूसरे से लूट की सामग्री, प्रतिष्ठा और क्षेत्रीय संसाधनों के लिए लड़े। दोनों ने कृष्ण और तुंगभद्रा के बीच वाली भूमि पर वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास किया। यह दोआब फिर से विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों के बीच गले की हड्डी साबित हुई। बार-बार, पल्लव शासकों ने तुंगभद्रा पार करने की कोशिश की, जो दक्कन के कई राज्य और सुदूर दक्षिण के बीच प्राकृतिक ऐतिहासिक सीमा थी। अतः यह संघर्ष उतार-चढ़ाव के साथ लम्बा चला।
इस लम्बे संघर्ष में पहली महत्त्वपूर्ण घटना सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा, पुलकेशिन द्वितीय (सन् 609-42), के शासनकाल के दौरान घटी। जिसका विवरण उनके दरबारी कवि रविकीर्ति द्वारा लिखित प्रशस्ति ग्रन्थ एहोल में दर्ज अभिलेख से मिलती है। यह अभिलेख संस्कृत में प्राप्त काव्य उत्कृष्टता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और अतिशयोक्ति के बावजूद यह पुलकेशिन के जीवन का एक मूल्यवान स्त्रोत है। उन्होंने कदम्ब की राजधानी बनवासी पर कब्जा कर लिया और मैसूर के गंग को अपनी सम्प्रभुता स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने नर्मदा पर हर्ष की सेना को हराया और उनके दक्कन अगुवाई को रोक दिया। पल्लवों के साथ संघर्ष में, वे लगभग पल्लव राजधानी तक पहुँच चुके थे, लेकिन पल्लवों ने अपने उत्तरी प्रान्तों को पुलकेशिन द्वितीय को देकर शान्ति समझौता कर लिया। सन् 610 के आस-पास पुलकेशिन द्वितीय ने कृष्णा और गोदावरी के बीच के पूरे क्षेत्र को जीत लिया, जिसे वेंगी कहा जाता था। यहाँ, मुख्य राजवंश का एक केन्द्र स्थापित किया गया, जिसे वेंगी के पूर्वी चालुक्य राजवंश के रूप में जाना जाने लगा। हालाँकि, पल्लव पर पुलकेशिन का दूसरा आक्रमण विफल हो गया। सन् 642 के आस-पास, जब पुलकेशिन द्वितीय शायद पल्लवों से युद्ध में मारे गए, पल्लव राजा नरसिंहवर्मन (सन् 630-68) ने चालुक्य राजधानी वातापी पर कब्जा कर लिया और वातापिकोण्डा या वातपी के विजेता का खिताब ग्रहण किया। कहा जाता है कि उन्होंने चोल, चेर, पण्ड्या और कलभ्र को भी हरा दिया था।
सातवीं शताब्दी के अन्त में, यह संघर्ष शान्त हो गया था, जो आठवीं सदी के पूर्वार्ध में फिर से शुरू हो गया। माना जाता है कि चालुक्य राजा विक्रमादित्य द्वितीय (सन् 773-45) ने काँची को तीन बार उखाड़ फेंका था। सन् 740 में, उन्होंने पल्लवों को भी बर्बाद कर दिया था। उनकी जीत ने सुदूर दक्षिण तक पल्लव वर्चस्व को समाप्त कर दिया था, भले ही सत्ता उसके बाद भी एक शताब्दी तक जारी रही। हालाँकि, चालुक्य राजा पल्लवों पर अपनी जीत का जश्न बहुत समय तक नहीं मना पाए। क्योंकि राष्ट्रकूट द्वारा सन् 757 में उनका भी वर्चस्व खत्म कर दिया गया।
मन्दिर
वैदिक यज्ञों के अलावा, ब्रह्मा, विष्णु और शिव, विशेषकर विष्णु और शिव की पूजा लोकप्रिय हो रही थी। सातवीं शताब्दी से, अलवार सन्तों, जो विष्णु के महान उपासक थे, ने इस ईश्वर की पूजा को लोकप्रिय बनाया। और नयनारों ने शैव सम्प्रदाय को। सातवीं शताब्दी से, दक्षिण भारतीयों के धार्मिक जीवन पर भक्ति मार्ग प्रभावी हो गया और अलवारों और नयनारों ने इसे प्रसारित करने में बहुत ही महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
इन देवताओं को स्थापित करने के लिए पल्लव राजाओं ने सातवीं और आठवीं शताब्दी में पत्थर के कई मन्दिरों का निर्माण किया। उनमें से सबसे प्रसिद्ध चेन्नई से 65 किलोमीटर दूर, महाबलीपुरम में स्थित सात रथ मन्दिर हैं। इन्हें सातवीं शताब्दी में नरसिंहवर्मन ने बनाया था, जिन्होंने बन्दरगाह शहर महाबलीपुरम या मामल्लापुरम बसाया था। यह शहर अपने तट मन्दिर के लिए भी प्रसिद्ध है, जो एक विशिष्ट संरचना में निर्मित था, जिसमें पत्थरों को काटे बिना ही स्वतन्त्र रूप से खड़ा किया गया था। इसके अलावा, पल्लवों ने अपनी राजधानी काँची में ऐसे कई संरचनात्मक मन्दिरों का निर्माण किया। आठवीं शताब्दी में बना कैलाशनाथ मन्दिर एक अच्छा उदाहरण है। बदामी के चालुक्यों ने सन् 610 में एहोल में कई मन्दिरों की स्थापना की, जिसकी संख्या लगभग सत्तर है। मन्दिर निर्माण कार्य बदामी और पट्टदकल के निकटवर्ती शहरों में जारी रहा। सातवीं और आठवीं शताब्दी में निर्मित पट्टदकल के दस मन्दिर हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध पापनाथ मन्दिर (सन् 680) और विरुपाक्ष मन्दिर (सन् 740) हैं। इनमें से पहला, जो 30 मीटर लम्बा, उत्तरी शैली में छोटी ऊँचाई और छोटे शिखर का है; दूसरा विशुद्ध रूप से दक्षिणी शैली में निर्मित है। जिसकी लम्बाई 40 मीटर है, इसका शिखर बहुत ऊँचा और वर्गाकार है। मन्दिर की दीवारें रामायण के दृश्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले शिल्प की सुन्दर मूर्तियों से सुशोभित हैं।
हमें यह स्पष्ट नहीं पता कि इन शुरुआती मन्दिरों का रख-रखाव कैसे किया जाता था। आठवीं शताब्दी के बाद, दक्षिण भारत में मन्दिरों के लिए भूमि अनुदान एक आम प्रथा बन गई: इन्हें अधिकतर मन्दिरों की दीवारों पर दर्ज किया गया। अधिकांश मन्दिर ब्राह्मणों द्वारा संचालित होते थे। प्रारम्भिक मध्ययुग से, ये मन्दिर दक्षिण भारत में धार्मिक अनुष्ठानों और जाति आधारित विचारधारा के केन्द्र बन गए; इन मन्दिरों के पास कृषि योग्य भूमि का 60 प्रतिशत हिस्सा होता था। हालांकि, प्राचीन मन्दिरों का निर्माण और रख-रखाव साधारणतः राजा द्वारा प्रजा से संग्रहीत करों से होता था। कर्नाटक में चालुक्य के अधीन कुछ मन्दिर जैन व्यापारियों द्वारा बनवाए गए थे। आम लोगों ने अपने ग्रामीण देवताओं की पूजा धान और ताडी से की, लेकिन कुछ लोग अपनी धार्मिक अभिलाषाओं और प्रतिष्ठा अर्जित करने के लिए अधिक सामग्री का भी अर्पण करते थे।
किसानों से कर की माँग
युद्ध संचालन, कला एवं साहित्य के संवर्द्धन, धर्म की उन्नति और प्रशासनिक तंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपार संसाधनों की जरूरत थी। जाहिर है कि इसकी प्रतिपूर्ति किसान करते थे। वाकाटक और पल्लव साम्राज्यों द्वारा कृषि समुदायों पर लादे गए बोझों की प्रकृति, कमोवेश समान थी, भले ही इनमें पहला पूर्व विदर्भ और महाराष्ट्र में था और दूसरा दक्षिणी आन्ध्र और उत्तरी तमिलनाडु में। भूमि कर के रूप में लिए गए उपज के एक हिस्से के अलावा, राजा अनाज और सोने के भेंट की माँग करते थे; नमक प्राप्त करने हेतु खजूर जैसे पेड़ों और चीनी एवं शराब उत्पन्न करने वाले पौधों की माँग करते थे। स्पष्टतः, गाँवों में धरती के गर्भ के सभी प्राकृतिक संसाधनों पर उनका अधिकार था। इसके अलावा, उनसे फूल, दूध, लकड़ी, घास की माँग की जाती थी, और ग्राम वासियों को मुफ्त में सामान ढोने पर मजबूर किया जाता था। राजा को बन्धुआ मजदूरी या विष्टि का भी हक था।
जब शाही अधिकारी कर संचय अथवा अपराधियों को सजा देने हेतु, गाँवों का दौरा करते और सेना कूच पर होती, तो ग्रामीण समुदायों को इनकी कई जरूरतों की आपूर्ति करनी पड़ती थी। उन्हें गाड़ियों में जोतने के लिए बैल और बिछावन, काष्ठ कोयला, चूल्हा, खाना पकाने के बर्तन और परिचारक प्रदान करते थे।
कर या लगान के रूप में थोपी गई इस पूरी सूची से स्पष्ट है कि राज्य ने किसानों से भारी श्रम और उत्पादन की वसूली की। इनमें से अधिकांश लगान चौथी शताब्दी के बाद ब्राह्मणों को दी गई अठारह प्रकार की छूट में शामिल हो गए। बाद में तो किसानों से अधिक से अधिक लगान की माँग की गई।
भूमि अनुदान और ग्रामीण विस्तार
राजा द्वारा कृषक समुदायों से की गई कई माँगों से उनके भुगतान की क्षमता का अनुमान लगाया जा सकता है। कृषि उत्पादन में वृद्धि के बिना संग्रह सम्भव नहीं हो पाता। इस काल में विन्ध्य क्षेत्रों के पार नए राज्यों का निर्माण दिखता है। हर राज्य में कई प्रमुख होते थे, बड़े राज्य के भीतर कई छोटे राज्य होते थे। हर बड़े-छोटे, आला अधिकारी या सामन्त को अपने प्रशासनिक कार्यकर्ता समूह, पुजारियों एवं अन्य कर्मियों की आवश्यकता होती थी। इसलिए प्रत्त्येक राज्य को संसाधनों की आवश्यकता थी। इसलिए, ग्रामीण समुदायों में या गाँवों के कृषि उत्पादन में वृद्धि के बिना कोई राज्य बढ़ नहीं सकता था। ऐसा लगता है कि कबीलाई इलाकों में, ब्राह्मणों को जमीन दी गई और आदिवासियों ने उनसे खेती के बेहतर तरीके एवं मवेशियों का संरक्षण सीखा। किसानों ने भी ब्राह्मणों से नए पंचांग के बारे में सीखा, जिससे कृषि में मदद मिली। कुछ क्षेत्रों को श्रम शक्ति की कमी का सामना करना पड़ा। ऐसे क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने की अनिवार्यता में कुछ फसल धारकों और बुनकरों को ब्राह्मण समुदाय को सौंपे गए कार्य को भी करना पड़ा। जैसा कि पल्लव अनुदान के एक प्राचीन अभिलेख से विदित होता है। इसलिए, ब्राह्मणों को दिए गए पर्याप्त अनुदानों ने खेती के नए तरीकों के प्रसार और ग्रामीण समुदायों के आकार की वृद्धि में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
इस अवधि में दक्षिण भारत में तीन प्रकार के गाँव देखे गए उर, सभा और नगरम। उर सामान्य प्रकार के गाँव थे, जहाँ किसान जातियाँ रहती थीं, जिनकी जमीनें शायद सार्वजानिक होती थीं; यह गाँव के प्रमुख की जिम्मेदारी होती थी कि वे उनसे कर वसूल कर उनकी ओर से करों का भुगतान करें। ऐसे गाँव मुख्यतः दक्षिणी तमिलनाडु में पाए जाते थे। गाँवों के दूसरे प्रकार सभा में ब्रह्मदेय गाँव या ब्राह्मणों को दिए गए गाँव और अग्रहार गाँव शामिल थे। ब्राह्मण भूस्वामियों ने देश में व्यक्तिगत अधिकार का फायदा उठाया, लेकिन अपनी सामूहिक गतिविधियाँ जारी रखी। नगरम प्रकार के गाँव में व्यापारियों और सौदागरों के वर्चस्व वाले गाँव शामिल थे। सम्भवतः व्यापार में गिरावट आने पर गाँवों में आकर बस गए व्यापारियों के कारण ऐसा हुआ हो। चालुक्य क्षेत्रों में, गाँवों का संचालन बुजुर्ग करते थे, जिन्हें महाजन कहा जाता था। कुल मिलाकर, सन् 300-750 में कृषि विस्तार, ग्रामीण संगठन और भूमि की उत्पादन क्षमता के अधिक उपयोग का बेहतर प्रमाण मिलता है।
सामाजिक संरचना और ब्राह्मणीकरण
हम इस अवधि में विकसित सामाजिक संरचना की एक नई रूपरेखा प्रस्तुत कर सकते हैं। समाज में शासकों और पुजारियों का वर्चस्व था। शासकों ने ब्राह्मणों या क्षत्रियों के दर्जे का दावा किया, हालाँकि उनमें से कई स्थानीय कबीले के प्रमुख थे, जिन्हें पुरोहितों ने प्राप्त उपकारों के बदले दूसरे वर्ण में पदोन्नत कर दिया था। पुजारियों ने इन प्रमुखों के लिए सम्माननीय पारिवारिक इतिहास बनाया और उन्हें सूर्य और चन्द्र राजवंशों का बताया। इस प्रक्रिया ने नए शासकों को लोगों के बीच स्वीकार्य होने में सक्षम बनाया। पुजारी मुख्यतः ब्राह्मण थे, हालाँकि जैन और बौद्ध भिक्षुओं को भी इस श्रेणी में रखा जा सकता है। इस चरण में, भूमि अनुदान के माध्यम से पुजारियों का प्रभाव और अधिकार बढ़ा। कई दक्षिण भारतीय शासकों ने ब्राह्मण होने का दावा किया, जो दर्शाता है कि दक्षिण में क्षत्रिय उतने महत्त्वपूर्ण नहीं थे, जितने उत्तर में। वैश्यों के साथ भी ऐसा ही था। भले ही दक्षिण भारत में वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई, लेकिन इसकी प्रथा आर्यवर्त या उत्तर भारत के मुख्य भाग से अलग थी।
हालाँकि, उत्तर की तरह, पदक्रम में शासकों और पुजारियों के बाद किसान आते थे, जो विभिन्न किसानी जातियों में विभाजित थे। ब्राह्मणवादी व्यवस्था में सम्भवतः उनमें से ज्यादातर शूद्र कहलाते थे। यदि किसान और कारीगर जाति उत्पादन और भुगतान करने में असफल होते, तो इन्हें स्थापित धर्म या व्यवस्था से बाहर कर दिया जाता था। ऐसी परिस्थिति को कलियुग कहा गया। इन परिस्थितियों को समाप्त कर, प्रमुखों एवं पुजारियों के अनुकूल शान्ति एवं व्यवस्था बहाल करना राजा का कर्तव्य था। इसलिए, वाकाटकों, पल्लवों, कदम्बों और पश्चिमी गंग राजाओं को धर्म-महाराजा की उपाधि दी गई। पल्लव शासन के असली संस्थापक, सिम्हावर्मन को, कलियुग की बुराइयों से घिरे हुए, धर्म के बचाव का श्रेय जाता है। स्पष्टतः इसका इशारा कलभ्र विद्रोह की ओर है, जिसने पारम्परिक रूप से चली आ रही सामाजिक व्यवस्था को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया था।
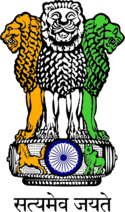
Hey all, has anyone ever used 555wincom? I’m curious! Looks like a nice platform for gaming. You can check it out here 555wincom.