शिल्प, वाणिज्य और शहरी विकास (प्राचीन भारत का इतिहास)
(ई.पू. 200-सन् 250)
शिल्प और शिल्पकार
शकों, कुषाणों, सातवाहनों (ई.पू. 200-सन् 250) और प्रथम तमिल राज्यों का शक काल, प्राचीन भारत के शिल्प और वाणिज्य के इतिहास में सर्वाधिक समृद्धि का काल था। इस दौरान कला और शिल्प में विशेष रूप से वृद्धि हुई। प्राचीन ग्रन्थों में हम इतने प्रकार के कारीगर नहीं पाते जितना इस अवधि के लेखन में। मौर्य काल से पूर्व से सम्बन्धित ग्रन्थ दीघ निकाय में लगभग दो दर्जन व्यवसायों का उल्लेख है, इसी काल के दूसरे ग्रन्थ महावस्तु में राजगीर शहर में रहने वाले छत्तीस प्रकार के कारीगरों की सूची है, फिर भी यह सूची सम्पूर्ण नहीं है। मिलिन्द पान्हो या मिलिन्द प्रश्न में पचहत्तर व्यवसायों का उल्लेख है, जिनमें से साठ विभिन्न शिल्पों से जुड़े हैं। अंग्रेजी में द गारलैण्ड ऑफ मदुरै के नाम से प्रसिद्ध तमिल मूलग्रन्थ में उपर्युक्त दिए गए दोनों बौद्ध ग्रन्थो की शिल्प और कारीगरों के बारे में दी गई जानकारी को और विस्तृत किया गया है। इसमें कारीगरों और दुकानदारों के बीच अन्तर नहीं है। इसके अनुसार, कई कारीगर अपनी दुकानों में काम करते थे, जिनमें चित्रकार, बुनकर, दर्जी, मालाकार, सुनार और ताम्रकार शामिल थे। ऐसे कारीगर-दुकानदार शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में रहते थे, यद्यपि साहित्यिक ग्रन्थों में कारीगरों के ज्यादातर कस्बों से जुड़े होने का ही उल्लेख है किन्तु कुछ उत्खननों से जानकारी मिली है कि वे गाँवों में भी रहते थे। तेलंगाना के करीमनगर में एक गाँव में, बढ़ई, लोहार, सोनार, कुम्हार जैसे लोग एक छोर पर और कृषि एवं अन्य मजदूर दूसरे छोर पर रहते थे।
सोना, चाँदी, शीशा, टिन, ताम्बा, पीतल, लोहा और कीमती पत्थरों या गहनों के काम करने वाले आठ शिल्प थे। इसके अतिरिक्त पीतल, जस्ता, सुरमा और लाल संखिया (आर्सेनिक) से जुड़े विभिन्न प्रकार के शिल्पों का भी उल्लेख है। इससे खनन एवं धातु कौशल ज्ञान के विकास एवं विशेषज्ञता का पता चलता है। लोहे के काम में भी तकनीकी ज्ञान ने भारी प्रगति की थी, विभिन्न उत्खनन स्थलों पर कुषाण और सातवाहन परतों में अनेक लौह कलाकृतियों की खोज हुई है किन्तु आन्ध्र के तेलंगाना क्षेत्र इस सम्बन्ध में सबसे अग्रणी रहे हैं। इस क्षेत्र के करीमनगर और नालगोण्डा जिले में हथियारों के अतिरिक्त, तराजू की डण्डी, गढ़ी हुई कुल्हाड़ी, फावडे, हँसिया, हल, उस्तरा और करछुल की खोज की गई है। छुरी-चाकू सहित भारतीय लोहा और इस्पात को एबिसिनियन बन्दरगाहों में निर्यात किया गया, जो पश्चिमी एशिया में बहुत प्रचलित हुए।
कपड़े बनाने, रेशम बुनाई की तकनीक और हथियारों एवं विलास की वस्तुओं के निर्माण की तकनीक भी विकसित हई। मथुरा एक विशेष प्रकार के कपड़े शाटक के निर्माण का मुख्य केन्द्र बन गया था। कुछ दक्षिण भारतीय शहरों में कपडों की रंगाई एक उन्नत शिल्प थी। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के उपनगर उरैयुर में एक ईंट निर्मित रंगाई कुण्ड का पता चला है। इसके अतिरिक्त एरिकामेड में भी इसी तरह के रंगाई वाले कुण्डों की खोज हुई है। ये सभी कुंड पहली-तीसरी शताब्दियों से सम्बन्धित माने जाते हैं, उस समय इन क्षेत्रों में करघे पर वस्त्र बुनाई का व्यवसाय विकसित अवस्था में था। कोल्हू के उपयोग से तेल के उत्पादन में वृद्धि हुई। इस काल के अभिलेखों के अनुसार बुनकरों, सोनारों, रंगरेजों, धातु एवं हाथी दाँत से बनी सामग्री के कारीगरों, जौहरियों, मूर्तिकारों, मछुआरों, लोहारों, गंधियों या इत्र व्यवसायियों ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया तथा उन्हें स्तम्भों, पट्टिकाओं एवं जलाशयों आदि का दान दिया। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय की शिल्पकारी एवं उनसे जुड़े व्यवसायों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी।
हस्तशिल्प में हाथी दाँत तथा शीशे से बनी वस्तुओं और मनी-माणिक्य को तराशने के काम का उल्लेख किया जा सकता है। शंख या सीपियों से उपयोगी सामान बनाने का शिल्प भी सम्पन्न अवस्था में था। कुषाण स्थलों के उत्खनन के परिणामस्वरूप कई शिल्प वस्तुएँ पाई गई हैं। भारतीय हाथी दाँत से बनी वस्तुएँ अफगानिस्तान और रोम में भी पाई गई हैं। जिनको सातवाहन स्थलों पर खुदाई में मिलने वाली हाथी दाँत की वस्तुओं से जोड़कर देखा जाता है। तक्षशिला और अफगानिस्तान में रोमन शीशे की वस्तुएँ पाई गई हैं, यद्यपि भारत में शीशे के शिल्प का ज्ञान ईस्वी के प्रारम्भिक काल में आया, किन्तु यहीं पर यह शिल्प ज्ञान अपनी उन्नत अवस्था में पहुँचा। इसी प्रकार, उत्तरवर्ती मौर्य स्तरों से बड़े पैमाने पर रत्न या मणियाँ मिली हैं, जिनमें सीपियों से बने मनकों एवं चूड़ियों की संख्या सर्वाधिक है। सिक्कों का निर्माण इस काल का एक महत्त्वपूर्ण शिल्प था। यह काल सोने, चाँदी, ताम्बे, काँसे, शीशा और पोटिन से बने कई प्रकार के सिक्कों के लिए प्रसिद्ध है। कारीगरों ने नकली रोमन सिक्के भी बनाए थे। इस अवधि से सम्बन्धित विभिन्न सिक्कों के साँचे, उत्तर भारत और दक्कन में पाए गए हैं। सातवाहन काल के सिक्कों के साँचे से पता चलता है कि एक बार में ही आधे दर्जन सिक्कों की ढलाई हो जाती थी। यद्यपि यूनानी, शक, सातवाहन, कुषाण आदि सभी ने सिक्कों के प्रसार में योगदान दिया। किन्तु, संग्रहालयों में एकत्र सिक्कों के संग्रह को देखते हुए ऐसा लगता है कि सातवाहनों ने सर्वाधिक सिक्के जारी किए। अल्प अवधि तक शासन करने वाले राजाओं ने भी पर्याप्त संख्या में सिक्के जारी किए थे। यह स्थितियां उन इण्डो-ससैनियनयों की है, जिनके सिक्के ब्रिटिश संग्रहालय सहित आधे दर्जन संग्रहालयों में पाए जाते हैं।

कई स्थानों पर इन सिक्कों की ढलाई के साथ प्रचुर मात्रा में खूबसूरत मूर्तियों और अन्य हस्तशिल्पों का निर्माण भी किया गया था। ये लगभग सभी कुषाण और सातवाहन स्थलों पर पाए गए हैं, किन्तु नालगोण्डा जिले का येलेश्वरम विशेष उल्लेखनीय है जहाँ पर उत्खनन में मूर्तियाँ एवं उसे ढालने वाले साँचे सर्वाधिक संख्या में प्राप्त हुए हैं। हैदराबाद से लगभग 65 किलोमीटर दूर स्थित कोण्डापुर में भी मूर्तियाँ और उनके साँचे पाए गए हैं। इन मूर्तियों का उपयोग अधिकतर शहरों में बसे उच्चवर्गीय लोग ही करते थे। उल्लेखनीय है कि गुप्त काल और विशेषकर उत्तर-गुप्त काल के पतन के साथ ऐसी मूर्तियाँ वस्तुतः फैशन से बाहर हो गईं थी।
इस काल के कारीगर मण्डलियों में संगठित थे, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। महाराष्ट्र में दूसरी शताब्दी में, बौद्ध धर्मावलम्बी गृहस्थ लोगों ने कुम्हारों, तेलियों और बुनकरों के पास अपने धन जमा किए ताकि भिक्षुओं को कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुएँ प्रदान की जा सके। इसी शताब्दी में मथुरा के एक प्रमुख द्वारा मासिक आय से धन बचाकर आटा पीसने वाले संघों के पास जमा किया गया था, जिससे हर रोज सौ ब्राह्मणों को भोजन खिलाया जा सके। विभिन्न ग्रन्थों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि इस अवधि के कारीगर कम से कम दो दर्जन मण्डलियों में संगठित थे। अभिलेखों से जानने वाले अधिकांश कारीगर मथुरा क्षेत्र और पश्चिमी दक्कन में ही पाए जाते थे, जो कि पश्चिमी तट पर व्यापार मार्गों एवं बन्दरगाहों से जुड़ा था।
व्यापारियों के प्रकार
द गारलैण्ड ऑफ मदुरै में हुए उल्लेख के अनुसार लोगों की सड़कों पर भीड़ देखकर, सड़कों को बाजार में खरीद और बिक्री करने वालों की नदियों की संज्ञा दी गई है। साकल शहर के विवरण में आपण शब्द की पुनरावृत्ति से दुकानदारों के महत्त्व का संकेत मिलता है। काशी, कोटुम्बरा एवं अन्य जगहों में बने विभिन्न प्रकार के कपड़ों से इनकी दुकानें भरी रहती थीं। कई कारीगर और व्यापारी श्रेणी एवं अयतन नामक मण्डलियों में संगठित थे, लेकिन इन संगठनों के संचालन एवं इनकी कार्य शैली का विवरण न तो महावस्तु में है और न ही मिलिन्द-पन्हो में। व्यापारी और कारीगर, दोनों उच्च, मध्य और निम्न वर्गों में विभाजित थे।
बौद्ध ग्रन्थों में, संगठनों के मुख्य व्यापारी श्रेष्ठी एवं वणिक्-निगम (वणिजग्रामो) के प्रमुख सार्थवाह का उल्लेख है। इसमें लगभग आधे दर्जन छोटे व्यापारियों का भी वर्णन है, जिन्हें वणिज कहा जाता था। वे फल, कन्द-मूल, पके हुए भोजन, चीनी, छाल से बने वस्त्र, घास के रूप में प्रयुक्त मकई का गट्ठर और बाँस बेचते थे। कई दुकानदारों का वर्णन तमिल ग्रन्थों में भी है, वे मिठाई, सुगन्धित पाउडर, बीज और फूलों की माला बेचते थे। इस तरह से ये व्यापारीगण भोजन, वस्त्र, आवास सहित शहरी लोगों की विभिन्न जरूरतें पूरी करते थे। इनमें इत्र के व्यापारी या गन्धिका नाम से प्रसिद्ध बहुविध व्यापारियों को भी जोड़ सकते हैं, जिसके अन्तर्गत कुछ सुगन्धित तेल बनाने वाले व्यवसायी भी आते हैं। उस समय व्यवहारी शब्द का उपयोग भी किया जाता था जिसका अर्थ होता है, जो व्यापार करे; लेकिन व्यापारी शब्द नहीं मिलता। अग्रिवनिजा शब्द स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ भाषाई परिवर्तन करने पर यह व्यापारी अग्रवालों के पूर्ववर्ती हो सकते हैं। इसका चाहे जो भी अर्थ हो, किन्तु उस समय यह निश्चित रूप से थोक व्यापारी हुआ करते थे, जो आन्तरिक और विदेशी व्यापार दोनों करते थे।
व्यापारिक मार्ग और केन्द्र
इस काल का सबसे महत्त्वपूर्ण आर्थिक विकास भारत और पूर्वी रोमन साम्राज्य के बीच विकसित हो रहा व्यापार था। शुरू-शुरू में, थल मार्ग से भरपूर व्यापार होता था, लेकिन शक, पार्थियन और कुषाणों की गतिविधियों ने जमीनी व्यापार मार्ग को बाधित कर दिया। हालाँकि, ईरान के पार्थियन भारत से लोहे और इस्पात का आयात करते थे, लेकिन उन्होंने सुदूर पश्चिमी ईरान तक भारतीय व्यापार के मार्ग में बड़ी बाधाएँ उत्पन्न कीं। इसलिए पहली शताब्दी में व्यापार मुख्यतः समुद्री मार्ग से होने लगा था। ईस्वी के शुरुआती समय में, लोग सम्भवतः मानसून को समझने लगे थे। नाविक कम समय में अरब सागर के पूर्वी तट से सीधे पश्चिमी तट पहुँच जाते थे और इस रास्ते, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित भड़ौच एवं सोपारा; पूर्वी तट पर स्थित अरिकामेडु और ताम्रलिप्ति जैसे विभिन्न बन्दरगाहों तक पहुँच आसान हो गई थी। इन सभी बन्दरगाहों में भड़ौच सबसे महत्त्वपूर्ण और समृद्ध था। यहाँ न केवल सातवाहन साम्राज्य में उत्पादित वस्तुएँ, बल्कि शक और कुषाण राज्यों में उत्पादित वस्तुएँ भी बेची जाती थीं। शक और कुषाण उत्तर-पश्चिमी सीमा से पश्चिमी समुद्री तट तक दो मार्गों का इस्तेमाल करते थे। ये दोनों मार्ग तक्षशिला में मिलते थे और मध्य एशिया होते हुए रेशम मार्ग तक जाते थे। पहला मार्ग सीधे उत्तर से दक्षिण जाता था जो तक्षशिला को सिन्धु घाटी से जोड़ते हुए भड़ौच तक पहुँचता था। दूसरा मार्ग, जिसे उत्तरपथ कहा जाता था, अधिक उपयोग होता था। तक्षशिला से यह आधुनिक पंजाब होते हुए यमुना के पूर्वी तट तक जाता था। यमुना के रास्ते यह दक्षिण में मथुरा और मथुरा से मालवा में उज्जैन पहुँचकर भड़ौच तक जाता था। उज्जैन एक अन्य मार्ग का भी मिलन बिन्दु था, जो इलाहाबाद के पास कौशाम्बी से शुरू होता था।
विदेशी व्यापार के सामान
यद्यपि भारत और रोम के बीच व्यापक स्तर पर व्यापार होता था, किन्तु इसमें जनसाधारण के रोजमर्रा के सामान नहीं होते थे। भोग-विलास वाली वस्तुओं का व्यापार अधिक था, जिसे भव्यता की वस्तुएँ भी कहा जा सकता है। रोम के लोगों ने पहले भारत के दक्षिणी हिस्से के साथ व्यापार शुरू किया, इसीलिए उनके सबसे प्राचीन सिक्के तमिल राज्यों में पाए गए हैं, जो सातवाहन के राज्य की सीमा से बाहर था। रोम के लोग मुख्य रूप से मसालों, जिसके लिए दक्षिण भारत प्रसिद्ध था, के साथ-साथ मध्य और दक्षिण भारत के मलमल, मोती, गहने और कीमती पत्थरों का भी आयात करते थे। रोमन साम्राज्य को भेजी जाने वाली वस्तुओं में लोहे के सामान, विशेषकर छुरी-काँटा, बर्तन आदि महत्त्वपूर्ण थे। मोती, हाथी दाँत, कीमती पत्थर एवं जानवर आदि विलासिता की वस्तुएँ मानी जाती थीं, लेकिन पौधों एवं उसके उत्पादों ने लोगों की बुनियादी जरूरतें जैसे धार्मिक वस्तुएँ, मृत्यु संस्कार से जुड़ी वस्तुएँ, रसोई और औषधि आदि जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति की। आयात की वस्तुओं में बर्तन भी शामिल थे। छुरी-काँटा आदि का प्रयोग उच्च वर्ग के लोगों के लिए महत्त्वपूर्ण था।
भारत द्वारा सीधे निर्यातित वस्तुओं के अतिरिक्त चीन और मध्य एशिया से कुछ वस्तुएँ भारत लाई जाती और फिर रोमन साम्राज्य के पूर्वी हिस्से में पहुँचती थीं। उत्तर अफगानिस्तान और ईरान होते हुए रेशम मार्ग से रेशम सीधे चीन से रोमन साम्राज्य जाता था। हालाँकि ईरान में पार्थियन शासन की स्थापना से पार्थियानों ने एवं उसके पड़ोसी क्षेत्रों ने कठिनाइयाँ उत्पन्न कीं। इसलिए पश्चिमी भारतीय बन्दरगाहों पर रेशम, व्यापार मार्ग में परिवर्तन कर उपमहाद्वीप के उत्तर-पश्चिमी भाग से होकर लाना पड़ता था। रेशम लाने के लिए कभी-कभी चीन से भारत के पूर्वी तट के रास्ते का इस्तेमाल भी होता था और फिर वहाँ से पश्चिम में भेजा जाता था। इस प्रकार भारत और रोमन साम्राज्य के बीच रेशम का पर्याप्त पारगमन व्यापार होता था।
निर्यातित वस्तुओं के बदले, रोम भारत को शराब, सुरा-सुराही और अन्य विभिन्न प्रकार के बर्तन निर्यात करते थे, जो पश्चिम बंगाल के तामलुक, पाण्डिचेरी के निकट अरिकमेडु और दक्षिण भारत एवं अन्य कई स्थलों पर उत्खनन में मिले हैं। कभी-कभी रोम की वस्तुएँ गुवाहाटी तक पहुँचती थीं। जिस शीशे का इस्तेमाल सातवाहन सिक्का बनाने के लिए करते थे, प्रतीत होता है कि वे रोम से छल्ले के रूप में मोड़कर आयातित होते थे। रोमन वस्तुएँ उत्तर भारत में पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते हैं, लेकिन इसमें कोई सन्देह नहीं कि कुषाण काल में रोमन साम्राज्य के पूर्वी भाग के साथ दूसरी शताब्दी में उपमहाद्वीप का उत्तर-पश्चिमी भाग व्यापार करता था। यह मेसोपोटामिया की विजय से सम्भव हुआ था, जिसे सन् 115 में रोम का प्रान्त बनाया गया था। रोम का सम्राट ट्राजन ने न केवल मस्कट पर विजय प्राप्त की, बल्कि फारस की खाड़ी का भी पता लगाया। व्यापार और विजय के परिणामस्वरूप, रोमन वस्तुएँ अफगानिस्तान और उत्तर-पश्चिमी भारत पहुँचीं। काबुल से 72 किलोमीटर उत्तर बेग्राम में, इटली, मिस्त्र और सीरिया में बने बड़े शीशे के जार पाए गए हैं। यहाँ कटोरे, काँसे से निर्मित स्टैण्ड, इस्पात के बने पैमाने और पश्चिमी क्षेत्रों के बाट, यूनानी-रोमन काँसे से बनी छोटी मूर्तियाँ, जग और सिलखड़ी के बने अन्य बर्तन भी मिले हैं। तक्षशिला, जिसे पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिम सीमान्त क्षेत्र में आधुनिक सिरकाप बताया गया है, में यूनानी-रोमन काँसे से बनी छोटी मूर्तियों की कला के अच्छे उदाहरण मिलते हैं। चाँदी के गहने, कुछ काँस्य-बर्तन, एक जार और रोमन सम्राट टाईबेरियस के सिक्के भी पाए गए। हालाँकि, दक्षिण भारत में नियमित रूप से पाए जाने वाले अरेटाइन बर्तन, न तो मध्य या पश्चिमी भारत में दिखाई देते हैं, न ही अफगानिस्तान में। जाहिर है, इन जगहों से वे लोकप्रिय पश्चिमी वस्तुएँ प्राप्त नहीं हुईं, जो दक्षिण में सातवाहन साम्राज्य और उससे भी दक्षिण में पाई गईं। इस प्रकार सातवाहन और कुषाण- दोनों राज्य रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार से लाभान्वित हुए। हालाँकि, सबसे बड़ा लाभ सातवाहनों को हुआ।
यद्यपि भारत में ताम्बे के कुछ रोमन सिक्के भी पाए गए हैं, किन्तु रोमन से मंगाई गई वस्तुओं में सबसे उल्लेखनीय निर्यात सोने और चाँदी के सिक्कों का ही था। पूरे उपमहाद्वीप में लगभग 150 रोमन सिक्कों की खोज हुई है, उनमें से ज्यादातर विन्ध्य के दक्षिण में मिले हैं। भारत में पाए जाने वाले सोने और चाँदी के रोमन सिक्कों की कुल संख्या 6000 से अधिक नहीं है, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि केवल इतने सिक्के ही रोम से आए थे। यह संख्या बहुत बड़ी थी। सन् 77 में रोमन लेखक प्लीनी द्वारा लैटिन में लिखित दस्तावेज नेचुरल हिस्ट्री में अफसोस प्रकट किया गया है कि भारत के साथ व्यापार बढ़ने के कारण रोम में सोना खत्म हो रहा था। यह अतिशयोक्ति हो सकती है, किन्तु रोम द्वारा पूर्व से काली मिर्च की खरीद पर अत्यधिक खर्च की बात सन् 22 की शुरुआत में भी सुनी गई है। पश्चिम के लोग भारतीय काली मिर्च के बड़े शौकीन थे, इसे संस्कृत में यवनप्रिया कहा जाता है। भारत में निर्मित इस्पात के छुरी-काँटे के इस्तेमाल के विरुद्ध भी तीक्ष्ण प्रतिक्रिया थी, क्योंकि इसके लिए रोम के उच्च वर्ग के लोग ऊँची कीमत चुकाते थे। व्यापार के सन्तुलन की अवधारणा तब ज्ञात नहीं थी, लेकिन प्रायद्वीप में रोमन सिक्कों और मिट्टी के बर्तनों की खोज से कोई सन्देह नहीं कि भारत को रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार में लाभ ही मिला और रोम को धन की इतनी गहरी हानि महसूस हुई कि अन्ततः रोम ने भारत से काली मिर्च और इस्पात निर्मित वस्तुओं की खरीद पर प्रतिबन्ध लगा दिया।
प्रतीत होता है कि भारत-रोमन व्यापार और समुद्री व्यापार में रोम ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। भले ही, रोमन व्यापारी दक्षिण भारत में बस गए हों किन्तु इसके बहुत कम प्रमाण मिलते हैं कि भारतीय लोग रोम में जाकर बस गए हों। हालाँकि तमिल में भित्तिचित्रों के मिले कुछ टुकड़ों से पता चलता है कि कुछ तमिल व्यापारी रोमन काल में मिस्त्र में रहते थे।
मुद्रा अर्थव्यवस्था
रोम से आए चाँदी और सोने की मुद्रा का इस्तेमाल भारतीयों ने किस प्रकार किया? सोने के रोमन सिक्के मूल्यवान धातु से निर्मित होने के कारण स्वाभावतः मूल्यवान थे साथ ही उनका इस्तेमाल बड़े लेन-देन में भी होता था। उत्तर में, हिन्द-यूनानी शासकों ने सोने के कुछ सिक्के जारी किए, लेकिन कुषाणों ने बडी संख्या में सोने के सिक्के चलाए। ऐसा सोचना गलत होगा कि सोने के सभी कुषाण सिक्के, रोमन सोना से ही निर्मित थे। ई.पू. पाँचवीं शताब्दी में, भारत ने ईरानी साम्राज्य को 320 तोला स्वर्ण मुद्राएँ अर्पित किया था। यह सोना सिन्ध में सोने की खानों से निकाला गया था। कुषाण सम्भवतः मध्य एशिया से सोना प्राप्त करते थे। या फिर बाद में उनके अधीन हुए कर्नाटक या झारखण्ड के ढालधूम के सोने की खदानों से निकालते रहे होंगे। रोम से सम्पर्क के कारण, कुषाणों ने दीनार रूपी स्वर्ण सिक्के जारी किए, जो गुप्त शासन काल में खूब प्रचलित हुए। हालाँकि, सोने के सिक्कों का उपयोग दिन-प्रतिदिन की लेन-देन में नहीं किया जाता था, ऐसी जगह शीशा, पोटिन या ताम्बे के सिक्के का प्रयोग होता था। आन्ध्र में शीशा और ताम्बा एवं कर्नाटक में सोने की खानें पाई जाती हैं। आन्ध्र ने दक्कन में बड़ी संख्या में शीशा या पोटिन के सिक्के जारी किए। यद्यपि सातवाहनों ने सोने के सिक्के जारी नहीं किए, किन्तु संग्रहालयों से पता चलता है कि उन्होंने अन्य धातुओं के सबसे अधिक सिक्के जारी किए। प्रायद्वीप से कुछ पंच-चिह्नित और प्राचीन संगम युग के सिक्के पाए गए हैं। कुषाणों ने उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी भारत में सबसे अधिक ताम्बे के सिक्के जारी किए। निचले सिन्ध में कुषाणों के उत्तराधिकारी इण्डो-ससैनियन ने भी कई सिक्के जारी किए। ताम्बा और काँस्य के सिक्कों का इस्तेमाल, मध्य भारत के शासक नाग, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती क्षेत्रों सहित पूर्वी राजस्थान में शासन करने वाले यौधेय और कौशाम्बी, मथुरा, अवन्ती और अहिच्छत्र (उत्तर प्रदेश में बरेली जिला) मित्रा जैसे कुछ स्वदेशी राजवंश के शासकों ने किया। ई.पू. 200 एवं 300 के बीच सिक्कों के सर्वाधिक उपयोग के प्रमाण मिले हैं, ये सिक्के केवल भारतीय एवं मध्य एशिया के शासकों द्वारा ही नहीं, कई नगरों और कबीलों द्वारा भी जारी किए गए थे। प्राचीन काल की इस अवधि में, सिक्का निर्माण के ठप्पे एवं साँचा सर्वाधिक संख्या में मिले हैं। नगरों एवं उपनगरों में रहने वाले आम लोगों के जीवन में मुद्रा अर्थव्यवस्था का इतना गहरा प्रवेश सम्भवतः अन्य किसी काल में नहीं हुआ। इतना बड़ा परिवर्तन रोमन साम्राज्य के साथ भारत के व्यापरिक सम्बन्ध के अनुरूप ही था।
शहरी विकास
शिल्प, वाणिज्य एवं मुद्रा के बढ़ते उपयोग ने इस काल के कई शहरों की समृद्धि को बढ़ावा दिया। वैशाली, पाटलिपुत्र, वाराणसी, कौशाम्बी, श्रावस्ती, हस्तिनापुर, मथुरा, और इन्द्रप्रस्थ (नई दिल्ली का पुराना किला) जैसे उत्तर भारत के महत्त्वपूर्ण शहरों का उल्लेख सभी साहित्यिक ग्रन्थों में है; उनमें से कुछ का वर्णन चीनी तीर्थयात्रियों द्वारा भी किया गया है। उत्खनन से कुषाण युग से प्राप्त श्रेष्ठ संरचनाओं को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इन शहरों में से अधिकांश का विकास पहली और दूसरी शताब्दी में कुषाण काल के दौरान ही हुआ। बिहार के चिराँद, सोनपुर एवं बक्सर जैसे कई पुरास्थलों और पूर्वी उत्तर प्रदेश के खैराडीह एवं मसोन से कुषाण काल की समृद्धि के नमूने देखने को मिलते हैं। इसी तरह, उत्तर प्रदेश में सोहगौरा, भीता, कौशाम्बी, श्रृंगवेरपुर एवं अत्रंजिखेरा जैसे शहर स्थल कुषाण काल में समृद्ध अवस्था में थे। राजस्थान में रंगमहल और पश्चिमी क्षेत्रों में कई अन्य स्थान कुषाण काल में समृद्ध हुए। मथुरा के सोनख में हुए उत्खनन में कुषाण काल की सात परतों और गुप्त काल की केवल एक परत का पता चला है। उत्खनन के अनुसार वर्तमान में लखनऊ से 50 किलोमीटर दूर स्थित सच्नन-कोट, उत्तर भारत का सबसे बड़ा कुषाण शहर था। यह 9 वर्ग किलोमीटर में फैला है जिसमें से ईंटों के कई घर और ताम्बे के सिक्के मिले हैं। इसके अतिरिक्त पंजाब में जालन्धर, लुधियाना एवं रोपड़ तथा हरियाणा के कई स्थलों पर भी कुषाण काल के निर्माण की गुणवत्ता का पता चलता है।
कई उदाहरणों के अनुसार, गुप्त काल की संरचनाएँ खराब थीं इसलिए उस समय भी कुषाण ईंटों का इस्तेमाल होता था। कुल मिलाकर, कुषाण काल की इन संरचनाओं के भौतिक अवशेषों से शहरीकरण के विकास की उच्च अवस्था के संकेत मिलते हैं। मालवा के शक साम्राज्य और पश्चिम भारत के शहरों में भी ऐसा ही था। सबसे महत्त्वपूर्ण शहर उज्जैन था, जो कौशाम्बी और मथुरा से अलग-अलग आने वाले दो मार्गों का मिलन बिन्दु था। हालाँकि यह सुलेमानी और कार्नेलियन पत्थरों के निर्यात के लिए प्रसिद्ध था। खुदाई से पता चला है कि ई.पू. 200 के बाद मोती निर्माण के लिए सुलेमानी पत्थर, सूर्यकान्तमणि और कार्नेलियन पत्थर पर बड़े पैमाने पर काम होता था। ऐसा सम्भव था, क्योंकि उज्जैन में शिप्रा नदी की तलहटी से यह कच्ची सामग्री प्रचुरता से प्राप्त होती थी।
शक एवं कुषाण, तथा सातवाहन साम्राज्य में शहरों का विकास एक ही समय में हुआ। सातवाहन काल के दौरान पश्चिमी और दक्षिण भारत में तंगर (तेर), पैठन, धान्यकटक, अमरावती, नागार्जुनकोण्ड, भड़ौच, सोपारा, अरिकमेडु और कावेरीपट्टणम समृद्ध शहर थे। तेलंगाना में कई सातवाहन बस्तियों का पता चला है, जिनमें से कुछ प्लीनी द्वारा उल्लिखित आन्ध्र के तीस दीवारों वाले नगरों के समबर्ती होगी। वे तटीय आन्ध्र के शहरों की तुलना में बहुत पहले और पश्चिमी महाराष्ट्र के शहरों के कुछ ही समय बाद निर्मित हुए होंगे। महाराष्ट्र, आन्ध्र और तमिलनाडु में शहरों का पतन सामान्यतः तीसरी शताब्दी के मध्य या बाद के दिनों में शुरू हो जाता है।
रोमन साम्राज्यों के साथ विकसित व्यापारिक सम्बन्ध के कारण ही कुषाण और सातवाहन साम्राज्यों में शहरों का विकास आसानी से हुआ होगा। उन दिनों भारत, रोमन साम्राज्य के पवी भाग और मध्य एशिया के साथ व्यापार करता था। पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नगरों का विकास भी उत्तर-पश्चिमी भारत में कुषाण सत्ता का केन्द्र होने की वजह से हुआ होगा। भारत में अधिकांश कुषाण शहर मथुरा से तक्षशिला तक उत्तर-पश्चिम या उत्तरपथ मार्ग पर स्थित थे। कुषाण साम्राज्य में इन मार्गों पर सुरक्षा का पर्याप्त प्रबन्ध था। तीसरी शताब्दी में कुषाण साम्राज्य के पतन से इन कस्बों को बड़ा झटका लगा। शायद ऐसा ही दक्कन में भी हुआ। तीसरी शताब्दी में रोमन साम्राज्य द्वारा भारत के साथ व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाने से सातवाहन सत्ता का अन्त हुआ और शहरी कारीगरों और व्यापारियों की हालत गम्भीर हो गई। दक्कन में पुरातात्त्विक खुदाई से सातवाहन काल के बाद से शहरों का पतन स्पष्ट रूप से दिखता है।
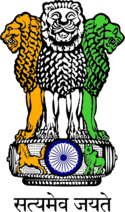
Blaze-4 is legit, been playing there for a while now. Good selection of games and fast payouts. Check it out! blaze-4